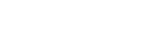आगही पर शेर
आगही उस ख़ज़ाने की चाभी
है जहाँ से सूफ़ी संतों से लेकर फ़लसफ़ियों ने भी बहुत कुछ हासिल किया है। इल्म और आगही की दुनिया मे इन्क़िलाब के इस दौर से पहले भी शायरों ने इस की अहमियत को समझा और तस्लीम किया है। यह आगही अपने वजुद से मुलअल्लिक़ भी हो सकती है और दुनिया के बारे में भी। आगही शायरी की एक झलक पेश हैः
पहाड़ जैसी अज़्मतों का दाख़िला था शहर में
कि लोग आगही का इश्तिहार ले के चल दिए
आगही से मिली है तन्हाई
आ मिरी जान मुझ को धोका दे
आगही दाम-ए-शुनीदन जिस क़दर चाहे बिछाए
मुद्दआ अन्क़ा है अपने आलम-ए-तक़रीर का
आगही कर्ब वफ़ा सब्र तमन्ना एहसास
मेरे ही सीने में उतरे हैं ये ख़ंजर सारे
क्या हो सके हिसाब कि जब आगही कहे
अब तक तो राएगानी में सारा सफ़र किया
अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़-ए-ज़ि़ंदगी
तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन
उजाला 'इल्म का फैला तो है चारों तरफ़ यारो
बसीरत आदमी की कुछ मगर कम होती जाती है
अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो
आगही गर नहीं ग़फ़लत ही सही
जुनूँ के कैफ़-ओ-कम से आगही तुझ को नहीं नासेह
गुज़रती है जो दीवानों पे दीवाने समझते हैं
आगही भूलने देती नहीं हस्ती का मआल
टूट के ख़्वाब बिखरता है तो हँस देते हैं
डुबोए देता है ख़ुद-आगही का बार मुझे
मैं ढलता नश्शा हूँ मौज-ए-तरब उभार मुझे
हम आगही को रोते हैं और आगही हमें
वारफ़्तगी-ए-शौक़ कहाँ ले चली हमें
जैसे जैसे आगही बढ़ती गई वैसे 'ज़हीर'
ज़ेहन ओ दिल इक दूसरे से मुंफ़सिल होते गए
यही आइना है वो आईना जो लिए है जल्वा-ए-आगही
ये जो शाएरी का शुऊर है ये पयम्बरी की तलाश है
उम्र जो बे-ख़ुदी में गुज़री है
बस वही आगही में गुज़री है
इक ज़माने तक बदन बे-ख़्वाब बे-आदाब थे
फिर अचानक अपनी उर्यानी का अंदाज़ा हुआ
उरूज-ए-माह को इंसाँ समझ गया लेकिन
हनूज़ अज़्मत-ए-इंसाँ से आगही कम है
'सौदा' जो बे-ख़बर है वही याँ करे है ऐश
मुश्किल बहुत है उन को जो रखते हैं आगही
अगर शुऊर न हो तो बहिश्त है दुनिया
बड़े अज़ाब में गुज़री है आगही के साथ
शिकवा-ए-ज़ुल्मत-ए-शब से तो कहीं बेहतर था
अपने हिस्से की कोई शम्अ' जलाते जाते
आगही ने दिए इबहाम के धोके क्या क्या
शरह-ए-अल्फ़ाज़ जो लिक्खी तो इशारे लिक्खे
न पूछिए कि वो किस कर्ब से गुज़रते हैं
जो आगही के सबब ऐश-ए-बंदगी से गए
जिन से ज़िंदा हो यक़ीन ओ आगही की आबरू
इश्क़ की राहों में कुछ ऐसे गुमाँ करते चलो
जुनूँ की ख़ैर हो तुझ को 'असर' मिला सब कुछ
ये कैफ़ियत भी ज़रूरी थी आगही के लिए
इस कार-ए-आगही को जुनूँ कह रहे हैं लोग
महफ़ूज़ कर रहे हैं फ़ज़ा में सदाएँ हम
तिरा वस्ल है मुझे बे-ख़ुदी तिरा हिज्र है मुझे आगही
तिरा वस्ल मुझ को फ़िराक़ है तिरा हिज्र मुझ को विसाल है
ख़ुदा का मतलब है ख़ुद में आ तू ख़ुद-आगही है ख़ुदा-शनासी
ख़ुदा को ख़ुद से जुदा समझ कर भटक रहा है इधर उधर क्यूँ
चराग़ सामने वाले मकान में भी न था
ये सानेहा मिरे वहम-ओ-गुमान में भी न था