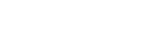ज़िंदाँ पर शेर
क्लासिकी और जदीद शायरी
में ज़िंदाँ का इस्तिआरा बहुत मुस्तामल है और दोनों जगह उस की मानविय्ती जहतें बहुत फैली हुई हैं। क्लासिकी शायरी में ज़िंदाँ का सयाक़ ख़ालिस इश्क़िया था लेकिन जदीद शोरा ने इस लफ़्ज़ को अपने अहद की सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल से जोड़ कर इस में और वुसअतें पैदा की हैं। हमारे इस इन्तिख़ाब को पढ़िए और देखिए कि तख़्लीक़-कार एक ही लफ़्ज़ को कितने अलग अलग रंगों में बरतता है और लफ़्ज़ किस तरह मानी की सतह पर अपना सफ़र तय करता है।
ज़िंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं
हाए इस क़ैद को ज़ंजीर भी दरकार नहीं
जेल से वापस आ कर उस ने पांचों वक़्त नमाज़ पढ़ी
मुँह भी बंद हुए सब के और बदनामी भी ख़त्म हुई
ज़रा सा शोर-ए-बग़ावत उठा और उस के बा'द
वज़ीर तख़्त पे बैठे थे और जेल में हम
अब उस ग़रीब चोर को भेजोगे जेल क्यूँ
ग़ुर्बत की जिस ने काट ली पादाश जेब में
लहू से मैं ने लिखा था जो कुछ दीवार-ए-ज़िंदाँ पर
वो बिजली बन के चमका दामन-ए-सुब्ह-ए-गुलिस्ताँ पर
न किसी आह की आवाज़ न ज़ंजीर का शोर
आज क्या हो गया ज़िंदाँ में कि ज़िंदाँ चुप है
जाने कितने बे-क़ुसूरों को सज़ाएँ मिल रहीं
झूट लगता है तुम्हें तो जेल जा कर देखिए
मैं संतरी हूँ औरतों की जेल का हुज़ूर
दो-चार क़ैदी इस लिए कम गिन रहा हूँ मैं
किन शहीदों के लहू के ये फ़रोज़ाँ हैं चराग़
रौशनी सी जो है ज़िंदाँ के हर इक रौज़न में
जो क़ैदी-ए-मेहन थे 'जमीला' वो चल बसे
ज़िंदाँ में कोई साहब-ए-ज़िंदाँ नहीं रहा
पत्थर ताने लोग खड़े हैं
ज़िंदाँ की दीवार के पीछे
ज़िंदाँ से निकलने की ये तदबीर ग़लत है
ज़ंजीर के टुकड़े करो दीवार गिरा दो
ज़िंदाँ की तो अपने सैर तू कर
शायद कोई बे-गुनाह निकले
हाए ज़ंजीर-शिकन वो कशिश-ए-फ़स्ल-ए-बहार
और ज़िंदाँ से निकलना तिरे दीवाने का