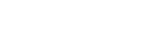मोहब्बत या हलाकत?
स्टोरीलाइन
कहानी एक ऐसे शख़्स की दास्तान को बयान करती है जो अपनी चचाज़ाद बहन से बहुत मोहब्बत करता है। एकाएक वह चचाज़ाद बीमार पड़ जाती है और उसके इलाज के लिए एक नौजवान डॉक्टर आने लगता है। चचाज़ाद डॉक्टर की तरफ़ मुतवज्जा होने लगती है और वह उसी से शादी करने का फै़सला कर लेती है। उसके इस फ़ैसले पर उसका चचाज़ाद भाई अपने उस रक़ीब डाक्टर का क़त्ल कर देता है।
(हयात-ए-इंसानी का एक इ’बरत-अंगेज़ वाक़िआ’)
(बाब - 1)
इ’श्क़ क्या-क्या हमें दिखाता है
आओ तुम भी तो इक नज़र देखो
लोगो मेरा दोस्ताना मश्वरा यही है कि ख़ुदारा दुनिया में सब कुछ करो। आसमानों पर पहुँच जाओ, ज़मीन के नीचे चले जाओ, हवा में मुअ’ल्लक़ हो, मिर्रीख़-ओ-ज़ुहरा के बाशिंदों से यगानगत पैदा करो, सब कुछ करो मगर लिल्लाह... मुहब्बत न करो। ख़ुद पर रहम करो। मुहब्बत न करो! ये तुम्हें तबाह कर देगी, फ़ना कर देगी और सफ़्हा-ए-हस्ती से हर्फ़-ए-ग़लत की तरह मिटा देगी। मेरे प्यारे दोस्तो कुँए में गिरना अच्छा, समंदर में कूदना बेहतर, मगर मुहब्बत की शफ़्फ़ाफ़ और ख़ूबसूरत नहर से एक बूँद लेना भी निहायत ख़तरनाक।
आज मैं चाहता हूँ कि अपनी इ’बरत-अंगेज़ दास्तान को अपनी ज़िंदगी की आख़िरी घड़ियों में आपको सुना दूँ ताकि मेरे बा’द मेरे हम-जिंसों पर रौशन हो जाए कि मुहब्बत और औ’रत हलाकत का दूसरा नाम है और कोई भूल कर भी इस हलाकत में पड़े।
दिल दे के उसको ये मुझे मा’लूम हो गया
सब कुछ करे मगर न मुहब्बत करे कोई
ख़ैर मुझे इन बातों से मतलब नहीं। वक़्त थोड़ा है और दास्तान तवील। इसलिए मैं मुख़्तसर अल्फ़ाज़ में अपना फ़साना-ए-ज़िंदगी अज़-इब्तिदा-ता-इंतिहा बयान कर दूँगा।
“कलेजा थाम लोगे जब सुनोगे दास्ताँ मेरी!”
मुझे जैरूस पहुँचे दूसरा ही हफ़्ता था कि एक अ’जीब-ओ-ग़रीब वाक़िआ’ गुज़रा। इसकी “अ’जीब-ओ-ग़रीबियत” सिर्फ़ एक अफ़साना या रोमांस (Romance) की हद तक ख़त्म नहीं होती बल्कि आह वो मेरे शीराज़ा-ए-हस्ती या यूँ कहिए कि किताब-ए-हयात के औराक़ को बिखेर देती है।
मैं वतन से निकल भागा था और एक ख़ास सिलसिले में जैरूस भागा-भागा आया था और गुमनामी रू-पोशी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। अक्सर-औक़ात अपनी ज़िंदगी की अलम-नाक वाक़िआ’त को याद कर के परेशान हो जाया करता था। अक्सर ऐसा हुआ कि शिद्दत-ए-वहशत में दिन-दिन भर चिलचिलाती-धूप में पहाड़ों के दामन में भूका प्यासा बैठा रहा हूँ। इस बादिया-पैमाई का सबब क्या है? मैं क्यों रुपोश हुआ? ये सब आपको आइंदा मा’लूम होगा।
एक गर्म शाम तबीअ’त मुतवहि्ह्श हुई तो अपने कमरे के बाहर सड़क पर टहलने निकल गया। दूर से एक हुजूम नज़र आने लगा। मैं खड़ा हो गया और ग़ौर से लोगों के जीते-जागते दरिया को देखने लगा। ऐसा ख़ामोश हुजूम आज तक मेरी नज़रों से न गुज़रा था। थोड़ी ही देर में ऊ’द-ओ-अ’बीर की मुतबर्रिक ख़ुश्बू आने लगी। मैं समझ गया कि किसी का जनाज़ा है। दफ़अ’तन लोग निहायत मुअस्सिर धीमे लहजे में क़ुरआनी मुक़द्दस आयतों को पढ़ने लगे। अब वो लोग बहुत क़रीब आ गए थे। जब ये हुजूम मेरे बिल्कुल क़रीब आया तो अगरचे मैं जैरूस के बाशिंदों के लिए बिल्कुल अजनबी था और किसी से मेरी वाक़्फ़ियत नहीं थी। ताहम मज़हबी एहतिराम और मुस्लिम क़ौमी की उख़ुव्वत के मुताबिक़ मुझे भी ख़ामोशी के साथ इस हुजूम में शरीक होना पड़ा ताकि क़ब्रिस्तान तक अपने मरहूम मज़हबी भाई को पहुँचा दूँ।
जब क़ब्रिस्तान पहुँच कर लोग मय्यत को एक तरफ़ रखकर नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हुए तो मैंने उनमें से एक से दरियाफ़्त किया कि किसका जनाज़ा है? मुझसे कहा गया कि शहर के एक मुअ’ज़्ज़िज़ और बड़े ताजिर का इंतिक़ाल हो गया है। इसके बा’द हम सबने मिलकर मरहूम भाई की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह पाक से दुआ’ माँगी।
मय्यत को सपुर्द-ए-ख़ाक कर के लोग क़ब्रिस्तान से वापिस हो रहे थे कि किसी ने दोस्ताना लहजे में मुझे पुकारा, “जा’फ़र! जा’फ़र!”
मैंने मुड़ कर देख तो एक मुअ’म्मर शख़्स खड़ा था। इसकी सफ़ेद लंबी सी दाढ़ी ने उसे निहायत क़ाबिल-ए-ता’ज़ीम बना दिया था। उसकी आँखें भूरी थीं और बाल रूई के गाले की तरह सफ़ेद, और इस क़दर लंबे थे कि कंधों को छुपा रहे थे। पहले-पहले तो मैं कुछ डर सा गया क्योंकि मेरा हाफ़िज़ा काम नहीं करता था। मुझे कभी ख़्वाब में भी उस शख़्स की सूरत नज़र न आई थी, मगर थोड़ी देर बा’द हम किसी क़िस्म की बे-तकल्लुफ़ी से बातें करने लगे। लोग जल्द-जल्द क़दम उठाते सड़क पर से गुज़र रहे थे मगर हम दोनों निहायत इत्मीनान से आहिस्ता-आहिस्ता बातें करते हुए अभी-अभी क़ब्रिस्तान की सरहद से निकले थे और एक सुनसान सड़क पर चले जा थे।
“जनाब मुझे याद नहीं पड़ता... जनाब का नाम?”
“फ़वाद।”
“फ़वाद?”
मैंने दोहराया, “फ़वाद? अच्छा... तुम्हारे ख़ानदान में कोई डाक्टर गुज़रा है?”
“क्यों?”
“नहीं तुमको बताना पड़ेगा”, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, “बताओ कोई डाक्टर भी था?”
बूढ़ा मुस्कुराया, “नौजवान आदमी मज़बूत और ताक़तवर हो कर एक बूढ़े शख़्स से इस क़दर क्यों वहशत-ज़दा होते हो।”
मैंने क़द्र-ए-बेपर्वाई से कहा, “मैं डरा नहीं हूँ। हाँ मुतअ’ज्जिब ज़रूर हूँ।”
बूढ़ा फ़वाद मुस्कुराया, “तुम्हारी हैरत बजा है क्योंकि मुझे तुमसे कभी मिलने का इत्तिफ़ाक़ नहीं हुआ। मगर शायद तुम्हें याद हो तीन साल पहले पहली दफ़ा’ मैंने तुम्हें दमिश्क़ के एक बाज़ार में देखा था। फिर एक दफ़ा’ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते भी देखा, इस वाक़िए’ को आज तीन साल का अ’र्सा गुज़र गया है।”
मैं किसी क़दर बेचैन हो गया, “मुझे कुछ याद नहीं, मुम्किन है कि आपने मुझे देखा हो। आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपके ख़ानदान में कोई डाक्टर भी गुज़रा है?”
बूढ़ा फ़वाद मुस्कुराया, “मुझे कुछ याद नहीं तुम बार-बार मुझसे ये सवाल क्यों करते हो? हाँ तुम ये बताओ तुम दमिश्क़ में भी रह चुके हो ना?”
मुझे ये सवाल बहुत ना-गवार गुज़रा। चंद साल से मुझे सवाल के नाम से नफ़रत और दहशत पैदा हो जाती थी। मैंने निहायत ख़ुश्क लहजे में कहा, “जनाब मैं इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि मुझे इस गुफ़्तगू से किसी क़िस्म की दिलचस्पी नहीं।”
फ़वाद हँस पड़ा, “वल्लाह तुम भी अ’जब वहशत-पसंद हो। मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हें तीन साल हुए दमिश्क़ के बाज़ार में देखा था।”
मैं अब ज़ब्त न कर सका, “अजी हज़रत, उठा रखिए, देखा होगा आपने मुझे कहीं। अब बार-बार ज़िक्र करने की क्या ज़रूरत है?”
बूढ़ा फ़वाद बड़े मीठे लहजे में कहने लगा, “और उसी वक़्त से मुझे तुमसे मुहब्बत हो गई।”
“वज्ह?”
फ़वाद मुस्कुराया, “नौजवान आदमी तुम तो मुहब्बत की वज्ह अदालती लहजे में दरियाफ़्त करते हो!”
मैं अपनी पहली वहशत पर पछताया।
“मुआ’फ़ कीजिए, लेकिन आख़िर मुझ अजनबी से मुहब्बत करने का सबब?”
“मुहब्बत के अस्बाब क्या होते हैं। ये तो कोई बता ही नहीं सकता। मगर ख़ुश-अख़्लाक़ी, ख़ूबसूरती, शीरीं-बयानी भी इंसान को इंसान का गिरवीदा कर देती...”
मैं बोल उठा, “मगर मेरा ख़याल है कि इन आ’ला सिफ़ात में से एक भी मुझमें मौजूद नहीं!”
फ़वाद ने मुझ पर एक सरसरी नज़र डालते हुए कहा, “नौजवान शख़्स, इंसान अपने अख़्लाक़ का आप नक़्क़ाद नहीं हो सकता। ये ग़लती है। मुम्किन है कि तुम में और औसाफ़ न हों मगर एक हक़ीक़त तुम में बिल्कुल नुमायाँ है और वो तुम्हारा बे-नज़ीर हुस्न है। अगरचे अब मैं उस उ’म्र को पहुँच गया हूँ कि किसी के हुस्न से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकता मगर (मुस्कुरा कर) शायद तुम्हें हैरत हो कि अब भी मैं हुस्न-परस्त हूँ। जवानी के आ’लम में मैं उ’मर ख़य्याम की रूबाईयात गाया करता था जो हुस्न और शराब की तारी’फ़ में लिखी गई हैं।”
मुझे एक ख़याल ने चौंका दिया। मैंने अपने मज़बूत हाथों को क़द्र-ए-नफ़रत से देखा और निहायत हिक़ारत से कहने लगा, “मैं हसीन हूँ? हुस्न? तुफ़ है ऐसे हुस्न पर, ला’नत जो किसी को मुसख़्ख़र न कर सके। मैं ख़ूबसूरत हूँ? ग़लत है। जनाब मुझे कहने दीजिए कि ग़लत है। अगर मैं हसीन ही होता तो आज किसी की निगाह-ए-इंतिख़ाब “दूसरे” पर क्यों पड़ती?”
“ओ-हो…!”, फ़वाद चौंक पड़ा, “मा’लूम होता है कि किसी ने तुमसे बेवफ़ाई की है। भई रंज न करो। औ’रतें ऐसी ही होती हैं।”
मैं चिल्ला उठा, “मुझे औ’रत के नाम से नफ़रत है मुहब्बत के नाम से हैबत और वहशत है!”
फ़वाद ने एक सर्द आह खींची, “ठीक! दुनिया की जन्नत कहो या दोज़ख़ औ’रत और मुहब्बत ही के दो मुख़्तलिफ़ नाम हैं!”
मैंने इल्तिजा के पैराया में कहा, “ख़ुदा के लिए अब इस तज़्किरे को जाने भी दो। मेरे आगे औ’रत का नाम न लो। हाँ ये तो कहो कि तुमने इससे पहले मुझसे तआ’रुफ़ क्यों न पैदा कर लिया? तीन साल की तवील मुद्दत हमको वफ़ादार दोस्त बनाने के लिए काफ़ी थी। (थोड़ी देर बा’द) शायद तुमने पर्वा न की।”
“क्यों नहीं? ये तो मेरी ऐ’न तमन्ना थी कि तुमसे तआ’रुफ़ पैदा कर लूँ।”, फ़वाद ने जवाब दिया।
“तो फिर…”, मैं कहने लगा, “तो फिर रुकावट ही क्या थी? मैं यक़ीनन कोई सियासी क़ैदी या जासूस नहीं था कि मुझसे मिलने मैं तुम्हें दिक़्क़तें पेश आतीं।”
“ये तो सच है।”, बूढ़ा कहने लगा कि, “तुमसे बा-आसानी मिल सकता था मगर हज़रत दमिश्क़ से आप ऐसे ग़ाइब हुए कि कहीं पता न लगा। अक्सर महफ़िलों, जलसों में मेरी मुश्ताक़ नज़रें तुमको ढूँढा करती थीं। तुम आख़िर किधर चले गए थे? मिस्र? अफ़्रीक़ा? हिन्दोस्तान?”
मैं किसी क़दर बेचैन हो गया, “हाँ... मैं बाहर चला गया था।”
“क्या तीन साल से यहीं हो?”
मेरा इज़्तिरार बढ़ता गया। मेरा साँस फूलने लगा। दिल चाहता था कि किसी तरफ़ को भाग जाऊँ। मजबूरन जवाब दिया, “ठीक है सिर्फ़ इन्हीं तीन ममालिक पर क्या मुनहसिर है, बग़दाद, बसरा, शाम वग़ैरह भी गया था।”
“शायद तिजारती सिलसिले में? अब मुस्तक़िल सुकूनत कहाँ इख़्तियार की है?”
मैं हिक़ारत से मुस्कुराने लगा। नहीं नहीं आह।।
सब अहल-ए-मकाँ मुझसे मकाँ पूछ रहे हैं
ग़ुर्बत-ज़दा, आवारा, पता दूँ मैं कहाँ का
मेरा दिल बे-क़रार हो गया। गुज़िश्ता अलम-नाक वाक़िआ’त यके-बा’द-दीगरे याद आने लगे और मेरी आँखों में आँसू चमक उठे। थोड़ी देर हम ख़ामोश रहे। आहिस्ता-आहिस्ता क़दम उठाते हुए उस तंग रास्ते से गुज़र रहे थे। शाम गर्म थी और क़ब्रिस्तान का रास्ता वीरान हो गया था। कोई राहगीर नज़र न आता था। सनोबर और देवदार के तनावर दरख़्तों के पत्तों में हुआ साँय-साँय करती चल रही थी।
हर तरफ़ मौत की सी ख़ामोशी थी। हाँ कभी-कभी कोई यूनानी बुलबुल किसी दूर के ख़शख़ाश के दरख़्त पर बैठी ज़ोर से सीटी बजा दिया करती थी। मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया तो तबीअ’त को बहलाने के लिए मैंने बातें शुरू’ कर दीं। अगरचे फ़ुज़ूल बातें।
“मरहूम को क्या बीमारी थी?”, मुझे क्या ख़बर थी कि इस सवाल के साथ ही एक अ’जीब-ओ-ग़रीब गुफ़्तगू का सिलसिला छिड़ जाएगा जो मेरे शीराज़-ए-ज़िंदगी को ही बिखेर देगा।
फ़वाद कहने लगा, “जो शख़्स आज मरा है, वो शहर का निहायत मो’तबर और मुअ’ज़्ज़िज़ ताजिर था। ख़ुदा ग़रीक़-ए-रहमत करे मरहूम को, जिसकी आ जाती है वो हर बहाने से जाता है। उसे क्या था? सिर्फ़ दो दिन का बुख़ार था, भला-चंगा आदमी था। देखो मियाँ मौत कैसी अंधी होती है कि पीर-ओ-जवान को नहीं देखती।”
मुझे बचपन ही से मौत के नाम से वहशत थी। मैंने निहायत बे-क़रारी से पूछा, “क्या मौत ऐसी ज़ालिम होती है?”
मैंने गर्दन झुका ली। रास्ता और भी वीरान होता गया।
फ़वाद कहता रहा, “ज़िंदगानी का ए’तिबार ही क्या? फिर भी लोग मौत को भूले हुए हैं। गुनाह करते हैं, चोरी, क़िमार-बाज़ी, झूट।”
मुझे ग़ुस्सा आ गया। मैं कह चुका हूँ कि जब से जैरूस आया था, एक दीवानगी की सी कैफ़ियत महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे अंदरूनी जज़्बात और सदमात मुझे हमेशा मुतवहि्ह्श रखते थे। मैं बे-साख़्ता बोल उठा, “गुनाह सभी करते हैं, इससे तो ख़ुद आप भी बरी नहीं।”
“बे-शक नहीं!”, फ़वाद मुस्कुरा कर बोला, “मगर ख़ुदा अ’लीम है कि मैंने कभी चोरी नहीं की। कभी किसी से दग़ा-बाज़ी नहीं की। किसी को धोका नहीं दिया। ई’साईयों और यहूदियों की तरह शराब नहीं पी, मगर सोचो लोग आए दिन कैसे जैसे जुर्म करते हैं!”
“जुर्म?”
जुर्म के नाम ही से मेरा ख़ून ख़ुश्क होता था। मुझे इस नाम से वहशत थी। मैं चिल्ला उठा, “ख़ुदा के लिए ख़ामोश रहो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता!”
फ़वाद ज़ियादा पुर-असरार नज़र आने लगा। बोला, “तुम अभी कमसिन हो नौजवान दोस्त! जुर्म के नाम से ही वहशत-ज़दा हो गए? मगर ख़याल करो कि लोग किस बेबाकी से जुर्म के मुर्तक़िब होते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक दूसरे को ज़ख़्मी करते हैं और बा’ज़ तो क़त्ल भी करते हैं।”
मेरे मुँह से एक चीख़ निकल गई।
“क़त्ल?”
मैं लरज़ गया।
“उफ़ क़त्ल?”
मैं बहुत देर तक काँपता रहा। फिर आ’लम-ए-बे-इख़्तियार में चीख़ें निकल निकल गईं।
“बूढ़े आदमी क़त्ल? लोग क़त्ल भी करते हैं...? तो... तो इसकी सज़ा क्या मिलती है?”
“ख़ून का बदला ख़ून... ये मज़हब का हुक्म है।”
फ़वाद ने एक अ’जीब हिक़ारत-आमेज़ तबस्सुम के साथ कहा। मैं अब तक अपने होश में न था।
“उफ़ उफ़... बुलंद आसमान! चुप रहो! चुप रहो!”
मैंने फ़वाद के कंधों को पकड़ लिया और क़ब्रिस्तान के आसेब-ज़दा दरख़्तों के सायों से निकल कर जल्दी से एक तंग रास्ते पर ले आया। सूरज बिल्कुल डूब चुका था और तारीकी फैल रही थी। शाम की मनहूस चिड़ियाँ वीरान रास्तों पर चीख़ें मार थीं।
बूढ़े फ़वाद ने ख़ौफ़ से काँप कर कहा, “बेटा तुम तो पागल मा’लूम होते हो, मज़हब का यही हुक्म है। मगर अब क़ातिल कहाँ मिलते हैं? उनका सुराग़ कौन लगाता है? अ’दालतें हैं मगर इन्साफ़ मफ़क़ूद!”
मैं मुस्कुराया, “तो फिर आजकल के क़ातिल यूँही छोड़ दिए जाते हैं?”
(हँसकर)
“ख़ूब क़त्ल करो और ज़िंदा रहो! ज़िंदगी के मज़े लूटो, ख़ूब!”
फ़वाद ने निहायत जोशीले लहजे में कहा, “नहीं मियाँ नहीं, ऐसा मत समझो। अ’दालत पर ख़ाक डालो। यहाँ की अ’दालत क़ातिल को न पहचान सके तो क्या हुआ...? परवरदिगार मौजूद है और उसकी ताक़त मौजूद... वो एक ऐसी ज़बरदस्त ताक़त है जो हर मुजरिम को उसकी सज़ा को पहुँचाता है।”
“वो किस तरह?”, मैंने सवाल किया।
वो कहने लगा, “मैंने हाल ही में एक मुसन्निफ़... एक पुराने मुसन्निफ़ का क़िस्सा पढ़ा।”
“उसमें क्या लिखा है भला?”
मैंने शौक़ ज़ाहिर किया। वो निहायत आ’लिमाना लहजे में कहने लगा, “उसमें लिखा है कि क़ातिल पोशीदा नहीं रह सकता। छिपा हुआ क़ातिल नीचे की तरफ़ से पकड़ा जाता है। और...”
मैंने क़त्अ’-ए-कलाम किया, “उफ़! ज़ालिम झूटे हो तुम!”
“मैं झूट नहीं बोलता!”
मैंने कुछ सोच कर सवाल किया, “बोलो। तुम्हारे ख़ानदान में कोई डाक्टर भी गुज़रा है?”
“मुझे ख़बर नहीं!”
“तो ख़ैर... अच्छा कहो कि छिपा हुआ क़ातिल किस तरह पकड़ा जाता है।”
उसने फिर गुफ़्तगू शुरू’ की, “सुनो उस किताब में लिखा है कि एक क़ातिल तीन साल, तीन माह, तीन दिन के अंदर ही अंदर अपने जुर्म का इक़बाल कर लेता है।”
“क्यों कर लेता है?”, मैंने निहायत बेचैनी और हैरत से पूछा।
“उसे करना पड़ता है। वो ज़रूर करेगा। कर चुका है। बहुत से क़ातिलों ने कर लिया। तीन साल तीन माह, तीन दिन अगरचे वो अ’दालत में झूट बोलता है, इन्साफ़ की आँखों में ख़ाक डालता है। क़ानूनी मुशीरों को रिश्वत दे देकर उन्हें काठ की पुतलियाँ बना छोड़ता है। ताहम... ताहम... इक मज़बूत ताक़त उसे मजबूर करती है कि वो... वो अपने जुर्म का इक़बाल कर ले।”
“वो क्या ताक़त है?”, मेरे मुँह से एक चीख़ निकल गई।
“ज़मीर... मा’मूली लफ़्ज़ है। हर लुग़त में मौजूद!!”
मैं बुत बन गया था, “क्या ज़मीर हर इंसान में मौजूद होता है?”
फ़वाद मुस्कुराया, “मेरा तो ख़याल है कि हैवान में भी ज़मीर मौजूद है, जभी तो पालतू कुत्ता भी मालिक के हाँ चोरी नहीं करता।”
“तो फिर मुझमें भी... ज़मीर की बला मौजूद है?”
फ़वाद मुतअ’ज्जिब हुआ, “हाँ यक़ीनन जब कि तुम इंसान हो। मगर तुम इसे बला कहते हो भले आदमी?”
मैं कोई जवाब न दे सका मगर पूछा, “तुमने किस किताब में ये बातें पढ़ीं?”
“एक पुराने मुसन्निफ़ की किताब में। हाँ तीन साल... इस अस्ना में क़ातिल की मौत वाक़े’ हो जाती है। ख़्वाह किसी बहाने से, वबा से, बुख़ार से या फिर अ’दालत की तरफ़ से। कुछ नहीं तो ज़मीर ख़ुद उसे ख़ुदकुशी की तरग़ीब देता है। उसे मजबूर करता है।”
“तुम पर ला’नत हो, ला’नत!”, मैंने नफ़रत-अंगेज़ लहजे में कहा।
मेरा ख़ून मेरी रगों में दौड़ने लगा। मेरा सर चकराने लगा। कहीं मुझे ग़श तो नहीं आ रहा? एक अ’जीब जुनून की सी कैफ़ियत में मैंने अपने घर की राह ली और रास्ते भर यही सोचता गया कि कहीं फ़वाद डाक्टर रुश्दी का कोई रिश्तेदार तो नहीं, मैं बे-तहाशा अपने कमरे में भागा।
(बाब - 2)
मुहब्बत या हलाकत
मेरी मौत थी राज़-ए-उलफ़त के साथ
रहा ज़ब्त आख़िर गला घोंट कर
जब मैं वापिस अपने कमरे में आया तो तारीकी बढ़ रही थी। ज़िंदगी की तमाम क़ुव्वतें जिस तरह मौत के वक़्त सल्ब हो जाती हैं, उसी तरह दिन की रौशनियाँ मग़रिब में गुम होती जाती हैं। गर्म मौसम की शफ़क़ की गहरी सुर्ख़ी कमरे की ऊँची-ऊँची सफ़ेद दीवारों को रंगीन कर रही थी। ऐसा मा’लूम होता था जैसे कि किसी मक़्तूल के ताज़ा गर्म ख़ून के छींटे हैं। मेरे मिज़ाज में सौदा समा गया। आ’लम-ए-वहशत में भागा-भागा कमरे के आख़िरी हिस्से में गया। मेज़ पर एक आईना पड़ा था, उसमें अपनी शक्ल देखकर मुँह से बे-तहाशा चीख़ें गईं।
“आह वो मेरी अगली हसीन सूरत किधर ग़ाइब हो गई थी? वो शगुफ़्ता रुख़्सार सुर्ख़ लब क्या हो गए?” आईना देखकर मैं लरज़ गया... सुर्ख़ अंगारों की सी आँखें, गले की रगें उभरी हुई, चेहरा तमतमाया हुआ। इस पर ग़ज़ब ये कि ख़ुद-ब-ख़ुद एक ना-मा’लूम तरीक़ पर मेरी मुट्ठियाँ मज़बूती से बंद हुई जाती थीं। मैं आ’लम-ए-वहशत में नौकर को चीख़-चीख़ कर आवाज़ें देने लगा। ज़ोर से चीख़ा। ऐसी बुलंद आवाज़ से कि दर-ओ-दीवार लरज़ गए! उफ़ वहशत!
“हुज़ूर”, नौकर ने कमरे में आकर जवाब दिया।
“दोस्त, एक छुरी तो लाओ... एक तेज़ छुरी... छुरा... जल्दी करो, जल्दी करो।”
वो सहम गया, “हुज़ूर…!”
“बे-वक़ूफ़”, मैं चिल्ला उठा, “ज़ियादा मत बको! जाओ भागो तुमने लंबा सा कुर्ता पहन रखा है। इसके नीचे... चमकदार... लंबी सी तेज़ छुरी ले आओ...”
उधर वो कमरे से बाहर निकल गया। उधर मैंने नेकटाई खोल कर फेंक दी। कोट उतार दिया। छुरी के इंतिज़ार में लंबे-लंबे क़दम डालता टहलने लगा... यका-य़क चौंक पड़ा। कहीं वो मेरे मजनूनाना हरकात की इत्तिला पुलिस को न दे। इस ख़याल के आते ही कमरे से बाहर निकला, देखा तो वाक़ई’ वो ज़ीना तय कर रहा था। मैंने पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया और साथ ले आया और एक कमरे में डाल कर कमरा मुक़फ़्फ़ल कर दिया। इस कार्रवाई के बा’द मैं निहायत इत्मीनान से अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुर्सी खींची और मेज़ पर बैठ गया और अपनी इ’बरत-अंगेज़... मुख़्तसर ज़िंदगी के हालात लोगों की इ’बरत के लिए निहायत जल्दी-जल्दी एक काग़ज़ पर लिखने लगा।
(बाब - 3)
बेरूत
अभी कमसिन हो रहने दो, कहीं खो दोगे दिल मेरा
तुम्हारे ही लिए रक्खा है ले लेना जवाँ हो कर
बेरूत मेरे चचा की लड़की थी, जिसे उनके वालिदैन के इंतिक़ाल के बा’द मेरे वालिदैन ने अपने साया-ए-आ’तिफ़त में ले लिया था। वो शाम मुझे कभी न भूलेगी जब कि छोटी बेरूत पहली मर्तबा अपने वालिदैन के इंतिक़ाल के बा’द हमारे पास अपनी अन्ना के साथ हमेशा के लिए आ गई थी।
चूँकि अम्माँ-जान को लड़कियाँ बहुत पसंद थीं और उनके कोई लड़की न थी, इसलिए उन्होंने बेरूत को एक अ’तिय्या-ए-इलाही समझ कर उसकी परस्तिश शुरू’ कर दी। उनकी मुहब्बत बेरूत से कुछ इस क़दर बढ़ी हुई थी कि बाज़-औक़ात मुझे रश्क होता था। अब्बा जान भी उस पर फ़रेफ़्ता थे। एक तो भतीजी, उस पर मरहूम भाई की निशानी। जितना भी चाहें कम।
एक इन्हीं दोनों पर क्या मुनहसिर है। बेरूत का हुस्न उसकी हर दिल-अ’ज़ीज़ी का सबब था। बच्चा, बूढ़ा, अपना, पराया, सभी उसके गिरवीदा थे। अम्माँ-जान से उनकी सहेलियाँ मिलने आती थीं तो बेरूत को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थीं। ग़रज़ बेरूत बहुत जल्द हमारे ख़ानदान में घुल मिल गई। वो महल में एक बुलबुल की तरह चहचहाती फिरती थी और हर शख़्स उसके नाज़ उठाने को तैयार नज़र आता था। वो मुझसे दो साल छोटी थी और हम दोनों में बेहद मिलाप था!
अब हम दोनों की ता’लीम-ओ-तरबियत का ज़माना शुरू’ हो गया था। अब्बा जान ने हम दोनों को स्कूल में दाख़िल करा दिया। घर पर भी हमारे लिए अतालीक़ मुक़र्रर किए गए। बेरूत के लिए एक और उस्ताद भी मुक़र्रर किया गया जो हफ़्ते में दो मर्तबा उसे मौसीक़ी के सबक़ दिया करता था। ये हुआ ता’लीम का इंतिज़ाम।
इधर हमारी तरबियत के लिए अम्माँ-जान ही क्या कम थीं, इस फिर दो फ़्रांसीसी गवर्नसें भी मुक़र्रर की गईं। एक मिस्री मौलवी-साहब भी थे जो ख़ास मज़हबी बातों के लिए मुक़र्रर किए गए थे। इन तमाम बातों का ख़ुश-गवार नतीजा ये हुआ कि हम तरक़्क़ी करने लगे। बेरूत तो आठ साल की उ’म्र ही से फ़्रांसीसी ज़बान ऐसी शुस्ता और ख़ुश-लहजे में बोला करती थी, जैसे वो अपनी मादरी ज़बान फ़ारसी या अ’रबी बोलती थी। उसने “मुक़द्दस किताब” की कई दुआ’एँ याद कर ली थीं। सितार वो निहायत उ’म्दगी से बजाया करती थी।
ग़रज़ दिन गुज़रते गए। अब बचपन की मंज़िल तय कर के हम आहिस्ता-आहिस्ता लड़कपन के ज़ीने पर क़दम रख रहे थे। बेरूत को उसी महीने तेरहवाँ साल लगा था और अब तो वो इस क़दर तरक़्क़ी कर गई थी कि लोग अ’श-अ’श कर रहे थे, मगर अभी वो बच्चा ही थी, उसे अभी बहुत कुछ सीखना था।
हरम-सरा में अम्माँ-जान का एक निहायत ख़ूबसूरत मुलाक़ाती कमरा था, जिसके आगे सुर्ख़ गुलाब और चम्बेली का बाग़ीचा लगा था। गरमियों की एक सुब्ह में गर्मी से परेशान हो कर अपने कमरे से बाहर निकाला और अम्माँ-जान के पाईं-बाग़ में बेरूत को ढूँढता हुआ चला गया, मगर बेरूत वहाँ नहीं थी। अम्माँ-जान अपने कमरा-ए-मुलाक़ात में थीं और उधर से बहुत सी ख़वातीन के हँसने बोलने की सुरीली आवाज़ें आ रही थीं। उस कमरे के दरवाज़ों पर हरी-हरी चिलमनें पड़ी थीं। कभी-कभी कनीज़ें जल्द-जल्द कमरे से बाहर निकलती हुई और वापिस जाती नज़र थीं।
मुझे हैरत थी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगरचे मैं अभी पंद्रह साला बच्चा ही था, ताहम मुझे ख़वातीन से बड़ी झिझक मा’लूम होती थी। मैं दबे-पाँव ज़ीने तय कर के एक दरीचे के पास गया और झाँकने लगा मगर में कुछ न देख सका सिवाए इसके कि बहुत सी औ’रतें किसी एक चीज़ को घेरे हुए थीं और निहायत मसरूर मा’लूम होती थीं। वो सब मुसल्लम सिंगार किए हुए थीं। आँखों में सुर्मा लगा हुआ था। नाख़ुनों पर हिना का रंग चढ़ा हुआ था और सियाह रेशमी रूमाल सब के सरों पर लिपटे हुए थे। गर्दनों पर संदल भी लगाया गया था, जिसे मशरिक़ी औ’रतें ख़ुशी के मौक़ों’ पर इस्ति’माल करती हैं।
या अल्लाह! ये क्या माजरा है! मैं सख़्त परेशान हो गया। उसी वक़्त एक बूढ़ी और पुरानी हब्शन ख़ादिमा बाहर निकल आई। मैंने उससे सवाल किया, “ज़ैनब! यहाँ क्या हो रहा है? बेरूत कहाँ है
बूढ़ी हब्शन बहुत ही मसरूर नज़र आ रही थी। बिगड़ी हुई अ’रबी में बोली, “तुम अंदर जा सकते हो! कोई तुमसे पर्दा न करेगा। अभी तुम बच्चे हो।”
ये कह कर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मगर मैं उड़ गया।
“कभी नहीं मैं अंदर जाऊँगा मेरा हाथ छोड़ दो। यहाँ क्या हो रहा है? बेरूत को बुला दो…”
वो अपनी भद्दी आवाज़ में हँसने लगी, “साहब-ज़ादे अब तुम्हारी बहन यहाँ न आएगी।”
“यहाँ न आएगी क्यों?”, मैंने मुतहय्यर हो कर पूछा।
“वो ग़ुलामों और दूसरे मर्द ख़िदमत-गारों की मौजूदगी में यहाँ नहीं आ सकेंगी।”
उसके जवाब ने मुझे और भी मुतअ’ज्जिब कर दिया। मुझे ग़ुस्सा आ गया। पूछा, “ओ तुम बूढ़ी लोमड़ी मज़ाक़ करती हो मुझसे? क्या ग़ुलाम और दूसरे मर्द ख़िदमत-गार उसे खा लेंगे?”
बूढ़ी हब्शन ने कोई जवाब नहीं दिया और चोबे मलीदे का एक बड़ा तबाक़ उठा कर अंदर चली गई और मैं परेशान बरामदे में टहलता रहा। थोड़ी देर बा’द मेरी छोटी चची बाहर निकल आईं। उन्होंने मुझे पुकारा, “आओ... शर्बत पियो...”
“बेरूत कहाँ है?” मैंने सवाल किया। वो मुस्कुराईं। सब्ज़ लिबास में वो एक परी मा’लूम होती थीं। बोलीं, “वो अंदर है।”
“तो उसे यहाँ भेज दीजिए।”, मैंने इल्तिजा की।
उनके रुख़्सार जगमगाने लगे, “वो यहाँ नहीं आ सकतीं।”
“क्यों? क्या बीमार हैं? और ये सब औ’रतें क्यों आई हैं?”
“तुम्हारी शादी होगी।”, चची ने हस्ब-ए-मा’मूल मज़ाक़ शुरू’ कर दिया। वो बड़ी चुलबुली औ’रत थीं।
“जा’फ़र की शादी हो रही है और हम सब के सब शरीक हैं।”
“लिल्लाह चची…”, मैंने तंग आकर कहा, “मुझे परेशान न कीजिए और फ़रमाइए कि क्या हो रहा है। बेरूत को आप लोगों ने क्यों पकड़ रखा है?”
चची शीरीं ज़ोर से हँसने लगीं, “बच्चे तेरी बहन ने आज पहली दफ़ा’ निक़ाब पहनी है। इसी की ख़ुशी में सबकी दा’वत है, ख़वातीन की। मैं तुम्हारी माँ के बुलावे पर सुब्ह से आई हुई हूँ। बेरूत अब मर्दों के आगे बे-नक़ाब नहीं आएगी। ये है।”
ये सुनकर मेरा सर चकरा गया, “आह वो औ’रत बन गई! अब वो क़ैदियों की सी ज़िंदगी बसर करेगी!हरम-सरा की ऊँची-ऊँची दीवारों में मुक़य्यद कर दी जाएगी। अम्मी जान और कुन्बे की दूसरी ख़वातीन की तरह सियाह रूमाल से अपने बाल और निस्फ़ चेहरा छुपाएगी। आह! आह मेरे साथ बाग़ों में कूदती न फिरेगी! हुक्म है। ये हुक्म है पर्दा... औ’रतों पर ज़ुल्म है। ये रस्म तो बूढ़ियों के लिए मख़्सूस होनी चाहिए ना कि लड़कीयों के लिए।”
चची शीरीं हँस पड़ीं, “तुम बड़े बे-वक़ूफ़ हो। क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों की तरह और ई’साईयों के मानिंद तुम्हारी बहन मारी मारी गलियों में फिरा करे।”
इन बातों पर बहस करने के लिए मैं बहुत छोटा था। मैं घबरा कर अपने कमरे में भाग गया और दरीचे के पास एक कोच पर लेट कर रोने लगा। बेरूत आज़ादी का नौहा!
आज़ादियाँ कहाँ वो बचपन की थी वो बातें
अपनी ख़ुशी से आना, अपनी ख़ुशी से जाना
ख़ुदा जाने मैं कितनी देर रोता रहा कि घड़ियाल ने आठ बजा दिए। देखा तो धूप शीशे के दरीचों और दरवाज़ों में से छन-छन कर अंदर आ रही है और कमरा जगमगा रहा है। दफ़अ’तन मेरी नज़र दरीचे की तरफ़ उठी। देखा कि अम्माँ-जान और चची बरामदे में से गुज़र रही हैं और उनके साथ सियाह रेशमी और लंबी चादरों में लिपटी हुई एक लड़की चुप-चाप चली जा रही है। मैं दो लम्हे ग़ौर से देखता रहा फिर समझ गया कि यही मेरी बहन बेरूत है! आह! मेरी बेरूत! वो आज किन मसाइब में गिरफ़्तार है।
मैं उठ खड़ा हुआ और दबे-पाँव अम्माँ-जान और चची के साथ-साथ गया। वो लोग बेरूत को लेकर उसके कमरे में दाख़िल हो गए और मैं कमरे की दीवार के पीछे खड़ा हो गया और झाँकने लगा।
“जा’फ़र”, मेरी माँ की आवाज़ थी।
“जी...?”
“अंदर आओ बेटा! अंदर कोई नहीं है। अंदर चले आओ प्यारे।”
मैं डरते-डरते बेरूत के कमरे का सब्ज़ पर्दा हटा कर अंदर दाख़िल हुआ। कमरे में ऊ’द-ओ-अ’बीर की बू फैली हुई थी। बेरूत एक मख़मली सोफ़े पर बैठी हुई थी। एक छोटी सी दरीची में से सूरज की तेज़ और गर्म
शुआएँ उस पर पड़ रही थी। वो बिल्कुल एक गुड़िया मा’लूम होती थी। उसका निस्फ़ चेहरा बारीक जाली के सियाह निक़ाब में छिपा हुआ था। सिर्फ़ उसकी आँखें और पेशानी मुझे नज़र आ रही थी। उसके लंबे सियाह बाल चादर में से हो कर नीचे क़ालीन पर कुछ-कुछ लटक रहे थे। वो उस वक़्त एक मग़रूर सुल्ताना की तरह बैठी ज़मीन को देख रही थी और ब-ज़ाहिर बहुत ख़ुश-नज़र आती थी। उसे इसका एहसास न था कि उसकी आज़ादी सल्ब कर ली गई है।
अम्माँ-जान उस वक़्त एक सफ़ेद रेशम का ख़ूबसूरत लिबास पहने हुए थीं। उनका चेहरा मसर्रत के सबब सुर्ख़ हो रहा था। वो हँसकर बोलीं, “तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ अब बाहर नाचती न फिरेगी।”
मैं कुछ न बोल सका। मैंने दरवाज़ा खोला और जल्दी से बाहर निकल गया।
(बाब - 4)
चाह का नाम जब आता है बिगड़ जाते हो
वो तरीक़ा तो बता दो तुम्हें चाहें क्योंकर
इन वाक़िआ’त को पाँच साल का अ’र्सा गुज़र गया। अगरचे अब हम बच्चे न रहे थे मगर हमारे तअ’ल्लुक़ात में किसी क़िस्म का फ़र्क़ नहीं आया था। हम दोनों अब भी दिन-भर दार-उल-मुताला’ में बैठे अपने इ’ल्मी मशाग़िल में मसरूफ़ रहते। बड़े-बड़े मुसन्निफ़ीन के अफ़साने, मशहूर-मशहूर शो’रा की नज़्में पढ़ा करते। इस पुर-लुत्फ़ सिलसिले और इख़्तिलात-ए-बाहमी का नतीजा ये हुआ कि हमारी ज़िंदगी पर मुहब्बत की ख़ामोश मगर ज़बरदस्त ताक़त ने असर डालना शुरू’ कर दिया और हम दोनों बहुत जल्द एक दूसरे पर फ़रेफ़्ता हो गए। जब हम दोनों बाग़ में जाते तो चिड़ियों के ख़ूबसूरत लहजे ऐ’न मुहब्बत के सुरीले और मीठे सुर मा’लूम होते थे। कैसा पर-लुत्फ़ ज़माना था।
सुब्ह-ए-इ’शरत के मज़े, शाम-ए-मुहब्बत के मज़े
उन दिनों कुछ और ही थे रंज-ओ-राहत के मज़े
बचपन के ज़माने में तो किसे ऐसी अ’क़्ल होती है कि किसी की मुहब्बत पर ग़ौर कर के पहचान सके कि ये मुहब्बत असली ह्यया नक़ली मगर जब मैं सन के मौसम-ए-बिहार मैं ऑक्सफ़ोर्ड से डिग्री लेकर वापिस आया तो चंद ही दिनों के तजुर्बे ने इस अलम-नाक राज़ का इन्किशाफ़ किया कि जिस शिद्दत की मुहब्बत मुझे सियाह चश्म बेरूत से है, उसे मुझसे नहीं। मुम्किन है ये मेरा ख़याल ही ख़याल हो। बेरूत मुझसे मुहब्बत ज़रूर करती थी क्योंकि उसके वो ख़ुतूत जो मुझे हर हफ़्ते ऑक्सफ़ोर्ड में पहुँचते थे, उसकी मुहब्बत के शाहिद हैं जो मेरे साथ थी मगर उसे वो इ’श्क़ न था जो मुझे उसके साथ था। अम्माँ जान को भी मेरे इस इ’श्क़ की ख़बर थी और एक उन्हीं पर क्या मुनहसिर है, सब जानते थे कि मुझे बेरूत से मुहब्बत है। मेरी मुहब्बत को भला मुहब्बत कौन कहता था। उसे सब दीवानगी या जुनून जैसे अल्फ़ाज़ में याद करते थे।
एक दफ़ा’ रात के खाने के बा’द हम सब के सब गाड़ियों में सैर को निकले। ग्यारह बजे के क़रीब वापिस आए। मैं बड़े हाल की एक फ़्रांसीसी खिड़की में खड़ा चाँद देख रहा था कि बेरूत मुझे “शब-ब-ख़ैर” कहने आ गई।
मैंने उसका हाथ थाम लिया, “बेरूत तुमको वो चाँद दिखाई दे रहा है? तुम ऐसी ही ख़ूबसूरत हो।”
वो हँसने लगी।
“मगर जा’फ़र!”, वो कहने लगी, “ऐसी चमक-दमक लेकर मैं क्या करूँगी? न भई, मुझे ये हरगिज़ गवारा नहीं कि मेरी गर्दन पर बजाए मेरे चेहरे के एक गोल और ज़र्द चाँद जगमगाए।”
मैंने मुस्कुराकर एक मुहब्बत-पाश नज़र डाली और निहायत आ’जिज़ी से बोला, “मैं सच कहता हूँ तुम मुझे ऐसी ही ख़ूबसूरत मा’लूम होती हो।
ये हुस्न ये आ’लम-ए-जवानी
यूसुफ़ का फ़साना इक कहानी
ये नर्म-ओ-सियाह ता-कमर बाल
हैं ताइर-ए-दिल के वास्ते जाल
ये फूल से सुर्ख़-सुर्ख़ रुख़्सार
फिर इस पर ग़ज़ब जमाल-ए-ख़ुद्दार
रफ़्तार बला की फ़ित्ना पर्वर
है जिसके तलामिज़ा में मह्शर
ये नर्गिस-ए-नीम-बाज़ आँखें
आफ़ाक़ में इंतिख़ाब आँखें
क़ामत वो कि सर्व पा-ब-गुल है
पामाल दम ख़िराम-ए-दिल है
आँखों से शराब है टपकती
सूरत से है सादगी बरसती
ग़ोश है प्यारे कुशादा
ढाता है ग़ज़ब ये हुस्न-ए-सादा
प्यारी बेरूत मैं सच कहता हूँ, मुझे तुमसे इ’श्क़ है।”
वो हँसकर बोली, “भई इ’श्क़ है तो रहने दो। मैं उसे क्या करूँ?”
मैं उसकी सादगी पर मुस्कुराया।
“बेरूत ऐसा सितम न करो! ऐसे ख़ुश्क जवाब न दिया करो। ब-ख़ुदा में इसका मुतहम्मिल नहीं! तुम मेरा मज़हका न उड़ाओ। अपने आ’शिक़ का मज़हका... !”
वो ज़ोर से हँस पड़ी, “आप आ’शिक़...?”
मैंने संजीदगी से कहा, “ख़ुदा के लिए बेरूत हँसी में न टालो। सच कहो मेरे मुतअ’ल्लिक़ तुम्हारा क्या ख़याल है?”
वो निहायत बे-पर्वाई से बोली, “तुम अच्छे लड़के हो।”
मैं चौंक पड़ा, “बस? अच्छा लड़का? बस इसी क़दर बेरूत?”
वो हँसी और बोली “तो क्या बुरा लड़का...? अच्छा यूँही सही।”
ये गुफ़्तगू यहीं ख़त्म हो गई मगर दूसरे दिन दोपहर के खाने की मेज़ पर मैं बहुत ही उदास पाया गया, क्योंकि मैं बेरूत से अपनी मुहब्बत का इक़रार करना चाहता था, मगर वो शरीर टाल जाती थी। मेज़ पर अम्माँ-जान ने मुझे ख़िलाफ़-ए-मा’मूल ख़ामोश देखकर अपनी छुरी और कांटा रकाबी में रख दिया और घबरा कर मुझसे पूछने लगीं, “प्यारे तुम बहुत ख़ामोश हो, मिज़ाज अच्छा है?”
इत्तिफ़ाक़ से चची शीरीं भी खाने पर आई हुई थीं। वो मेज़ के दूसरे सिरे पर थीं। वो शोख़ी से मुस्कुरा कर कहने लगीं :
हाय इस ज़ख़्मी-ए-शमशीर-ए-मुहब्बत का जिगर
दर्द को अपने जो नाचार छिपा रखा है
मेज़ पर अब्बा जान ग़ैर-हाज़िर थे। वो कहीं दा’वत में गए थे। सिर्फ़ हम चारों खाना खा रहे थे। अम्माँ-जान ने तो चची शीरीं के शे’र पर चंदाँ ग़ौर नहीं किया, मगर शरीर बेरूत ज़ोर से हँस पड़ी और मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया।
(बाब - 5)
बेरूत की अ’लालत और आग़ाज़-ए-मसीबत
कुछ और दिल-लगी नहीं उस ख़ुशनसीब से
हम जानते हैं खेलते हो तुम रक़ीब से
क्या ख़ूब राज़दार मिला है नसीब से
खुल खेले पर्दे-पर्दे में तुम तो रक़ीब से
इन्हीं अय्याम में एक दफ़ा’ शहर में कहीं शादी थी। हमारे हाँ की तमाम औ’रतें मदऊ’ थीं। अम्माँ-जान और बेरूत भी गई थीं। ये लोग दिन-भर वहीं रहे मगर जब शाम को दोनों वापिस आए तो बेरूत बेचैन और
मुज़्महिल नज़र आ रही थी। मैं उसकी ज़रा सी बे-कली पहचान जाता था और ख़ुद बे-कल हो जाता था। जूँही गाड़ी से अम्माँ-जान और वो उतरीं, मैंने उससे पूछा, “क्यों बेरूत कैसी तबीअ’त है? मुज़्महिल सी नज़र आती हो?”
“कुछ नहीं... कोई बात नहीं।”, ये कह कर वो अम्माँ-जान के साथ बड़े हाल में चली गई। अब्बा जान बड़े हाल में बैठे ”बग़दाद टाईम्स” पढ़ रहे थे। मैं भी वहीं आ गया और दरीचे के पास खड़ा हो गया। अम्माँ-जान दिन भरके वाक़िआ’त बड़े लुत्फ़ से अब्बा जान से कह रही थीं और वो सुन रहे थे। बेरूत ख़ामोश थी और एक कुर्सी पर लेटी थी।
“क्या बात है?”, अब्बा जान कहने लगे, “बेटी बेरूत! तुम बहुत सुस्त हो।”
ये कहते हुए इस पर झुके और उसका माथा छू कर कहने लगे, “उफ़्फ़ोह, बेरूत तो सख़्त बुख़ार में मुब्तला है।”
ये सुनकर अम्माँ-जान हवास-बाख़्ता बेरूत की तरफ़ आईं। मेरी परेशानी का तो ज़िक्र फ़ुज़ूल है। मैंने निहायत इज़्तिरार की हालत में पूछा, “अब्बा जान क्या किसी डाक्टर को टेलीफ़ोन करूँ?”
“बेहतर है कि डाक्टर रुश्दी को बुला लिया जाए।”, अब्बा जान ने जवाब दिया। इस अस्ना में अम्माँ-जान बेरूत को लेकर उसके कमरे में चली गईं थीं। अब शाम हो गई थी और हर तरफ़ अंधेरा छा रहा था। मैं टेलीफ़ोन
कर के डाक्टर के इंतिज़ार में बरामदे में टहल रहा था। इतने में डाक्टर रुश्दी की कार बरसाती में आकर रुकी। वो ख़ुश-रू नौजवान और बहुत ख़लीक़ आदमी मा’लूम होता था।
“क्या आप ही डाक्टर रुश्दी हैं?”, मैंने सवाल किया। उसने निहायत ख़लीक़ अंदाज़ में मुस्कुरा कर टोपी उठाई। मैं उसे लेकर बेरूत के कमरे में गया। अम्माँ-जान और अब्बा जान भी वहीं थे। बेरूत बिल्कुल निढाल नज़र आ रही थी और सफ़ेद बर्फ़ के से बिस्तर पर ज़र्द चम्बेली की कली की तरह पड़ी थी।
डाक्टर रुश्दी ने उसका मुआ’इना किया और तसल्ली दी कि मा’मूली बुख़ार है। कल तक तबीअ’त सँभल जाएगी। दूसरे दिन वाक़ई’ बुख़ार उतर गया, मगर तीसरे दिन ही वो यका-य़क बेहोश हो गई। डाक्टर रुश्दी की तशख़ीस ये हुई कि वो हिस्ट्रिया में मुब्तला हो गई है। इसके बा’द उसे ग़शी के दौरे पड़ने शुरू’ हुए और वो ख़तरनाक तौर पर इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गई। बा-क़ायदा इ’लाज शुरू’ हो गया। डाक्टर रुश्दी दिन में दो दफ़ा’ बिला-नाग़ा और कभी-कभी तीन दफ़ा’ आ जाया करते थे और मरीज़ा से उन्हें बेहद दिलचस्पी हो गई थी। कहना फ़ुज़ूल है कि मैंने बेरूत की बीमारी के ज़माने में उसकी ख़िदमत किस तरह की। दिन का चैन और रातों की नींद मुझ पर हराम थी।
तीन माह इस हालत में गुज़र गए। सबको बेरूत की ज़िंदगी से ना-उम्मीदी हो गई थी मगर बेरूत की ख़ुश-क़िस्मती से उसे डाक्टर ऐसा मिला था कि सर तोड़ कर कोशिश कर रहा था। इस पर तुर्रा ये कि तीमार-दार ऐसा था कि रात-दिन मरीज़ की पट्टी से लगा रहता था। सच पूछिए तो ख़ुदा की मेहरबानी के बा’द हम दोनों या’नी मेरी और रुश्दी की अनथक कोशिशों ने मरीज़ा को दूसरी ज़िंदगी बख़्शी थी। तक़दीर को तदबीर ने इस दफ़ा’ ख़ूब तमाशा दिखाया था। ये सवाल मुश्किल है कि इस बीमारी में डाक्टर रुश्दी ने ज़ियादा मेहनत की या मैंने। दोनों एक साथ नौटंकी करते रहते जिसका ख़ुश-गवार नतीजा ये था कि आज बेरूत ने ग़ुस्ल-ए-सेहत किया था।
अम्माँ-जान के लिए बेरूत की तंदुरुस्ती का दिन ई’द से ज़ियादा था। वो इसी ख़ुशी में नीचे दा’वत का इंतिज़ाम कर रही थीं, मगर मैं बेरूत के साथ ऊपर बाला-ख़ाने पर था। उसे चलने फिरने की अगरचे मुमानअ’त न थी मगर उसमें इतनी ताक़त ही न थी कि चल फिर सकती। डाक्टर अब तक दिन में दो मर्तबा आकर देखा करता था।
इतने में किसी ने दरवाज़ा आहिस्ता से खटखटाया ही था कि मैंने कहा, “डाक्टर रुश्दी होंगे तशरीफ़ लाइए।”
वो अंदर आया। उस वक़्त उसने हल्के ज़र्द रंगत के रेशम का कोट पहना था। मैं पहले अ’र्ज़ कर चुका हूँ कि वो एक ख़ुश-रू नौजवान था। अब तो मसर्रत और कामयाबी ने उसके चेहरा को और भी रौशन कर दिया
था। वो बेरूत को देखकर मुस्कुरा कर बोला, “ओहो ख़ातून! आपने आज ग़ुस्ल कर लिया। मुझे बेहद मसर्रत है, दिली मुबारकबाद!”
बेरूत मुस्कुराई और ख़ामोश हो गई। मैं बोल उठा, “रुश्दी मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आपने जो एहसान-ए-अ’ज़ीम मुझ पर किया है, इसके लिए अगर मैं उ’म्र-भर भी शुक्रिया अदा करता हूँ
तो कम है।”
रुश्दी बोला, “मुझे आपके शुक्रिये की ज़रूरत नहीं, और जनाब सच तो ये है कि मैं ये एहसान आप पर नहीं बल्कि अपने आप पर किया है।”
ये कह कर इस अंदाज़ से हँस पड़ा कि मैं सन्नाटे में आ गया। बेरूत एक सफ़ेद नफ़ीस फ़लालीन की शाल ओढ़े लेटी थी और दरीचे की सुब्ह की हवा से शायद किसी क़दर काँप रही थी।
“बेरूत क्या दरीचा बंद कर दूँ?”, ये कह कर मैंने खिड़की बंद कर दी।
(बाब - 6)
तब्दील-ए-आब-ओ-हवा की राय
इब्तिदा-ए-इ’श्क़ है रोता है क्या
आगे आगे देखिए होता है क्या
मई का महीना शुरू’ हो गया था। मौसम निहायत गर्म हो चुका था। अक्सर औक़ात शिद्दत-ए-गर्मी से परेशान हो कर हम लोग सर्द पानी में कपड़ा भिगो कर ओढ़ लिया करते थे। एशियाई ममालिक का गर्म आफ़ताब आग के शो’ले की तरह दहक रहा था। उफ़!
बेरूत अगरचे बीमार और फ़रीश न थी मगर हद दर्जा मुज़्महिल और नातवाँ थी और ज़र्द रहा करती थी। यही वज्ह थी कि वो अक्सर लेटी रहती थी और मैं उसकी दिल-जूई और दिल-बस्तगी के लिए अफ़साने या अख़बार पढ़ कर उसे सुनाया करता था।
एक ख़ुश-गवार और चमकीली सुब्ह, वो लेटी हुई थी और मश्ग़ले के तौर पर एक पुराने लिफ़ाफ़े को मरोड़ रही थी। मैं हस्ब-ए-मा’मूल उसके पास कुर्सी पर निस्फ़ लेटा था और ऑस्कर वाइल्ड का एक मा’रकतुलआरा अफ़साना पढ़ कर सुना रहा था। कभी-कभी हम दोनों अफ़्सानों के किसी मौज़ू’ पर बेहस भी करने लग जाते थे। दरीचे खुले हुए थे और लेमू की घास की ख़ुश्बू कमरे में आ रही थी। सामने बाग़ीचे में रौशन धूप जगमगा रही थी। नारंगी के दरख़्तों पर गर्म मौसम के ख़ुश-रंग परिंदे बैठे अभी तक सुब्ह का गीत गा रहे थे।
इतने में अब्बा जान अंदर आए। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
“तस्लीम! आईए चचा जान, तशरीफ़ रखिए।”, बेरूत ने उन्हें देखकर कहा। अब्बा जान ने झुक कर बेरूत की पेशानी चूमी और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गए।
“कैसी तबीअ’त है बेरूत?”, वालिद ने सवाल किया, फिर कमरे में इधर-उधर देखकर रूमाल से पेशानी ख़ुश्क करते हुए बोले, “उफ़! किस क़दर गर्म दिन है। आज तो सुब्ह ही से आग लगी! पंखा खोल दो बेटा जा’फ़र... पंखा मौजूद है फिर क्या वज्ह है कि इसको इस्ति’माल न किया जाए। ऐसी भी क्या हिमाक़त।”
मैंने पंखा खोल दिया। बेरूत बोली, “हाँ चचा जान, बस इसी गर्मी ने मुझे बेहाल कर दिया है। वर्ना मैं कभी की अच्छी हो चुकी होती। डाक्टर रुश्दी गुज़िश्ता शाम मुझसे यही कह रहे थे।”
“जा’फ़र!”, अब्बा जान ने गर्मी से परेशान होते हुए मेरी तरफ़ देखा, “क्या ये बेहतर होगा कि बेरूत बराए-चंदे किसी पहाड़ चली जाएँ? मेरे ख़याल में “मारिस फ़ौर” की आब-ओ-हवा इसके लिए मुफ़ीद है। यहाँ की गर्मी उसके लिए बहुत मुज़िर होंगी। तुम्हारी क्या राय है?”, ये जुमला अभी ख़त्म भी न हुआ था कि डाक्टर रुश्दी अपने वक़्त पर दरवाज़े पर आ मौजूद हुए।
“तस्लीम”, आते ही उन्होंने हम सबको देखकर कहा।
“ए लो... डाक्टर रुश्दी भी आ गए।”, अब्बा जान बोल उठे, “डाक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि बेरूत को मारिस फ़ौर भेज दूँ।”
डाक्टर रुश्दी चौंक पड़ा, “क्या इत्तिफ़ाक़ है जनाब! मैं ख़ुद अगले हफ़्ते मारिस फ़ौर जा रहा हूँ। मैंने कल ही साहबज़ादी से कहा था कि अगर वो मारिस फ़ौर चंद दिनों के लिए चली जाएँ तो बेहतर है।”
मेरे वालिद निहायत मसरूर लहजे में बोले, “वाह! ख़ुश-क़िस्मती है कि आप भी मारिस फ़ौर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो जा’फ़र मेरी राय है कि तुम सब के सब अगले हफ़्ते की शाम ही को चले जाओ।”
“जनाब क्या मैं भी जाऊँ?”, मैंने सवाल किया।
“हाँ! हाँ! तुम भी... मेहरबानी कर के ज़रा अपनी अम्माँ से पूछ आओ। वो भी साथ चलेंगी या नहीं। उन्हें हमेशा शहर की दा’वतों में शरीक रहना पड़ता है। मुझे उम्मीद नहीं कि वो चलें।”
ये सुनकर मैं हरम-सरा की तरफ़ गया और अम्माँ-जान से कुल कैफ़ियत कह सुनाई। इस वक़्त वो अपनी चंद बूढ़ी सहेलियों से मसरूफ़-ए-गुफ़्तगू थीं। कैफ़ियत सुनकर कहने लगीं, “एहे तुम्हारे अब्बा को क्या हो गया? बेरूत को कहाँ भेज रहे हैं? मेरा तो इरादा है कि इस माह के इख़्तिताम पर उसका ब्याह कर दिया जाए। ख़ैर से अब तुम भी तो हर तरह से तैयार हो। शादी हो जाए तो दोनों “अय्याम-ए-उ’रूसी” बसर करने मारिस फ़ौर जा सकते हो।”
उनकी दूसरी सहेलियों ने भी यही राय दी।
मैं कहने लगा, “अम्माँ-जान बेरूत अभी बहुत कमज़ोर है। मेरे ख़याल में उसे चंद दिन के लिए मारिस फ़ौर भेजा जाए तो वाक़ई’ बहुत बेहतर है, शादी की क्या जल्दी है।”
अम्माँ-जान बोलीं, “कमज़ोर है तो क्या हुआ, ताक़त आ ही जाएगी। वो ख़ुदा-न-ख़्वास्ता कुछ बूढ़ी थोड़ी है कि ताक़त आते साल-हा-साल लग जाएँ, और तुम मेरे जाने के मुतअ’ल्लिक़ पूछते हो। मैं तो जा ही नहीं सकती। शहर में कई ऐसी शादियाँ होने वाली हैं, जहाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। लो... मैं ख़ुद वहाँ आऊँगी और तुम्हारे अब्बा से बातचीत करूँगी। तुम जाओ।”
मैं ऊपर आया। जूँही मुझ पर अब्बा जान की नज़र पड़ी बोले, “भई तुमने तो बड़ी देर लगा दी।”
मैंने कह दिया कि, “वालिदा नहीं जा सकतीं।”
ये सुनकर अब्बा जान कहने लगे, “तो मैं साथ चलूँगा। तुम, मैं, बेरूत और डाक्टर रुश्दी। तो ये मुख़्तसर क़ाफ़िला अगले हफ़्ते यहाँ से कूच करेगा”
उसी वक़्त अम्माँ-जान ऊपर आईं, “कौन सा क़ाफ़िला? कहाँ जाएगा...?”
उनके अचानक सवाल पर सबकी नज़र ऊपर उठी। सबने उनका ख़ैर-मक़्दम किया और वो एक सोफ़े पर बैठ गईं। अब्बा जान ने कुल कैफ़ियत कह सुनाई। अम्माँ-जान अब्बा जान की तरफ़ देखकर बोलीं, “नासिर तुम तो मेरी उम्मीदों पानी फेर रहे हो। ऐसी क्या ज़रूरत है कि अभी से बेरूत मारिस फ़ौर भिजवा दी जाए।”
“मतलब?”, अब्बा जान ने सवाल किया, “तो आप ये चाहती हैं कि दो महीने बा’द जब गर्मियाँ रुख़्सत हो जाएँगी और सर्दियाँ तशरीफ़ लावेंगी, हम पहाड़ की सर्दी से ठिठुरने के लिए वहाँ जाएँ?”
अम्माँ-जान हँस पड़ीं, “मेरे ख़ुदा! अच्छा मतलब अख़ज़ किया आपने। मेरी तमन्ना ये है कि इस माह के इख़्तिताम पर अ’क़द हो जाए।”
“अ’क़द? किस का अ’क़द करोगी?”, अब्बा जान ने पूछा।
अम्माँ-जान मुस्कुराईं, “माशाअल्लाह! आप तो आज किसी बात को पहचानते ही नहीं। जाने क्या हो गया है... अ’क़द किस का करूँगी? भतीजी का, बेटे का। क्यों डाक्टर साहब! क्या ये बेहतर होगा कि अ’क़द के बा’द दोनों को अय्याम-ए-उ’रूसी बसर करने के लिए मारिस फ़ौर भेजा जाए?”
डाक्टर रुश्दी गोमगो की हालत में था। अब्बा जान ने फ़रमाया, “ओ... मैं अब समझा। ये मतलब था आपका। मुझे कोई उ’ज़्र नहीं मगर डाक्टर की राय सब पर मुक़द्दम है।”
ये सुनकर अम्माँ-जान डाक्टर रुश्दी की तरफ़ देखने लगीं, “क्यों डाक्टर साहब आप अपना ख़याल ज़ाहिर कीजिए।”
डाक्टर थोड़ी देर बा’द मुस्कुराए, “ख़ातून! मैं... मैं क्या अ’र्ज़ कर सकता हूँ? मगर मेरी राय तो यही है कि बेहतर होता अ’क़द का ख़याल दो-चार माह के लिए मुल्तवी कर दिया जाए। आप लोगों को कोई उ’ज़्र तो नहीं?”
“नहीं कोई उ’ज़्र नहीं।”, अब्बा जान ने जवाब दिया मगर अम्माँ-जान मायूस नज़र आने लगीं।
“ख़ैर, जब आपका यही ख़याल है तो मैं सब्र कर लूँगी।”, बारे वो फिर अब्बा जान की तरफ़ देखकर बोलीं, “तो आप सब लोग कब जाएँगे?”
“अगले हफ़्ते की शाम।”
ग़रज़ हम लोग हफ़्ते की शाम मारिस फ़ौर के लिए निकल गए।
(बाब - 7)
मारिस फ़ौर
वही मैं हूँ कि ग़ैरों को वहाँ आने देता था
वही मैं हूँ कि पहरों मिन्नतें करता हूँ ग़ैरों की
बेरूत इस सफ़र से बेहद ख़ुश थी और उसे ख़ुश देखकर मैं ख़ुश था। बेरूत गोया मेरी जान थी और मैं क़ालिब। मारिस फ़ौर का मौसम बेहद ख़ुश-गवार था और सुब्ह के वक़्त ख़ासी ख़ुनकी महसूस होती थी। बाज़-औक़ात ऐ’न दोपहर के वक़्त भी जर्सी पहन लेनी पड़ती थी।
सुब्ह का वक़्त था। हम लोग नाशते के बा’द बाग़ीचे में आ गए थे। यहाँ तो अच्छी ख़ासी सर्दी थी। बेरूत एक नीली रेशमी शाल में लिपटी हुई थी और इस क़दर ख़ूबसूरत मा’लूम होती थी जैसी नीली चिड़िया होती है। उसे देखकर मैंने कहा, “मेरी जान तुम किस क़दर प्यारी-प्यारी हो।”
“भई मुझसे तो चला न जाएगा सर्दी है।”, ये कह कर अब्बा जान रोज़ाना अख़बार लेकर बाग़ की पहली रविश पर बैठ गए। डाक्टर रुश्दी मुलाक़ाती कमरे में किसी दोस्त से बातें कर रहे थे। मैं बेरूत को लेकर बाग़ के आख़िरी हिस्से की तरफ़ चला। उसकी ख़ूबसूरती को देखकर दिल ही दिल में मर-मिट रहा था। आख़िर ज़ब्त न कर सका, “बेरूत! आज की सुब्ह तो तुम मा’मूली तौर पर हसीन नज़र आ रही हो।”
“दीवाने तो नहीं हो गए?”, उसने बे-साख़्ता हँसते हुए कहा। मैं चलते-चलते रुक गया। उसकी तरफ़ देखकर बोला, “वल्लाह मैं मज़ाक़ नहीं करता! तुम आख़िर यक़ीन क्यों नहीं करतीं? ख़ुदा के लिए बेरूत ये तो बताओ कि तुम मुझे कितना चाहती हो?”
“इतना... !”, उसने दोनों हाथों से एक गोल दाएरा बनाते हुए कहा। अब तो मुझे भी हँसी आ गई, “तुम बड़ी शरीर हो बेरूत! शरीर और प्यारी!”
“और तुम?”, उसने शोख़ लहजा में कहा, “शरीर और अहमक़!”
“अहमक़? बेरूत तुम मुझे अहमक़ समझती हो?”
“हाँ... क्योंकि मुहब्बत करना बेवक़ूफ़ी है। इसीलिए आ’शिक़ को मैं अहमक़ कहा करती हूँ।”
“हाय तुम बड़ी ज़ालिम हो। ख़ैर यूँही सही। हम अहमक़ हैं मगर ये तो कहो आख़िर तुम भी तो मुहब्बत करती हो। तुम में भी तो ये हिमाक़त मौजूद है।”
उसी वक़्त डाक्टर रुश्दी सुब्ह की एक निहायत नफ़ीस फ़लालीन में हल्की हल्की सीटी बजाते उधर आ गए। एक छोटा सा सफ़ेद गुलाब कोट के काज में लगा हुआ था और ये नौजवान बहुत शोख़-नज़र आ रहा था। बेरूत ने मुस्कुरा कर उनकी तरफ़ देखा, “सुब्ह-बख़ैर रुश्दी! आप तो सुब्ह से ग़ाइब थे!”
रुश्दी मुस्कुराया, “जी हाँ ख़ातून, कुछ दोस्त आ गए थे। उन्हें रुख़्सत कर के आ रहा हूँ।”
“गोया उनसे पीछा छुड़ा के आ रहे हैं आप।”, बेरूत ने शगुफ़्ता लहजा में कहा।
“बिल्कुल यही…”, डाक्टर रुश्दी ने हँसकर कहा।
थोड़ी देर इधर-उधर की गुफ़्तगू होती रही। फिर दफ़अ’तन रुश्दी ने बेरूत की तरफ़ देखकर कहा, “ख़ातून तुमने धूप घड़ी नहीं देखी? पहले ज़माने में लोग इसी से घड़ी का काम लेते थे।”
“मैंने नहीं देखी, किधर है?”, मुश्ताक़ लहजे में बेरूत ने सवाल किया।
“वो बहुत दूर है बेरूत।”, मैंने जवाब दिया।
बेरूत बोली, “बस तुम बड़े काहिल हो। तुमसे चला नहीं जाता तो यहीं बैठे रहो। हम दोनों देख आएँगे। डाक्टर रुश्दी तुम मुझे ले चलोगे?”
रुश्दी फ़ौरन राज़ी हो गया। मैं हँसकर बोला, “हाँ तुम दोनों देख आओ। मैं यहाँ बैठा रहूँगा।”
ये कह कर मैं एक कोच पर बैठ गया और सिगरेट सुलगा लिया। दोनों बातें करते हुए अंगूर के बेलों में नज़रों से ओझल हो गए।
अब तो अब्बा जान भी अपनी डाक देखने के लिए अंदर चले गए थे। मैं अकेला बैठा बैठा उकता गया। देखा तो सूरज सर पर आ रहा था। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ और मकान के ज़ीने तय कर ही रहा था कि पीछे से बाग़ में बेरूत की सुरीली आवाज़ आई, “ये लोग तो अंदर चले गए।”
मैं ज़ीने पर खड़ा हो गया, “तुम दोनों ने बड़ी देर लगा दी। बेरूत! तुम थक तो नहीं गईं प्यारी?”
बेरूत भी ऊपर आ गई बोली, “तुम इतनी फ़िक्र क्यों करते हो। डाक्टर मेरे साथ हैं फिर मुझे क्या फ़िक्र?”
मैं मुस्कुराया, “ठीक है डाक्टर की मौजूदगी में मरज़ महसूस नहीं होता।”
इसके बा’द हम सब कमरा-ए-तआम में आ गए। खाना खाने के दौरान में मेज़ पर बेरूत अब्बा जान से धूप घड़ी का हाल बयान करती रही। उफ़ उसकी तक़रीर में बला का जादू था अगरचे वो कभी मुझसे इ’श्क़िया लहजे में बात नहीं करती थी, ताहम उसके अल्फ़ाज़ कुछ इस क़दर मीठे होते थे कि मैं घंटों उनसे लुत्फ़-अंदोज़ हुआ करता था।
एक सुब्ह मैं और डाक्टर रुश्दी बाग़ में बैठे शतरंज खेल रहे थे कि बेरूत आ गई और क़हक़हा लगाकर बोली, “शतरंज... ख़ुदा ख़ैर करे मगर यक़ीन करो मियाँ जा’फ़र तुम डाक्टर रुश्दी का मुक़ाबला कभी न कर सकोगे। (हँसकर) डाक्टर बड़ा चलता पुर्ज़ा है मगर तुम निहायत काहिल और कुंद-ज़हन हो।”
उसे लोगों में मेरी तहक़ीर कर के एक ख़ास लुत्फ़ आता था और मैं इन बातों का आ’दी था, इसलिए मुस्कुराकर कर बोला, “बेरूत साहिबा आपके फ़रमाने से पहले ही हमें इ’ल्म है कि रुश्दी साहब निहायत मश्शाक़ी शातिर हैं और अगर मैं कुंद-ज़हन हूँ तो तुम आ जाओ मेरी मदद को।”
“कभी नहीं।”, वो शरारत-आमेज़ हँसी हँसने लगी, “बल्कि मैं तो डाक्टर की तरफ़ हो जाऊँगी।”
ये कह कर वो डाक्टर के पहलू में बैठ गई और मेरा खेल फ़ना करने लगी। मैं तंग आकर बोला, “बेरूत ये तुम क्या ग़ज़ब करती हो। रुश्दी ख़ुद अच्छे शातिर हैं। अब तुम्हारी मदद की उन्हें ज़रूरत नहीं।”
“ख़ैर ख़ातून।”, रुश्दी ने मुस्कुरा कर कहा, “मिस्टर जा’फ़र मुझसे जलने लगेंगे, आप मुझे अब कुछ न बताएँ।”
बेरूत ने रुश्दी का हाथ पकड़ लिया, “कभी नहीं डाक्टर रुश्दी मैं कभी न उठूँगी। ता-वक़्त कि आप जीत न जाएँ। हाँ जा’फ़र हासिद हैं, अ’जब नहीं कि जी में जल रहे हों।”
मैं हँस पड़ा, “हरगिज़ नहीं! तुम ये क्या कहती हो... जिसमें तुम ख़ुश, उसमें मैं ख़ुश... तुम रुश्दी साहब की तरफ़ से खेल कर जीतना चाहती हो तो लो... मैं हारने पर तैयार हूँ।”
बेरूत हँसकर बोली, “लो... अब ये शर्मा कर लगे बातें बनाने। इनका खेल बिगड़ चुका रुश्दी साहब। आप बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हैरान हूँ कि ख़ुदा ने तुम में कितनी अच्छी अच्छी बातें भर दीं। देखो जा’फ़र ये रुश्दी साहब कैसे अ’जीब-ओ-ग़रीब आदमी हैं। अच्छे शिकारी हैं, अच्छे डाक्टर हैं, दिलचस्प जलीस हैं, मेहरबान दोस्त हैं।”
डाक्टर रुश्दी अपनी ख़ुश-क़िस्मती पर मुस्कुराने लगा। सच तो है कि अगर रुश्दी की जगह में होता तो सुनकर मर-मर जाता। थोड़ी ही देर बा’द बेरूत यका-य़क उठ खड़ी हुई, “जा’फ़र तुमसे तो चला नहीं जाता, तुम एक सुस्त मफ़लूज बूढ़े की तरह ही बैठे रहो, हम धूप घड़ी तक जाएँगे। क्यों डाक्टर?”
“ब-सर-ओ-चश्म।”
ये कह कर रुश्दी भी उठ खड़ा हुआ और दोनों चले गए। उसी दिन शाम के वक़्त मैं बरामदे में बैठा सिगरेट पी रहा था और अख़बार पढ़ता जाता था। बेरूत बाग़ के रास्ते से मेरे पास आ गई।
“क्या कर रहे अख़बार! इसे उठा कर फेंको! ये ख़ुश्क बूढ़ों का मशग़ला है।”
मैं मुस्कुरा कर अख़बार रखते हुए बोला, “क्या अख़बार पढ़ना ख़ुश्क मशग़ला है? बल्कि यूँ कहो कि न पढ़ना ख़ुश्क मशग़ला और बूढ़ों का मशग़ला। इससे दुनिया के मुख़्तलिफ़ हिस्सों की कैफ़ियत से आदमी बा-ख़बर हो जाता है।”
“अच्छा तो लाओ मैं भी पढ़ूँ…”, वो कोच पर बैठ गई और बड़े ग़ौर से अख़बार पढ़ने लगी। दो ही मिनट में उसने अख़बार फेंक दिया।
“मुझसे तो अब पढ़ा न जाएगा। शाम के वक़्त ये मशग़ला मौज़ूँ नहीं। आज मेरा जी नहीं लगता। डाक्टर रुश्दी अपने चंद दोस्तों के साथ हिरन के शिकार को गए हैं।”
“हिरन के शिकार...? ये तो औ’रतों या लड़कियों का काम है…”, मैंने मुस्कुरा कर कहा।
“क्यों?”, बेरूत ने मुतअ’ज्जिब हो कर मुझे देखा, “हाँ इतने बड़े से तवाना मर्द को एक ख़ूबसूरत से हिरन को मार कर ख़ुश नहीं होना चाहिए। ये उसके शायान-ए-शान नहीं। या कम-अज़-कम तुम्हारा आ’शिक़ तो हिरन को मारकर ख़ुश नहीं होता।”
“अपना-अपना मज़ाक़ है जा’फ़र तुम अपनी तारी’फ़ करते हो...? ख़ैर भई अब कुछ अच्छी बातें करो।रुश्दी की अ’दम-मौजूदगी में मेरा दिल मुश्किल से बहलता है।”
मैं फ़ौरन उसकी तरफ़ मुतवज्जेह हो गया।
“जान-ए-जा’फ़र क्या में इस क़ाबिल नहीं हूँ कि रुश्दी की अ’दम-मौजूदगी में तुम्हारा दिल बहलाऊँ? वो हँसने लगी, “क़ाबिल...? क़ाबिल की भी एक ही कही। इससे तुम्हारा मतलब क्या है?”
“मेरा मतलब ये था कि क्या तुम मुझे अपना दिलचस्प जलीस या रफ़ीक़ नहीं समझतीं?”
“जा’फ़र तुम ब-निस्बत अच्छे रफ़ीक़ के, अच्छे तीमारदार हो। तुमने मेरी बहुत तीमार-दारी की है। रुश्दी अलबत्ता बेहतरीन रफ़ीक़ कहलाए जा सकते हैं। बात ये है कि उनमें बहुत सी दिलचस्प बातें हैं।”
मैंने सिगरेट फेंक दिया, “मैं बेहद ख़ुश हूँ बेरूत तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया है। मैं डाक्टर रुश्दी का बहुत ही ममनून हूँ कि वो हर वक़्त तुम्हारी दिल-जूई का ख़याल रखते हैं। बेरूत आजकल सच्चे दोस्तों का फ़ुक़दान है।”
ये सुनकर बेरूत जोशीले लहजे में बोली, “हाँ और क्या... तुम रुश्दी को फ़रिश्ता कहो, वो इसी के क़ाबिल हैं।
“अगर तुम उन्हें फ़रिश्ता कहना पसंद करती हो तो मुझे भला क्या इंकार हो सकता है? तुम्हारी ख़ुशनूदी मुझे हर वक़्त मंज़ूर है।”
“मगर जा’फ़र वो अभी तक नहीं आए। क्या मुआ’मला है?”
मैं हँसा, “प्यारी बेरूत तुम नहीं जानती कि शिकार का शौक़ इंसान को कैसा दीवाना बना देता है।”
दफ़अ’तन मकान की तरफ़ से किसी के कराहने फिर लोगों के बोलने की आवाज़ आई। हम हवास-बाख़्ता चले।
(बाब - 8)
ज़ख़्मी
हम बाग़ीचे से हवास-बाख़्ता मकान में दाख़िल हुए ही थे कि अब्बा जान ने घबरा कर मुझे आवाज़ दी, “जा’फ़र-जा’फ़र...”
सुनते ही मैं बरामदे की तरफ़ दौड़ा। देखा तो बरसाती में एक कार खड़ी थी। डाक्टर रुश्दी नीम-होशी की हालत में थे और दो-चार आदमी उन्हें पकड़े थे।
“उफ़! ये क्या हो गया अब्बा जान!”. मैंने निहायत परेशान हो कर सवाल किया, “ज़ख़्मी हो गए हैं।”
“किस तरह?”, वालिद जल्दी में कुछ न कह सके सिवाए इसके, “शिकार को गए थे।”
हम सब उन्हें उठा कर कमरे में ले आए और कोच पर लिटा दिया। वो बुरी तरह से ज़ख़्मी हो गए थे। पेशानी पर भी ख़राशें आईं थीं। उनकी आँखें बंद थीं। अब्बा जान निहायत परेशान थे और डाक्टर को बुलाने के लिए टेलीफ़ोन कर के बरामदे में टहल रहे थे। मुझे मरीज़ के पास छोड़ा था।
थोड़ी देर बा’द बेरूत कमरे में आई। वो निहायत परेशान नज़र आ रही थी और बार-बार रुश्दी को झुक-झुक कर देखती थी। मुझसे उसकी परेशानी देखी न गई। मैं उसके क़रीब गया और उसका हाथ पकड़ कर बोला, “बेरूत! तुम इस क़दर परेशान न हो। मुझसे देखा नहीं जाता, वो अच्छे हो जाएँगे।”
उसी वक़्त रुश्दी ने आँखें खोल दीं और इत्तिफ़ाक़ से उनकी नज़र बेरूत पर पड़ी, “कया है?” रुश्दी ने सवाल किया।
“कुछ नहीं रुश्दी। तुम अच्छे हो।”, बेरूत ने निहायत धीमे लहजे में जवाब दिया... मैंने दिल में कहा। रुश्दी? सिर्फ़ रुश्दी? बेरूत तो उन्हें डाक्टर रुश्दी कहा करती थी। शायद आ’लम-ए-परेशानी और बद-हवासी में मुँह से डाक्टर रुश्दी के बजाए सिर्फ़ रुश्दी निकल गया। मैं उसकी बदहवासी पर मुस्कुराने लगा। रुश्दी ने बेरूत से फिर सवाल किया, “कमरे में कौन कौन हैं?”
बेरूत इस पर झुक कर बोली, “तुम ये क्यों पूछते हो?”
“बेरूत तुम कहीं न जाओ! मैं सख़्त दर्द में मुब्तला हूँ।”
ये कह कर रुश्दी ने आँखें बंद कर लीं। मैं अब तक रुश्दी के सिरहाने खड़ा था और उसे मेरी मौजूदगी का इ’ल्म न था। अब मैं सामने आया और निहायत हम-दर्द लहजे में बोला, “साहब! बेरूत कहीं न जाएँगी। वो यहीं रहेंगी। हम सब आपके पास हैं। बे-शक तीमारदारी के लिए सिवाए औ’रत के कोई हस्ती मौज़ूँ न हो सकती।”
डाक्टर ने कोई जवाब न दिया और आँखें बंद किए पड़ा रहा। बेरूत एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई। आह! इस क़दर ख़ून बह गया है... ओ... मैं भोली... मजरूह के आगे बार-बार इसका ज़िक्र न करना चाहिए।” (दफ़अ’तन) “मगर आह!... कितना ज़ियादा... कितना बहुत ख़ून... उफ़! मैं देख नहीं सकती।” डाक्टर रुश्दी ने ब-मुश्किल करवट बदली और बेरूत की तरफ़ मुड़ कर मुस्कुरा कर कहने लगा, “प्यारी ख़ातून इस क़दर न हिरासाँ हो।”
मैंने ग़ौर से देखा तो बेरूत की सियाह आँखें आँसुओं से जगमगा रही थीं। मुझे सख़्त सदमा हुआ, बोला, “प्यारी बेरूत !ओ मैं तुम्हारे आँसू नहीं देख सकता। इन्हें जल्द ख़ुश्क कर लो।”
मैं कुछ सोचता हुआ दरीचे तक आया। आसमान पर गुलाबी गुलाबी बादल इधर-उधर दौड़ते फिरते थे।हवाएँ निहायत सुरीली थीं और कायनात की हर चीज़ बे-फ़िक्र नज़र आ रही थी, जब कि मैं एक निहायत अहम पेचीदा मुआ’मले पर ग़ौर कर रहा था जो मेरी समझ से यक़ीनन बाला-तर था। वो क्या मुअ’म्मा था।
(बाब - 9)
मेरी अ’लालत
तू पूछे या न पूछे मुझको ये सौदा मुबारक हो
ये क्या कम है कि दम भरता हूँ मैं तेरी मुहब्बत का
बेचारे डाक्टर रुश्दी बुरी तरह से ज़ख़्मी हो गए थे। कामिल दो हफ़्ते बीमार रहे। हम सबको उनका बड़ा ख़याल था। बेरूत ने तो उनकी वाक़ई’ बड़ी ख़िदमत की। वो दिन-भर उनके पास रहती थी, मगर रात को मेरी ड्यूटी थी। एक रात ही पर क्या मुनहसिर है, मैंने महज़ बेरूत को ख़ुश करने के लिए उसके दोस्त की चौबीस घंटे वो ख़िदमत की कि उसकी माँ ने भी उसको पालने में इतनी तकलीफ़ न उठाई होगी। आ’शिक़ को सग-ए-हबीब महबूब होता है... यही वज्ह थी कि मैंने अपने आराम का कोई ख़याल न किया। इसका सिला मुझे मिल गया या’नी बेरूत मुझसे बेहद ख़ुश थी और मेरी आ’ला ज़र्फ़ी की तारी’फ़ करती थी। मेरा ख़ाल था कि तीमारदारी की मेहनत ने मुझे मुज़्महिल और अ’लील कर दिया है मगर निकला मलेरीया... ख़ुद रुश्दी मेरा इ’लाज करने लगे।
मैं दिन-भर अपने कमरे में अकेला पड़ा सर्द आहें भरा करता था, मगर मेरी तसल्ली के लिए वहाँ कोई न था। अब्बा जान दिन में अक्सर आया करते थे मगर वो मेरे हम-उ’म्र और साथ के खेले तो थे नहीं कि उनसे बे-तकल्लुफ़ी की बातें कर के ज़माना-ए-अ’लालत की वहशत को दूर करता। अगरचे रुश्दी ब-हैसियत-ए-तबीब मेरे देखने के लिए दिन में दो मर्तबा तशरीफ़ लाते थे मगर बहुत जल्द कमरे से बाहर चले जाते। लिहाज़ा उनका आना न आना मेरी दिल-बस्तगी के लिए यकसाँ था। अलबत्ता मुझे हल्की सी शिकायत अपनी बेरूत से ज़रूर थी कि वो मेरी मिज़ाज-पुर्सी को दिन में सिर्फ़ एक दफ़ा’ और वो भी बेहद जल्दी में आती और चली जाती। मगर ये सोच कर चुप हो जाता था :
फ़ायदा क्या हवस-ए-दिल के बढ़ाने से जलील
वही निकलेंगे जो अरमाँ हैं निकलने वाले
शाम का वक़्त था। आफ़ताब ग़ुरूब हो चुका था। मैं अपनी तन्हाई और अ’लालत पर रंज करता एक कोच पर नीम-दराज़ था। दरीचा खुला था और उसमें से हो कर मद्धम रौशनी उस किताब पर पड़ रही थी जो मेरे हाथ में थी और जिसे मैं निहायत बे-तवज्जोही से पढ़ रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला, ख़ुश्बू कमरे में महकने लगी। नज़र उठा कर देखा तो बेरूत अपने शाम के तफ़रीही लिबास में खड़ी मुस्कुरा रही थी।
“मेरी जान तुम अपने क़द्र-दान को कल सुब्ह से देखने नहीं आईं।”
बेरूत आकर मेरे पास बैठ गई।
“हाँ जा’फ़र मुझे मुआ’फ़ करो। मौक़ा’ न था। ऐं क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? तारीकी में आँखें ख़राब हो जाएँगी।”
मैं मुस्कुराया, “फिर तन्हाई में क्या करता?”
अपने बीमार से परहेज़ किया करते हो
जाओ भी बस तुम्हें ऐ रश्क-ए-मसीहा देखा
“क्या चचा जान नहीं आते तुम्हें देखने? मैं क्या करूँ जा’फ़र ये रुश्दी बड़ी ज़िद्दी शख़्स है। भई सच पूछो तो अब मैं ख़ुद इससे तंग आ गई हूँ। वो आज मुझे दरिया पर मछली का शिकार दिखाने ले गए थे। मैंने हर-चंद चलने से इंकार किया और कहा कि मैं जा’फ़र को बीमार छोड़कर कहीं नहीं जा सकती मगर उसने न माना। यही कहता रहा कि मैं ख़ुद डाक्टर हूँ और जानता हूँ कि मिस्टर जा’फ़र अब बिल्कुल अच्छे हैं। सिर्फ़ नक़ाहत बाक़ी है। अब तुम ही कहो में क्या करती?”
मैं मुस्कुराया, “डाक्टर ने वाक़ई’ सच कहा है। अब मैं अच्छा हूँ सिर्फ़ नक़ाहत बाक़ी है।”
“क्या दिन-भर तन्हा थे।”
मैंने किताब बंद कर के रख दी। दरीचे का पर्दा रौशनी के लिए हटा दिया और कोच पर बैठ कर बोला, “हाँ... मगर तुम फ़िक्र न करो। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी वज्ह से तुम्हारी दिलचस्पियों में रुकावट पैदा हो। ये तो ख़ुद-ग़रज़ी है कि बीमार अपनी मसर्रत के लिए एक तंदुरुस्त ख़ुश-मिज़ाज आदमी को अपने कमरे की उदास फ़िज़ा में मुक़य्यद कर रखे। मैं इसे सख़्त ना-पसंद करता हूँ।”
उसने फिर गुफ़्तगू शुरू’ की, “रुश्दी अ’जब शौक़ीन नौजवान है। उन्हें मछली के शिकार से ख़ास दिलचस्पी है। उन्होंने कुछ इस इसरार से बुलाया कि मैं इंकार न कर सकी। तुम भी होते तो इंकार न कर सकते।”
मैं मुस्कुराया, “अब मैंने तुमसे शिकायत थोड़ा ही की थी? तुमने बहुत अच्छा किया जो कुछ किया। तुम्हारा दिल बहल जाता है तो गोया मेरी दिल-बस्तगी का सामान हो जाता है।”
मैं नहीं कहता कि अग़यार से ज़िंहार न मिल
मेरी उलफ़त में कोई हो नहीं सकता हाइल
कभी होगा असर-अंदाज़ मिरा दिल जज़्बा-ए-दिल
इक न इक रोज़ छोड़ेगा कर के क़ाइल
अब बुरा है तो कोई वक़्त भला आएगा
आपसे आप मिरे घर तू चला आएगा
“अब वो कल मुझे फूलों की नुमाइश में ले जाना चाहते हैं मगर तुम बीमार हो। ऐं... तुम्हारा हाथ बहुत ही गर्म है!”, बेरूत ने दरीचे की तरफ़ देखते हुए कहा।
“कुछ मुज़ाइक़ा नहीं, तुम कल ज़रूरी चली जाओ।”
“हाँ... मैंने वा’दा कर लिया है, जाना ही पड़ेगा। अच्छा अब ख़ुदा-हाफ़िज़ ख़ुदा। जाने तुम इस कमरे में तन्हा किस तरह पड़े रहते हो। दस मिनट मुझसे बैठा नहीं जाता। शाम का वक़्त ही कुछ ऐसा होता कि सिर्फ़ तफ़रीह में गुज़ारना चाहिए। मैं कल शाम यक़ीनन तुम्हें देखने आऊँगी।”
“शुक्रिया प्यारी बेरूत! ज़रूर आओ।”
(बाब - 10)
तक़दीर का नविश्ता!
एक दिन अपने कमरे में आईना के आगे खड़ा नेकटाई बाँध रहा था कि एक पुरानी मुलाज़िमा ने मेरे शाने को छुवा और बोली, “साहब-ज़ादे! क्या साहब का इरादा डाक्टर साहब को दामाद बनाने का है?”
“इसका क्या मतलब?”, मैंने झल्लाकर सवाल किया। वही बुढ़िया बोली, “डाक्टर रुश्दी से साहबज़ादी बेरूत ब्याही जाएगी।”
मेरा सर चकराने लगा और मैंने नफ़रत-अंगेज़ लहजा में कहा, “बेहूदा मत बको पगली बूढ़ी चुहिया।” कुछ दिनों बा’द यही सवाल मेरे एक दोस्त ने मुझसे किया जिसके जवाब में मैंने उसे थप्पड़ रसीद किया। मैं किसी क़दर परेशान हो कर बाग़ में निकल आया। शाम हो गई थी। सूरज नारंजी रंग का हो कर ग़ुरूब हो रहा था। घर में कोई न था। अब्बा जान किसी दोस्त के पास गए थे। बेरूत और डाक्टर रुश्दी भी चहल-क़दमी के लिए निकल गए थे। मुझे तन्हाई महसूस होने लगी। तबीअ’त पहले ही से परागंदा थी। हरी-हरी दूब पर कुछ सोचता हुआ टहलने लगा। मैंने देखा कि बेरूत और डाक्टर रुश्दी वापिस आ रहे हैं। रुश्दी तो मकान में दाख़िल हो गया मगर बेरूत मुझे देखकर ठिटकी, “जा’फ़र! तुम यहाँ क्या कर रहे हो?”
“टहल रहा हूँ।”
“अकेले टहल रहे हो? चचा जान कहाँ हैं?”
“वो बाहर गए हैं।”
वो भी मेरे साथ टहलने लगी। हम आहिस्ता-आहिस्ता साहिल की तरफ़ चले। चाँद तुलूअ’ होने लगा था। कायनात पर एक ख़ामोश हुस्न बरस रहा था। कभी-कभी एक-आध परिंद दफ़अ’तन पुकार उठता था वर्ना हर तरफ़ ख़ामोशी छाई हुई थी। मौजें साहिल से टकरा रही थी। साहिल पर पहुँच कर बेरूत ने कहा, “तुम नहीं जानते रुश्दी बड़े अच्छे कश्तीबान हैं।”
“वाक़ई’?”
“हाँ... हम दोनों कश्ती चलाते रहे।”
“तुम भी?”
“हाँ... पहले तो मैं डरी मगर फिर मैं भी उनके साथ कश्ती में बैठ गई।”
मैं मुस्कुराया, “बेरूत तुम्हारे दोस्त हमा-सिफ़त मौसूफ़ हैं। अब तो एक दिन तुम भी इस फ़न में ताक़ हो जाओगी। तुम हर-रोज़ उनके साथ कश्ती पर जाया करो।”
“वैसे हर-रोज़ ही उनके साथ जाया करती हूँ मगर आज तो ख़ूब लुत्फ़ आया। उनके ख़यालात निहायत बुलंद हैं। उनकी सोहबत इंसान को शगुफ़्ता बना देती है।”
मैं फिर मुस्कुराया, “हाँ वो ऐसे ही हैं बेरूत वो ऐसे ही हैं। मगर मुझे फ़िक्र है तो यही कि वो बहुत जल्द हमसे जुदा हो जाएँगे। फिर क्या होगा।”
बेरूत क़दरे घबरा के लहजे में बोली, “क्यों-क्यों? वो कहाँ जाएँगे?”
“प्यारी बेरूत।”, मैं कहने लगा, “वो हमारे ज़र-ख़रीदे ग़ुलाम थोड़े ही हैं कि उ’म्र-भर हमारे घर पड़े रहें? हम बहुत जल्द घर वापिस जाएँगे। फिर डाक्टर रुश्दी भी अपनी मुलाज़िमत पर चले जाएँगे। अब तो वो अब्बा जान के कहने पर तुम्हारी तिब्बी ख़बर-गीरी के लिए हमारे साथ आए हैं।”
उसे बहुत ख़ामोश देखकर उसकी तसल्ली के लिए मैंने कहा, “मगर तुम इस क़दर उदास न हो जाओ। मैं उन्हें ताकीद करूँगा कि अक्सर शाम के वक़्त हमारे पास आ जाया करें।”
इसके जवाब में वो हँसने लगी, “तुम्हारी ताकीद की ज़रूरत नहीं। ये तो पहले ही तस्फ़िया हो चुका है।”
“कैसा तस्फ़िया?”
“यही कि हम कभी जुदा न हों।”
“ये कैसे हो सकता है कि कभी जुदा ही न हों?”
“क्यों नहीं? जा’फ़र हमने सोच-सोच कर ये तदबीर निकाली है कि एक दूसरे के शरीक-ए-ज़िंदगी बन जाएँ।”
मेरा सर चकराने लगा।
“या’नी?”
वो हँसने लगी, “या’नी क्या...? वाह इतना भी नहीं समझे, हम शादी कर लेंगे।”
हैरत ने मुझे मुर्दा कर दिया, अफ़सोस ये क्या सन रहा हूँ मैं? रूह क़फ़स-ए-उं’सर ही में फड़फड़ाने लगी। सर चकराने लगा। हाय मेरी ख़िरमन-ए-आरज़ू पर बेरूत की बेवफ़ाई ने बिजली गिराई। अब मैं नहीं जियूँगा। मौत मेरे लिए बेहतरीन तोहफ़ा, मेरा जीना फ़ुज़ूल, मेरी ज़िंदगी बे-फ़ाएदा, मुझे बेरूत से इ’श्क़ था। मैं बग़ैर उसके इतनी बड़ी इतनी लंबी पहाड़ सी ज़िंदगी क्योंकर बसर कर सकूँगा? ना-मुम्किन! आख़िर मैंने क्या ख़ता की? वो मुझे महरूम क्यूँ-कर रही है? मुझसे क्या क़सूर सरज़द हुआ आख़िर?
“जा’फ़र तुम ख़ामोश हो गए।”
मैं भला क्या जवाब दे सकता था? इतना कहा, “मेरी जान क्या ख़ाक बोलूँ? जिसमें तुम्हारी ख़ुशी है वही करो मगर... लिल्लाह ये तो बताओ मैंने आख़िर क्या ख़ता की? बेरूत तुम जानती हो कि
लब-कुशाई तो अज़ल से नहीं आ’दत मेरी
मुझको मजबूर मगर करती है हालत मेरी
तुझसे शिकवा है मिरा तुझसे शिकायत मेरी
ग़ैर की दाद की तालिब नहीं उलफ़त मेरी
तुझसे ज़ालिम पे तबीअ’त जो न आई होती
आज मैंने भी ये हालत न बनाई होती
भूल कर भी न किया तूने कभी याद मुझे
ज़ब्त की भी न मिली आह कभी दाद मुझे
रक्खा महरूम-ए-जफ़ा से सितम-ईजाद मुझे
इस तग़ाफ़ुल ने तेरी कर दिया बर्बाद मुझे
आँख उठा कर भी न देखा कभी शैदाई को
क्या करे कोई सनम तेरी मसीहाई को
मैं किसी तरह से भी क़ाबिल-ए-आज़ार न था
गर गुनहगार था, इतना भी गुनहगार न था
रह गई एक तमन्ना ये तिरी उलफ़त में
काश तू होता वफ़ादार मिरी उलफ़त में
याद है मुझको तिरा अहद-ए-फ़रामोशी भी
साथ अग़यार के सरगोशी भी रू-पोशी भी
उनकी महफ़िल में सरमस्ती भी मय-नोशी भी
उनसे इज़हार-ए-मुहब्बत भी हम-आग़ोशी भी
बा-वजूद यक्का मैं अंदोह-ए-सितम सहता हूँ
देख मजबूरियाँ मेरी कि मैं चुप रहता हूँ
आरज़ूओं की जो दुनिया थी मिटा दी तूने
बज़्म-ए-ख़लवत-कदा-ए-इ’श्क़ उठा दी तूने
रस्म अलताफ़-ए-मुरव्वत की भुला दी तूने
ऐ मिरी जान मुझे हाय दग़ा दी तूने
इन जफ़ाओं के सिले में मैं वफ़ा करता हूँ
तू सलामत रहे हर-दम ये दुआ’ करता हूँ
“चलो... अंदर चलो... मैं ख़ुशनसीब रुश्दी को मुबारकबाद दे लूँ।”
(बाब - 11)
कुछ अपनी निसबत
मैंने मजनूँ पे लड़कपन में असद
संग उठाया था सर याद आया
मैं एक मुद्दत से देख रहा था, आज़मा रहा था कि बेरूत रुश्दी पर फ़रेफ़्ता है। मैं ख़ूब जानता था कि वो दर-पर्दा मुझे धोका दे रही है। मेरे आगे वो मेरे रक़ीब से मसरूफ़ इख़्तिलात है। वो मुझे तन्हा छोड़कर मेरे रक़ीब के साथ तफ़रीह के लिए चली जाया करती थी। मैं ख़ामोश था और एक नतीजा पर पहुँचना चाहता था। आह! वो मेरे रक़ीब के आगे मेरी तहक़ीर करती थी और ना-मुराद शख़्स को ख़ुश क्या करती थी। मैं भी ज़ब्त करता रहा। इसके बा’द मैंने महज़ उसकी ख़ुशनूदी के लिए उसके आ’शिक़ और अपने रक़ीब का तीमारदार बना। उसकी ख़िदमत की मगर अ’लालत में दोनों ने तोता-चश्मी इख़्तियार की। मैं दिन-दिन भर अकेला रहता था और वो अपने आ’शिक़ के साथ सैर को निकल जाती थी, तब भी मैंने सब्र किया।
उफ़ न की मगर अब... अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब जब कि मेरा दामन-ए-आरज़ू तार-तार कर दिया गया है, मुझसे ज़ब्त-ओ-सब्र नहीं हो सकता। मैं अब वो कर गुज़रूँगा जो मेरे दिल में है। मैं बहादुर और जंग-जू क़ौम का मर्द हूँ। इंतिक़ाम की आग मेरे सीने में भड़क उठी है। मैं फ़ना कर दूँगा सबको... सबको, ला’नत है दुनिया पर, दुनिया की ज़िंदगी पर... यहाँ के धोकों पर, दग़ा-बाज़ियों पर। उफ़! ये दुनिया दोज़ख़ से भी ज़ियादा बुरी है,
ग़लत है दावा-ए-उलफ़त सरासर आ’शिक़ी झूटी
सबूत-ए-यकदिली झूटा दलील-ए-दोस्ती झूटी
अ’ज़ीज़ों की है तक़रीर-ए-ख़ुलूस-ए-बातिनी झूटी
ग़रज़ झूटी है दुनिया और झूटी भी बड़ी झूटी
मैं अपने रक़ीब को मौत के घाट उतार दूँगा। इसके बा’द मैं भी इस दुनिया में न रहूँगा। मेरी मुहब्बत मेरी तलवार... मेरा रीवौल्वर...!
(बाब - 12)
मुहब्बत का अंजाम
दिल दे के तुमको ये मुझे मा’लूम हो गया
सब कुछ करे मगर न मुहब्बत करे कोई
लीजिए मैंने अपना अफसाना-ए-ज़िंदगी आपको सुना दिया। मेरी ज़िंदगी की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपने इरादे, ख़ौफ़नाक इरादे में कामयाब हो गया। किस तरह हुआ, क्योंकर हुआ, उसके बताने की न मुझे ज़रूरत है न आपको सुनने की। मुख़्तसर ये कि मैंने अपने रक़ीब का ख़ात्मा कर दिया। एक लतीफ़ चाँदनी-रात में हम दोनों कश्तियों की सैर में निकले, बस वहीं उसका ख़ात्मा हो गया। अगरचे मैं इंतिक़ाम को निहायत कमीना हरकत समझता हूँ मगर इंसान रक़ाबत में क्या कुछ नहीं कर गुज़रता? आपको कभी किसी से इस शिद्दत की मुहब्बत हुई ही नहीं है। न ऐसी रक़ाबत का हादिसा आप पर गुज़रा है। फिर लिल्लाह कोई बताए कि आपको क्या हक़ है मुझे मौरिद बनाएँ?
इन वाक़िआ’त को आज तीन महीने और कई दिन गुज़र चुके हैं। मैं वतन छोड़कर जैरूस आ गया हूँ और एक कमरे में इत्मीनान से बैठा अपनी ज़िंदगी के इ’बरत-अंगेज़ वाक़िआ’त सफ़्हा-ए-क़िर्तास पर मुनक़्क़श करता जाता हूँ और जूँही ये अफ़साना ख़त्म होगा। मैं... बजाए इसके फ़रिश्ता-ए-मौत मेरे पास आने की तकलीफ़ करे, मैं ख़ुद उसके पास जा पहुँचूँगा।
मेरा ख़याल है कि मैंने अफ़साना ख़त्म कर दिया... लो... मेरी किताब-ए-ज़िंदगी भी बंद हुई जाती है... ख़ुदा-हाफ़िज़ मेरी इस अलम-नाक सवानह के पढ़ने वालो। दुआ’ करो कि तुम्हारे एक बद-नसीब भाई के एक अ’ज़ीम गुनाह को परवरदिगार मुआ’फ़ करे।
ख़ुदकुशी! उफ़... उफ़...
ऐसी हसरत से जान दी कि तुझे
इक तमाशा बना दिया हमने
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.