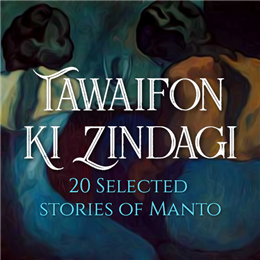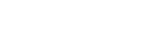काली शलवार
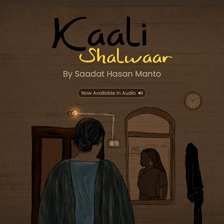
ख़ुलासा
एक पेशा करने वाली औरत सुल्ताना की आत्मा की पीड़ा और उसके अंत: के सन्नाटे को इस कहानी में बयान किया गया है। पहले ख़ुदा-बख़्श उसे प्यार का झांसा देकर अंबाला से दिल्ली लेकर आता है और उसके बाद शंकर मात्र काली शलवार के बदले उसके साथ जिस तरह का फ़रेब करता है उससे अंदाज़ा होता है कि मर्द की नज़र में औरत की हैसियत केवल एक खिलौने की सी है। उसके दुख-दर्द और इसके नारीत्व की उसे कोई पर्वाह नहीं।
दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी जहां कई गोरे उसके गाहक थे। उन गोरों से मिलने-जुलने के बाइस वो अंग्रेज़ी के दस पंद्रह जुमले सीख गई थी, उनको वो आम गुफ़्तगु में इस्तेमाल नहीं करती थी लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला तो एक रोज़ उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, “दिस लैफ़... वेरी बैड।” यानी ये ज़िंदगी बहुत बुरी है जबकि खाने ही को नहीं मिलता।
अंबाला छावनी में उसका धंदा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पी कर उसके पास आजाते थे और वो तीन-चार घंटों ही में आठ-दस गोरों को निमटा कर बीस-तीस रुपये पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे, उसके हम वतनों के मुक़ाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी ज़बान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था मगर उनकी ज़बान से ये लाइल्मी उसके हक़ में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रिआयत चाहते तो वो सर हिला कर कह दिया करती थी, “साहिब, हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता।”
और अगर वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी ज़बान में गालियां देना शुरू करदेती थी। वो हैरत में उसके मुँह की तरफ़ देखते तो वो उनसे कहती, “साहिब, तुम एक दम उल्लु का पट्ठा है। हरामज़ादा है... समझा।” ये कहते वक़्त वो अपने लहजे में सख़्ती पैदा न करती बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक़्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्ठे दिखाई देते।
मगर यहां दिल्ली में वो जब से आई थी एक गोरा भी उसके यहां नहीं आया था। तीन महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते होगए थे जहां उसने सुना था कि बड़े लॉट साहब रहते हैं, जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं, मगर सिर्फ़ छः आदमी उसके पास आए थे। सिर्फ़ छः, यानी महीने में दो और उन छः ग्राहकों से उसने ख़ुदा झूट न बुलवाए तो साढ़े अठारह रुपये वसूल किए थे। तीन रुपये से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था।
सुल्ताना ने उनमें से पाँच आदमियों को अपना रेट दस रुपये बताया था मगर तअज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, “भई हम तीन रुपये से एक कौड़ी ज़्यादा न देंगे।”
न जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ़ तीन रुपये के क़ाबिल समझा। चुनांचे जब छटा आया तो उसने ख़ुद उससे कह, “देखो, मैं तीन रुपये एक टेम के लूंगी। इससे एक धेला तुम कम कहो तो मैं न लूंगी। अब तुम्हारी मर्ज़ी हो तो रहो वर्ना जाओ।”
छट्ठे आदमी ने ये बात सुन कर तकरार न की और उसके हाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वरवाज़े बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, “लाइए एक रुपया दूध का।” उसने एक रुपया तो न दिया लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया है ग़नीमत है।
साढ़े अठारह रुपये तीन महीनों में... बीस रुपये माहवार तो इस कोठे का किराया था जिसको मालिक मकान अंग्रेज़ी ज़बान में फ़्लैट कहता था।
उस फ़्लैट में ऐसा पाख़ाना था जिसमें ज़ंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के ज़ोर से एक दम नीचे नल में ग़ायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ा-ए-हाजत के लिए उस पाख़ाना में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द होरहा था। फ़ारिग़ हो कर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई ज़ंजीर का सहारा ले लिया। उस ज़ंजीर को देख कर उसने ख़याल किया चूँकि ये मकान ख़ास हम लोगों की रिहायश के लिए तैयार किए गए हैं ये ज़ंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक़्त तकलीफ़ न हो और सहारा मिल जाया करे, मगर जूंही उसने ज़ंजीर पकड़ कर उठना चाहा, ऊपर खट खट सी हुई और फिर एक दम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुँह से चीख़ निकल गई।
ख़ुदाबख़्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ़ बोतल में हाइड्रोकुनैन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख़ सुनी। दौड़ कर वह बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, “क्या हुआ? ये चीख़ तुम्हारी थी?”
सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, “ये मुआ पाख़ाना है या क्या है। बीच में ये रेल गाड़ियों की तरह ज़ंजीर क्या लटका रखी है। मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुए ज़ंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुम से क्या कहूं।”
इस पर ख़ुदाबख़्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पैख़ाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें ज़ंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे ज़मीन में धँस जाती है।
ख़ुदाबख़्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ ये एक लंबी कहानी है। ख़ुदाबख़्श रावलपिंडी का था। इन्ट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा, चुनांचे चार बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से होगई। उसको भगा कर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूँकि उसको कोई काम न मिला। इसलिए उसने औरत को पेशे बिठा दिया।
दो-तीन बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। ख़ुदाबख़्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध होगया।
ख़ुदाबख़्श के आने से एक दम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूँ कि ज़ईफ़-उल-एतिका़द थी। इसलिए उसने समझा कि ख़ुदाबख़्श बड़ा भागवान है जिसके आने से इतनी तरक़्क़ी होगई, चुनांचे इस ख़ुश एतिक़ादी ने ख़ुदाबख़्श की वक़त उसकी नज़रों में और भी बढ़ा दी।
ख़ुदाबख़्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धर कर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने एक फ़ोटो ग्राफ़र से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फ़ोटो खींचा करता था। इसलिए उसने फ़ोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से साठ रुपये लेकर कैमरा भी ख़रीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, दो कुर्सियां खरीदीं और फ़ोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलाहिदा अपना काम शुरू कर दिया।
काम चल निकला, चुनांचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अंबाले छावनी में क़ायम कर दिया। यहां वो गोरों के फ़ोटो खींचता रहता। एक महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतअद्दिद गोरों से वाक़फ़ियत होगई, चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहां छावनी में ख़ुदाबख़्श के ज़रिये से कई गोरे सुल्ताना के मुस्तक़िल गाहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी होगई।
सुल्ताना ने कानों के लिए बुँदे ख़रीदे। साढ़े पाँच तोले की आठ कन्गनियाँ भी बनवा लीं। दस- पंद्रह अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा करलीं, घर में फ़र्नीचर वग़ैरा भी आगया। क़िस्सा मुख़्तसर ये कि अंबाला छावनी में वो बड़ी ख़ुशहाल थी मगर एका एकी न जाने ख़ुदाबख़्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली।
सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि ख़ुदाबख़्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख़याल करती थी। उसने ख़ुशी ख़ुशी दिल्ली जाना क़बूल करलिया। बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लॉट साहब रहते हैं उसका धंदा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ़ सुन चुकी थी। फिर वहां हज़रत निज़ाम उद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह थी। जिससे उसे बेहद अक़ीदत थी, चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो ख़ुदाबख़्श के साथ दिल्ली आगई। यहां पहुंच कर ख़ुदाबख़्श ने बीस रुपये माहवार पर एक छोटा सा फ़्लैट ले लिया जिसमें वो दोनों रहने लगे।
एक ही क़िस्म के नए मकानों की लंबी सी क़तार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्युनिसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा ख़ास कसबियों के लिए मुक़र्रर कर दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाएं। नीचे दुकानें थीं और ऊपर दोमंज़िला रिहायशी फ़्लैट। चूँकि सब इमारतें एक ही डिज़ाइन की थीं इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ़्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई थी पर जब नीचे लांड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहां मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ़्लैट तलाश कर लिया करती थी।
इसी तरह उसने और बहुत सी निशानियां क़ायम करली थीं, मसलन बड़े बड़े हुरूफ़ में जहां कोयलों की दूकान लिखा था, वहां उसकी सहेली हीरा बाई रहती थी जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी, जहां शरिफ़ा के खाने का आला इंतिज़ाम है। लिखा था वहां उसकी दूसरी सहेली मुख़्तार रहती थी। निवाड़ के कारख़ाना के ऊपर अनवरी रहती थी जो उसी कारख़ाना के सेठ के पास मुलाज़िम थी। चूँकि सेठ साहब को रात के वक़्त अपने कारख़ाने की देख-भाल करना होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे।
दूकान खोलते ही गाहक थोड़े ही आते हैं। चुनांचे जब एक महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोच कर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब दो महीने गुज़र गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने ख़ुदाबख़्श से कहा, “क्या बात है ख़ुदाबख़्श, दो महीने आज पूरे होगए हैं हमें यहां आए हुए, किसी ने इधर का रुख़ भी नहीं किया... मानती हूँ आजकल बाज़ार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने ही में न आए।”
ख़ुदाबख़्श को भी ये बात बहुत अर्सा से खटक रही थी मगर वो ख़ामोश था, पर जब सुल्ताना ने ख़ुद बात छेड़ी तो उस ने कह, “मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है, वो ये कि जंग की वजह से लोग-बाग दूसरे धंदों में पड़ कर इधर का रस्ता भूल गए हैं... या फिर ये हो सकता है कि...”
वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। ख़ुदाबख़्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज़ की तरफ़ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। ख़ुदाबख़्श ने लपक कर दरवाज़ा खोला। एक आदमी अंदर दाख़िल हुआ। ये पहला गाहक था जिससे तीन रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद पाँच और आए यानी तीन महीने में छः, जिनसे सुलताना ने सिर्फ़ साढ़े अठारह रुपये वसूल किए।
बीस रुपये माहवार तो फ़्लैट के किराये में चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके इलावा घर के दूसरे ख़र्च थे। खाना-पीना, कपड़े-लत्ते, दवा-दारू और आमदन कुछ भी नहीं थी। साढ़े अठारह रुपये तीन महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान होगई। साढ़े पाँच तोले की आठ कन्गनियाँ जो उसने अंबाले में बनवाई थीं आहिस्ता आहिस्ता बिक गईं।
आख़िरी कन्गनी की जब बारी आई तो उसने ख़ुदाबख़्श से कहा, “तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले में, यहां क्या धरा है?... भई होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहां ख़ूब चलता था, चलो, वहीं चलते हैं। जो नुक़्सान हुआ है उसको अपना सर सदक़ा समझो। इस कन्गनी को बेच कर आओ, मैं अस्बाब वग़ैरा बांध कर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहां से चल देंगे।”
ख़ुदाबख़्श ने कन्गनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, “नहीं जान-ए-मन, अंबाला अब नहीं जाऐंगे, यहीं दिल्ली में रह कर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियां सब की सब यहीं वापस आयेंगी । अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज़ है। यहां भी वो कोई न कोई अस्बाब बना ही देगा।”
सुल्ताना चुप हो रही, चुनांचे आख़िरी कन्गनी हाथ से उतर गई। बचे हाथ देख कर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आख़िर किसी हीले से भरना था।
जब पाँच महीने गुज़र गए और आमदन ख़र्च के मुक़ाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। ख़ुदाबख़्श भी सारा दिन अब घर से ग़ायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी दो-तीन मिलने वालियां मौजूद थीं जिनके साथ वो अपना वक़्त काट सकती थी पर हर रोज़ उनके यहां जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना-जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया।
सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती। कभी छालिया काटती रहती, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकोनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शैड में साकित और मुतहर्रिक इंजनों की तरफ़ घंटों बेमतलब देखती रहती।
सड़क की दूसरी तरफ़ माल गोदाम था जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर क़िस्म के माल अस्बाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल की पटड़ियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटड़ियाँ चमकतीं तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ़ देखती जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटड़ियों की तरह उभरी रहती थीं, इस लंबे और खुले मैदान में हर वक़त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं। कभी इधर कभी उधर।
उन इंजनों और गाड़ियों की छक-छक फ़क़-फ़क़ सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठ कर बालकोनी में आती तो एक अजीब समां नज़र आता। धुंदलके में इंजनों के मुँह से गाढ़ा-गाढ़ा धुआँ निकलता था और गदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था।
भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटड़ियों से उठते थे और आँख झपकने की देर में हवा के अंदर घुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को जिसे इंजन ने धक्का दे कर छोड़ दिया हो अकेले पटड़ियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख़याल आता।
वो सोचती कि उसे भी किसी ने ज़िंदगी की पटड़ी पर धक्का दे कर छोड़ दिया है और वो ख़ुदबख़ुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है... न जाने कहाँ। फिर एक रोज़ ऐसा आएगा जब इस धक्के का ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी। किसी ऐसे मुक़ाम पर जो उसका देखा भाला न होगा।
यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बांकी पटड़ियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ़ देखती रहती थी पर तरह तरह के ख़याल उसके दिमाग़ में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था मगर वहां उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग़ में ये भी ख़याल आता कि ये जो सामने रेल की पटड़ियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआँ उठ रहा है एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे-मोटे इंजन इधर-उधर धकेलते रहते हैं।
सुल्ताना को तो बा'ज़ औक़ात ये इंजन सेठ मालूम होते हैं जो कभी कभी अंबाला में उसके हाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की क़तार के पास से गुज़रता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाज़ार में से ऊपर कोठों की तरफ़ देखता जा रहा है।
सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग़ की ख़राबी का बाइस है, चुनांचे जब इस क़िस्म के ख़याल उसको आने लगे तो उसने बालकोनी में जाना छोड़ दिया। ख़ुदाबख़्श से उसने बारहा कहा, “देखो, मेरे हाल पर रहम करो। यहां घर में रहा करो। मैं सारा दिन यहां बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से ये कह कर उसकी तशफ्फी करदी, जान-ए-मन... मैं बाहर कुछ कमाने की फ़िक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों ही में बेड़ा पार हो जाएगा।”
पूरे पाँच महीने होगए थे मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था न ख़ुदाबख़्श का।
मुहर्रम का महीना सर पर आरहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी न था। मुख़्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वज़ा की क़मीज़ बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जट की थीं। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी।
अनवरी ने रेशमी जॉर्जट की एक बड़ी नफ़ीस साड़ी ख़रीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफ़ेद बोसकी का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फ़ैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मख़मल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाज़ुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखीं तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखती।
अनवरी और मुख़्तार के पास ये लिबास देख कर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मग़्मूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा होगया है। घर बिल्कुल ख़ाली था। ख़ुदाबख़्श हस्ब-ए-मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गाव तकिया सर के नीचे रख कर लेटी रही, पर जब उस की गर्दन ऊंचाई के बाइस अकड़ सी गई तो उठ कर बाहर बालकोनी में चली गई ताकि ग़म अफ़्ज़ा ख़यालात को अपने दिमाग़ में से निकाल दे।
सामने पटड़ियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे पर इंजन कोई भी न था। शाम का वक़्त था। छिड़काव हो चुका था इसलिए गर्द-ओ-गुबार दब गया था। बाज़ार में ऐसे आदमी चलने शुरू होगए थे जो ताक-झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख़ करते हैं।
ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ़ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटड़ियों पर एक इंजन नुमूदार होगया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ़ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़याल उसके दिमाग़ में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है।
ये अजीब-ओ-ग़रीब ख़याल दिमाग़ से निकालने की ख़ातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नज़र आया जिसने उसकी तरफ़ ललचाई नज़रों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देख कर एक लतीफ़ इशारे से पूछा, किधर से आऊं, सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया।
सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिल-ए-गुफ़्तुगू शुरू करने के लिए कहा, “आप ऊपर आते डर रहे थे।”
वो आदमी ये सुन कर मुस्कुराया, “तुम्हें कैसे मालूम हुआ... डरने की बात ही क्या थी?”
इस पर सुल्ताना ने कहा, “ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर इधर आए।”
वो ये सुन कर फिर मुस्कुराया, “तुम्हें ग़लतफ़हमी हुई। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ़्लैट की तरफ़ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंज़र पसंद आया। फिर बालकोनी में सब्ज़ बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज़ रोशनी मुझे पसंद है। आँखों को बहुत अच्छी लगती है।” ये कह उसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ।
सुल्ताना ने पूछा, “आप जा रहे हैं?”
उस आदमी ने जवाब दिया, “नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ... चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ।”
सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल ख़ामोशी से उन कमरों का मुआइना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आगए जहां पहले बैठे तो उस आदमी ने कहा, “मेरा नाम शंकर है।”
सुल्ताना ने पहली बार ग़ौर से शंकर की तरफ़ देखा। वो मुतवस्सित क़द का मामूली शक्ल-ओ-सूरत का आदमी था मगर उसकी आँखें ग़ैरमामूली तौर पर साफ़ और शफ़्फ़ाफ़ थीं। कभी कभी उनमें एक अजीब क़िस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। ख़ाकस्तरी रंग की गर्म पतलून पहने था। सफ़ेद क़मीज़ थी जिसका कालर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था।
शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को क़दरे परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा,“फ़रमाईए...”
शंकर बैठा था, ये सुन कर लेट गया, “मैं क्या फ़र्माऊँ, कुछ तुम ही फ़रमाओ। बुलाया तुम्हीं ने है मुझे।”
जब सुलताना कुछ न बोली तो वो उठ बैठा, “मैं समझा, लो अब मुझ से सुनो, जो कुछ तुम ने समझा, ग़लत है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ देकर जाते हैं। डाक्टरों की तरह मेरी भी फ़ीस है। मुझे जब बुलाया जाये तो फ़ीस देना ही पड़ती है।”
सुल्ताना ये सुन कर चकरा गई मगर इसके बावजूद उसे बेअख्तियार हंसी आगई, “आप काम क्या करते हैं?”
शंकर ने जवाब दिया, “यही जो तुम लोग करते हो।”
“क्या?”
“तुम क्या करती हो?”
“मैं... मैं... मैं कुछ भी नहीं करती।”
“मैं भी कुछ नहीं करता।”
सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, “ये तो कोई बात न हुई... आप कुछ न कुछ तो ज़रूर करते होंगे।”
शंकर ने बड़े इत्मिनान से जवाब दिया, “तुम भी कुछ न कुछ ज़रूर करती होगी।”
“झक मारती हूँ।”
“मैं भी झक मारता हूँ।”
“तो आओ दोनों झक मारें।”
“मैं हाज़िर हूँ मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता।”
“होश की दवा करो... ये लंगरख़ाना नहीं।”
“और मैं भी वालंटियर नहीं हूँ।”
सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, “ये वालंटियर कौन होते हैं।”
शंकर ने जवाब दिया, “उल्लु के पट्ठे।”
“मैं भी उल्लू की पट्ठी नहीं।”
“मगर वो आदमी ख़ुदाबख़्श जो तुम्हारे साथ रहता है ज़रूर उल्लु का पट्ठा है।”
“क्यों?”
“इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे ख़ुदा रसीदा फ़क़ीर के पास अपनी क़िस्मत खुलवाने की ख़ातिर जा रहा है जिसकी अपनी क़िस्मत ज़ंग लगे ताले की तरह बंद है।” ये कह कर शंकर हंसा।
इस पर सुल्ताना ने कहा, “तुम हिंदू हो, इसीलिए हमारे इन बुज़ुर्गों का मज़ाक़ उड़ाते हो।”
शंकर मुस्कुराया, “ऐसी जगहों पर हिंदू-मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पण्डित-मौलवी और मिस्टर जिन्ना अगर यहां आएं तो वो भी शरीफ़ आदमी बन जाएं।”
“जाने तुम क्या ऊट पटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे?”
“उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ।”
सुल्ताना उठ खड़ी हुई, “तो जाओ रस्ता पकड़ो।”
शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, “मैं कभी कभी इस बाज़ार से गुज़रा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बुला लेना... मैं बहुत काम का आदमी हूँ।”
शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूल कर देर तक उसके मुतअल्लिक़ सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहां कि वो ख़ुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुम्किन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता मगर यहां चूँकि वो बहुत उदास रहती थी, इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आईं।
शाम को जब ख़ुदाबख़्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, “तुम आज सारा दिन किधर ग़ायब रहे हो?”
ख़ुदाबख़्श थक कर चूर चूर होरहा था, कहने लगा, “पुराने क़िला के पास से आरहा हूँ। वहां एक बुज़ुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्ही के पास हर रोज़ जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं...”
“कुछ उन्होंने तुम से कहा?”
“नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए... पर सुलताना, मैं जो उनकी ख़िदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फ़ज़ल शामिल-ए-हाल रहा तो ज़रूर वारे-न्यारे हो जाऐंगे।”
सुल्ताना के दिमाग़ में मुहर्रम मनाने का ख़याल समाया हुआ था, ख़ुदाबख़्श से रोंनी आवाज़ में कहने लगी, “सारा सारा दिन बाहर ग़ायब रहते हो... मैं यहां पिंजरे में क़ैद रहती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ न आसकती हूँ। मुहर्रम सर पर आगया है, कुछ तुमने इसकी भी फ़िक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिऐं, घर में फूटी कौड़ी तक नहीं। कन्गनियाँ थीं सो वो एक एक करके बिक गईं, अब तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फ़क़ीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहां दिल्ली में ख़ुदा ने भी हम से मुँह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो। कुछ तो सहारा हो ही जाएगा।”
ख़ुदाबख़्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, “पर ये काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए... ख़ुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें न करो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकतीं। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने में सख़्त ग़लती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी ही के लिए करता है, क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम...”
सुल्ताना ने बात काट कर कहा, “तुम ख़ुदा के लिए कुछ करो। चोरी करो या डाका मॉरो पर मुझे एक शलवार का कपड़ा ज़रूर ला दो। मेरे पास सफ़ेद बोसकी की क़मीज़ पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा लूंगी। सफ़ेद नैनों का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दीवाली पर ला कर दिया था, ये भी क़मीज़ के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ़ शलवार की कसर है, सो वह तुम किसी न किसी तरह पैदा करदो... देखो तुम्हें मेरी जान की क़सम किसी न किसी तरह ज़रूर लादो... मेरी भत्ती खाओ अगर न लाओ।”
ख़ुदाबख़्श उठ बैठा, “अब तुम ख़्वाह-मख़्वाह ज़ोर दिए चली जा रही हो... मैं कहाँ से लाऊँगा... अफ़ीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं।”
“कुछ भी करो, मगर मुझे साढ़े चार गज़ काली साटन लादो।”
“दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह दो-तीन आदमी भेज दे।”
“लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे... तुम अगर चाहो तो ज़रूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन बारह चौदह आने गज़ मिल जाती थी, अब सवा रुपये गज़ के हिसाब से मिलती है। साढ़े चार गज़ों पर कितने रुपये ख़र्च हो जाऐंगे?”
“अब तुम कहती हो तो मैं कोई हीला करूंगा।” ये कह कर ख़ुदाबख़्श उठा, “लो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं।”
होटल से खाना आया दोनों ने मिल कर ज़हर मार किया और सो गए। सुबह हुई। ख़ुदाबख़्श पुराने क़िले वाले फ़क़ीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही। इधर उधर कमरों में टहलती रही, दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफ़ेद नैनों का दुपट्टा और सफ़ेद बोसकी की क़मीज़ निकाली और नीचे लांड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के इलावा वहां रंगने का काम भी होता था।
ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ीं जिनमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई, जब उठी तो चार बज चुके थे क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच चुकी थी।
नहा-धो कर फ़ारिग़ हुई तो गर्म चादर ओढ़ कर बालकोनी में आ खड़ी हुई। क़रीबन एक घंटा सुल्ताना बालकोनी में खड़ी रही। अब शाम होगई थी। बत्तियां रोशन हो रही थीं। नीचे सड़क में रौनक़ के आसार नज़र आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत होगई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम न हुई।
वो सड़क पर आते-जाते टांगों और मोटरों की तरफ़ एक अर्सा से देख रही थी। दफ़अतन उसे शंकर नज़र आया। मकान के नीचे पहुंच कर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ़ देख कर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने ग़ैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया।
जब शंकर ऊपर आगया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिला सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमइन था जैसे उसका अपना घर है, चुनांचे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पहले रोज़ की तरह वो गाव तकिया सर के नीचे रख कर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उससे कहा, “तुम मुझे सौ दफ़ा बुला सकती हो और सौ दफ़ा ही कह सकती हो कि चले जाओ... मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज़ नहीं हुआ करता।”
सुल्ताना शश-ओ-पंज में गिरफ़्तार होगई, कहने लगी, “नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है।”
शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, “तो मेरी शर्तें तुम्हें मंज़ूर हैं।”
“कैसी शर्तें?” सुल्ताना ने हंस कर कहा, “क्या निकाह कर रहे हो मुझ से?”
“निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर में किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं... छोड़ो इन फुज़ूलियात को। कोई काम की बात करो।”
“बोलो क्या बात करूं?”
“तुम औरत हो... कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाये। इस दुनिया में सिर्फ़ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, और कुछ भी है।”
सुल्ताना ज़ेह्नी तौर पर अब शंकर को क़बूल कर चुकी थी। कहने लगी, “साफ़ साफ़ कहो, तुम मुझ से क्या चाहते हो।”
“जो दूसरे चाहते हैं।” शंकर उठ कर बैठ गया।
“तुम में और दूसरों में फिर फ़र्क़ ही क्या रहा।”
“तुम में और मुझ में कोई फ़र्क़ नहीं। उनमें और मुझमें ज़मीन-ओ-आसमान का फ़र्क़ है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछना नहीं चाहिऐं ख़ुद समझना चाहिऐं।”
सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की फिर कहा, “मैं समझ गई हूँ।”
“तो कहो, क्या इरादा है।”
“तुम जीते, मैं हारी। पर मैं कहती हूँ, आज तक किसी ने ऐसी बात क़बूल न की होगी।”
“तुम ग़लत कहती हो... इसी मुहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लौह औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यक़ीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी ज़िल्लत क़बूल कर सकती है जो तुम बग़ैर किसी एहसास के क़बूल करती रही हो। लेकिन उनके न यक़ीन करने के बावजूद तुम हज़ारों की तादाद में मौजूद हो... तुम्हारा नाम सुल्ताना है न?”
“सुल्ताना ही है।”
शंकर उठ खड़ा हुआ और हँसने लगा, “मेरा नाम शंकर है... ये नाम भी अजब ऊटपटांग होते हैं, चलो आओ अंदर चलें।”
शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, “शंकर मेरी एक बात मानोगे?”
शंकर ने जवाबन कहा, “पहले बात बताओ।”
सुल्ताना कुछ झेंप सी गई, “तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ मगर।”
“कहो कहो... रुक क्यों गई हो।”
सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, “बात ये है कि मुहर्रम आरहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली शलवार बनवा सकूं... यहां के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। क़मीज़ और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।”
शंकर ने ये सुन कर कहा, “तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपये दे दूं जो तुम ये काली शलवार बनवा सको।”
सुल्ताना ने फ़ौरन ही कहा, “नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली शलवार बनवा दो।”
शंकर मुस्कुराया, “मेरी जेब में तो इत्तिफ़ाक़ ही से कभी कुछ होता है, बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख़ को तुम्हें ये शलवार मिल जाएगी। ले बस अब ख़ुश हो गईं।”
सुल्ताना के बुन्दों की तरफ़ देख कर शंकर ने पूछा, “क्या ये बुन्दे तुम मुझे दे सकती हो?”
सुल्ताना ने हंस कर कहा, “तुम इन्हें क्या करोगे। चांदी के मामूली बुन्दे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पाँच रुपये के होंगे।”
इस पर शंकर ने कहा, “मैंने तुम से बुन्दे मांगे हैं। उनकी क़ीमत नहीं पूछी, बोलो, देती हो।”
“ले लो। ये कह कर सुल्ताना ने बुन्दे उतार कर शंकर को दे दिए। इसके बाद अफ़्सोस हुआ मगर शंकर जा चुका था।
सुल्ताना को क़तअन यक़ीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा मगर आठ रोज़ के बाद मुहर्रम की पहली तारीख़ को सुबह नौ बजे दरवाज़े पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खड़ा था। अख़बार में लिपटी हुई चीज़ उसने सुल्ताना को दी और कहा, “साटन की काली शलवार है... देख लेना, शायद लंबी हो... अब मैं चलता हूँ।”
शंकर शलवार दे कर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में शिकनें पड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सो कर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है।
सुल्ताना ने काग़ज़ खोला। साटन की काली शलवार थी ऐसी ही जैसी कि वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत ख़ुश हूई। बुन्दों और इस सौदे का जो अफ़्सोस उसे हुआ था इस शलवार ने और शंकर की वादा ईफ़ाई ने दूर कर दिया।
दोपहर को वो नीचे लांड्री वाले से अपनी रंगी हुई क़मीज़ और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो अनवरी अंदर दाख़िल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ़ देखा और कहा, “क़मीज़ और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर ये शलवार नई है... कब बनवाई?”
सुल्ताना ने जवाब दिया, “आज ही दर्ज़ी लाया है।” ये कहते हुए उसकी नज़रें अनवरी के कानों पर पड़ी,। “ये बुन्दे तुमने कहाँ से लिये?”
अनवरी ने जवाब दिय, “आज ही मंगवाए हैं।”
इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक ख़ामोश रहना पड़ा।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.