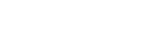संतर पन्च
मैं लाहौर के एक स्टूडियो में मुलाज़िम हुआ, जिसका मालिक मेरा बम्बई का दोस्त था। उसने मेरा इस्तक़बाल किया, मैं उसकी गाड़ी में स्टूडियो पहुंचा था। बग़लगीर होने के बाद उसने अपनी शराफ़त भरी मूंछों को जो ग़ालिबन कई दिनों से नातराशीदा थीं, थिरका कर कहा,“क्यों ख़्वाजा! छोड़ दी?”
मैंने जवाब दिया,“छोड़नी पड़ी।”
स्टूडियो का मालिक जो अच्छा फ़िल्म डायरेक्टर भी है (मैं उसे सहूलत की ख़ातिर गीलानी कहूंगा) मुझे अपने ख़ास कमरे में ले गया, इधर उधर की बेशुमार बातें करने के बाद उसने चाय मंगवाई जो निहायत ज़लील थी, ज़बरदस्ती पिलाई, कई सिगरेट इस दौरान ख़ुद फूंके और मुझ से फूंकवाए।
मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, चुनांचे मैंने उससे कहा, “यार, छोड़ो अब चाय की बकवास को, मुझे ये बताओ कि तुमने आज इतने बरसों के बाद कैसे याद कर लिया?”
“बस एक दिन अचानक याद आगए, बुला लिया... बताओ अब सेहत कैसी है?”
“तुम्हारी दुआ से ठीक है।” मेरे लहजे में दोस्ताना तंज़ था।
वो हंसा,“वाह, मेरे मौलवी साहब, मेरा ख़याल है कि जब से तुम ख़ुश्क ख़ुश्क हुए हो, तुम्हारी हर वक़्त शगुफ़्ता रहने वाली तबीयत ठहरे पानी की तरह ठहर गई है।”
“होगा ऐसा ही। ”
“होगा क्या, है ही ऐसा मुआ’मला, लेकिन ख़ुदा न करे, ऐसी ज़ेहानत जिसके सब मो’तरिफ़ हैं, उसका
भी यही हश्र हुआ। क्या तुम अब भी फ़िल्म कहानी का ढांचा तैयार कर सकते हो, फर्स्ट क्लास कहानी।”
मैंने उससे कहा, “फ़र्स्ट, सेकंड, इंटर और थर्ड मैं नहीं जानता, अलबत्ता कहानी ज़रूर होगी। तुम सोचते हो फ़र्स्ट की कहानी वो स्क्रीन पर आते ही थर्ड न बन जाये, या थर्ड जिसको तुमने डिब्बों में बंद कर के गोदाम में रख छोड़ा था, वो गोल्डन जुबली फ़िल्म साबित हुआ, क्या दुरुस्त नहीं। ख़ैर इन बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि चाहते क्या हो?”
उसने मुझे एक सिगरेट सुलगा कर दिया और संजीदगी से कहा,“देखो मंटो, मैं एक कहानी चाहता हूँ, बड़ा दिलचस्प रूमान हो और तुम मुझे उसका मुफ़स्सल स्कैच एक हफ़्ते के अंदर अंदर दे दो, क्योंकि में फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर से कंट्रैक्ट कर चुका हूँ, तुम बताओ कितनी देर में लिख लोगे?”
“फ़राग़त से एक महीने के बाद।”
सर्दियों का मौसम था, उसने अपने हाथ एक दूसरे के साथ बड़े ज़ोर के साथ मले। उसके इस अ’मल से दो चीज़ें ज़ाहिर होती थीं, अव्वल ये कि उसके हाथ गर्म हो गए हैं, दोम ये कि उसके सर का बोझ हल्का हो गया है कि उसको कहानी वक़्त पर मिल जाएगी और वो जो कि मेरी तरह तेज़ी से काम करने वाला है, उसे वक़्त-ए-मुक़र्ररा के अंदर अंदर डाइरेक्ट करके उसके प्रिंट डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले कर देगा और कंट्रैक्ट की रू से जो बक़ाया रक़म उसके नाम निकलती थी, उसी वक़्त मेज़ पर धरवा लेगा।
उस ने चंद लम्हात ग़ौर किया, “कल ही काम शुरू कर देगा?”
मैंने जवाब दिया, “काम तो मैं शुरू कर दूं, लेकिन यहां मेरे लिए कोई अ’लाहिदा कमरा होना चाहिए।”
“हो जाएगा।”
“और एक अस्सिटेंट...”
“मिल जाएगा... तो कल से आना शुरू कर दोगे।”
मैंने उससे कहा, “देखो गीलानी, मेरे घर से और तुम्हारे स्टूडियो तक का फ़ासला काफ़ी है, तांगे में आऊं तो क़रीब क़रीब डेढ़ घंटा... बस का सवाल ही पैदा नहीं होता।”
उसने पूछा,“क्यों?”
“या’नी उसका इंतिज़ार करना पड़ता है, बस स्टैंड पर खड़े रहो, ख़ुदा ख़ुदा कर के पाँच नंबर की बस आ गई। मुसाफ़िरों से भरी हुई और वो बग़ैर ठहरे चल दी और तुम ख़ुद को दुनिया का कम-तरीन इंसान महसूस करते हो, जी में आता है कि ख़ुदकुशी कर लो या फिर दुनिया वालों की बेरुख़ी से नजात हासिल करने के लिए सन्यास धार लो।”
गीलानी ने अपनी शरारत भरी मूंछें थिरकाईं।
“मैं शर्त बदने के लिए तैयार हूँ कि तुम कभी दुनिया त्याग नहीं सकते जिस दुनिया में हर क़िस्म की शराब मिलती है... और ख़ूबसूरत औरतें भी।”
मैंने चिड़ कर कहा, “औरतें जाएं जहन्नम में, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बम्बई के हर स्टूडियो में, जहां मैंने काम किया, उनसे दूर ही रहा।”
“तुम तो ख़ैर अपने वक़्त के डोन जोयान हो।”
“मज़ाक़ उड़ाते हो तुम ख़्वाजा मेरा।”
मैंने संजीदगी के साथ उससे कहा, “नहीं गीलानी;
रुत्बा बलंद मिला जिसको मिल गया
या यूं कह लो;
ईं सआ’दत बज़ोर बाज़ू नीस्त
ता न बख़शद ख़ुदाए बख़शिंदा
गीलानी मुस्कुराया,“ख़ुदाए बख़शिंदा तो बड़े अ’र्से से तुम्हें मरहूम ओ मग़फ़ूर कर चुका है। तुम बख़्शी हुई रूह हो।”
मैंने कहा,“इस से क्या होता है, मैं अपने गुनाहों की सज़ा भुगतना चाहता हूँ।”
“फ़लसफ़ा मत बघारो यार, ये बताओ, क्या अभी तक तुम्हारे पास वो उर्दू टाइपराइटर मौजूद है।”
“अच्छा तो ये बताओ कि वो एक्ट्रेस जिससे तुम ने कलकत्ता में शादी की थी, अभी तक तुम्हारे पास मौजूद है?”
गीलानी ने फ़ख़्रिया अंदाज़ में जवाब दिया,“मौजूद क्यों नहीं होगी, गोया तुम्हारी नज़र में एक्ट्रेस और टाइपराइटर में कोई फ़र्क़ नहीं?”
मैंने उससे कहा,“क्या फ़र्क़ है, एक फ़िल्म पर टाइप करती है दूसरी काग़ज़ पर, दोनों किसी वक़्त भी बिगड़ सकती हैं।”
गीलानी मेरी इन बातों से तंग आगया था। आख़िर मैंने उसको दिलासा दिया,“यार, ये सब मज़ाक़ था, तो मैं कल आजाऊँ? मेरा मतलब है तुम गाड़ी भेज दोगे?”
गीलानी सोफे पर से उठा, उसके साथ मैं भी। उसने कहा,“हाँ, हाँ भई, कब चाहिए तुम्हें गाड़ी?”
“कोई वक़्त भी मुक़र्रर कर लो... साढ़े नौ बजे सुबह।”
“ठीक है।”
“तुम काग़ज़ वग़ैरा आज ही मंगवा लेना, ताकि में स्टूडियो पहुंचते ही काम शुरू कर दूँ और तुम से उल्टा न सुनूं कि देखो तुमने मुझे लेट डाउन कर दिया। मेरा इतने हज़ार रुपये का नुक़्सान हो गया है।”
गीलानी ने बड़े प्यार से कहा, “क्या बकते हो यार, मैं तुम्हारी तबीयत से क्या वाक़िफ़ नहीं? कभी कभी तुम डुबकी लगा जाया करते हो।”
मैंने उसको यक़ीन दिलाया,“नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मुतमइन रहो। हाँ, मेरा टाइपराइटर यहां महफ़ूज़ तो रहेगा?”
गीलानी की आदत है कि वो ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाता है,“महफ़ूज़ नहीं रहेगा तो क्या गुंडे अग़वा करने आ जाऐंगे। अपने किसी आशिक़ के साथ तुम्हारी मशीन भाग निकलेगी।”
मैं बहुत हंसा।
हंसते हंसाते हम दोनों ने स्टूडियो का चक्कर लगाया। इसके बाद उसने मुझे अलविदा कही और मैं उसी गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गया, जहां पहुंचते ही मैंने टाइपराइटर की झाड़ पोंछ की। इसलिए कि एक मुद्दत से मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि फ़िल्मी कहानी लिखने का इस दौरान में कोई मौक़ा ही मयस्सर न आया।
बिगड़ा हुआ मकैनिक या मिस्त्री आर्टिस्ट बन जाता है, ये मेरा अपना ज़ाती इख़्तिरा करदा मुहावरा है।
गीलानी शुरू शुरू में मकैनिक था, बिगड़ कर वो आर्टिस्ट बन गया, पर वो मेहनती था। जब वो मिस्त्री था तो उसे ज़्यादा सहूलतें मयस्सर नहीं थीं लेकिन जब कैमरा क़ुली से तरक़्क़ी करता करता कैमरा मैन बन गया तो उसने कैमरे के हर पेच के मुतअ’ल्लिक़ अपनी ख़ुदादाद ज़ेहानत और जुस्तुजू तलब तबीयत की बदौलत ये दरयाफ़्त कर लिया कि इनका लोहे के इस चौखटे में अपनी अपनी जगह क्या मसरफ़ है।
कैमरे को वो उल्टा करता, कभी सीधा, कभी उसका गेट खोल कर बैठ जाता और घंटों उससे अपने मुख़्तलिफ़ साइज़ के पेच पुरज़ों के ज़रिये बोस-ओ-कनार में मशग़ूल रहता।
फ़ुर्सत के औक़ात, या’नी जब शूटिंग नहीं होती थी, वो अपनी साईकल पर शहर पहुंचता और सारा दिन कबाड़ियों की दुकानों पर सर्फ़ करता। उसको दुनिया के तमाम कबाड़ियों से मुहब्बत है, और उन के कबाड़ ख़ानों को वो बड़ी मुक़द्दस जगहें तसव्वुर करता था।
वो उन दुकानों में बैठ कर मंसूबा तैयार करता रहता कि सिलाई मशीन का हैंडिल जो बेकार पड़ा है अगर लोहे के फ़ुलां टुकड़े के साथ वेल्ड कर दिया जाये और उसके फ़ुलां के अंदर छोटे पंखे जो नुक्कड़ वाली दुकान में मौजूद हैं, लगा दिए जाएं तो फ़र्स्ट क्लास धौंकनी बन सकती है।
ख़ुदा मालूम वो क्या क्या सोचता था। इन दिनों दर असल ज़ेहनी वरज़िश कर रहा था। ये वो तैयारी थी जो वो अपने मंसूबों की तकमील के लिए इस्तेममाल करना चाहता था।
उसने एडिटिंग भी इसी तरह सीखी। आस पास की हर नन्ही से नन्ही शय का मुताला किया, और आख़िर एक दिन उसने स्टूडियो की एक फ़िल्म की ऐसी उम्दा एडिटिंग ऐकी कि लोग दंग रह गए।
सेठ ने सोचा कि अच्छे कैमरा मैन तो मिल जाऐंगे मगर ऐसा बाकमाल एडिटर जो सेलोलॉयड के छोटे बड़े फीते के टुकड़ों को इस चाबुकदस्ती से जोड़ता है कि फिर उसमें मज़ीद कतर-ब्योंत हो ही नहीं सकती, चुनांचे एडिटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। तनख़्वाह उसकी वही रही जो बहैसियत कैमरा मैन थी। वो अपना काम बड़ी मेहनत और तनदेही से करता रहा, लेकिन इसके साथ साथ वो लेबोरेट्री से भी दिलचस्पी लेता था।
थोड़ी ही देर में उसने उसके कल पुर्ज़ों में चंद इस्लाहात और तरकीबें पेश कीं जो बड़ी रद्द-ओ-कद के बाद क़बूल कर ली गईं। नतीजा देखा गया तो बड़ा हौसला अफ़ज़ा था।
सेठ ने एक दिन सोचा,“क्यों न गीलानी को एक फ़िल्म डायरेक्ट करने का मौक़ा दिया जाये।”
जब उससे पूछा,“तुम कोई फ़िल्म डायरेक्ट कर लोगे?”
तो उसने बड़ी ख़ुद ए’तिमादी से जवाब दिया,“हाँ सेठ, पर इसमें कोई दख़ल न दे!”
कहानी आधी गीलानी ने ख़ुद बनाई, आधी इधर उधर के मुंशियों से लिखवाई और अल्लाह का नाम लेकर शूटिंग शुरू कर दी। ये फ़िल्म ख़त्म हुआ और नुमाइश के लिए मुक़ामी सिनेमा हाउस में पेश किया गया तो उसने अगले पिछले तमाम रिकार्ड तोड़ दिए।
इसके बाद उसने लाहौर में दो फ़िल्म बनाए। ये भी सिलवर जुबली हिट साबित हुए। एक कलकत्ता जा कर फिर बनाया, वो भी कामयाब था। यहां वो बम्बई पहुंचा, क्योंकि वहां के फ़िल्मसाज़ों ने बड़ी तगड़ी तगड़ी आफ़रें भेजी थीं, चुनांचे एक जगह उसने ऑफ़र क़बूल कर के कंट्रैक्ट पर दस्तख़त कर दिए और कहानी “चन दे”का मंज़रनामा ख़ुद लिखा। फ़िल्म बन गया और इतना बड़ा बॉक्स ऑफ़िस साबित न हुआ।
शायद इसलिए कि बटवारे के बाइ’स दूसरे शहरों के मानिंद बम्बई में भी फ़िर्कावाराना फ़सादात शुरू हो गए। जिस तरह दूसरे मुसलमान हिज्रत कर रहे थे, उस तरह गीलानी भी बम्बई छोड़कर कराची चला गया। यहां से वो लाहौर पहुंचा और एक स्टूडियो की दाग़ बेल रखी, साउंड रिकार्ड सेट से लेकर कीलें ठोकने वाले तक को उसकी ज़ाती निगरानी में काम करना पड़ता था। क़िस्सा मुख़्तसर कि स्टूडियो तैयार हो गया।
लाहौर के मुसलमान हाथ पर हाथ धरे बैठे थे।
जब ये स्टूडियो बना तो उनकी जान में जान आई, चुनांचे यहां शूटिंग शुरू हो गई। इसके बाद ये चल निकला। गीलानी इस दौरान में स्टेज और इधर उधर के मुतअ’ल्लिक़ा सामान को दुरुस्त और मरम्मत कराने में मशग़ूल रहा। उसका दस्त-ए-रास्त लाहौर ही का एक नौजवान सिराजुद्दीन था, जो क़रीब क़रीब आठ बरस से उसके साथ था, ने कहा, “टाइपराइटर की दाल लेकर खा लो।”
इसके बाद गीलानी ने ख़ुद मेरे टाइपराइटर का मुआइना किया और फ़ैसला सादर कर दिया कि मशीन में कोई नुक़्स नहीं।
मगर सिराज अपने तजुर्बे के बलबूते पर मुसिर था, “नहीं हुज़ूर, ये अब मरम्मत तलब हो चुकी है,बड़े और छोटे रोलर सब नए लगवाने पड़ेंगे, ओवर हालिंग होगी, इसका कुत्ता भी नाक़िस हो चुका है, वो भी पड़ेगा।”
“तुम्हारी टांगों पर...”
“आप मेरा मज़ाक़ न उड़ाईए, अच्छा... ख़ैर आप ही सही कहते हैं।” ये कह कर वो अपने गंजे सर पर टोपी दुरुस्त करता हुआ चला गया।
गीलानी ने अपना ख़ास टूल बक्स मंगवाया और मशीन के सब पुर्जे़ अलग अलग कर के रख दिए। कोई पुर्ज़ा पत्थर पर घिसाया, कोई रेगमाल पर, किसी के सरेश लगाई, किसी को तेल। और उनको दुबारा फ़िट कर के फ़तहमंदाना अंदाज़ में मेरी तरफ़ देखा और कहा, “क्यों साहब! ठीक हो गई या नहीं।”
मैंने ऐसे ही कह दिया,“हाँ, अब ठीक है।”
गीलानी ने अपने पास खड़े अस्सिटेंट को बुलाया,“जाओ, उस उल्लु के पट्ठे एक्सपर्ट सिराज को बुला कर लाओ।”
चंद मिनट में सिराज हाज़िर हो गया।
उसने मशीन चलाई तो दस पंद्रह बार टप टप करने के बाद ही ख़ामोश हो गई। सिराज ने गीलानी से कुछ न कहा।
थोड़े वक़फ़े के बाद गीलानी बड़े तहक्कुमाना लहजे में उससे मुख़ातिब हुआ, “अच्छा तुम इसे बनाओ, देखें तुम क्या तीर मारते हो।”
मुझे अपनी पंद्रह साला अज़ीज़ मशीन की इस दुर्गत पर तरस आरहा था, मगर अब क्या हो सकता था,जब उसके अंजर पंजर ढीले हुए मेरी आँखों के सामने पड़े थे।
दूसरे दिन सिराज ने अपना टूल बक्स रिकार्डिंग में से मंगवाया और मेरी मशीन पर अपनी माहिराना सर्जरी शुरू कर दी।
ज़रूरी पुर्जे़ निकाल कर उसने अ’लाहिदा रख लिए और बाक़ी हिस्से पेट्रोल में डाल दिए। अब उनकी चिता जलाने के लिए सिर्फ़ माचिस की एक तीली ही काफ़ी थी।
मैं ख़ामोश रहा। ये सब कुछ देखता रहा।
कुत्ते के जबड़ों को एक पलास के साथ ज़ोर से पकड़ा और मेरी तरफ़ करते हुए बोला, “लो देख लो, मैं न कहता था... कुत्ता काम नहीं कर रहा। इसका तो संतर पंच ही ख़राब है।”
“संतर पंच?”
“हाँ...”
और सिराज एक बार फिर उसका संतर पंच ठीक करने लगा।
- पुस्तक : بغیر اجازت
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.