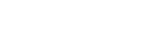एक शौहर की ख़ातिर
स्टोरीलाइन
दुनिया चाहे कितनी ही आधुनिक क्यों न हो जाए। हमारे समाज में एक औरत की पहचान उसके शौहर से ही होती है। ट्रेन के सफ़र करने के दौरान उसे तीन हमसफ़र मिलीं। तीनों औरतें और उन तीनों ने उस से एक ही क़िस्म के सवाल करने शुरू कर दिए। वह न चाहते हुए भी उनके अनचाहे जवाब देती रही। मगर जब आख़िरी स्टेशन पर क्लर्क ने उसे सामान की रसीद देते हुए शौहर का नाम पूछा तो उसे एहसास हुआ कि हमारे समाज में एक औरत की पहचान के लिए शौहर का होना कितना ज़रूरी है।
और ये सब कुछ बस ज़रा सी बात पर हुआ... मुसीबत आती है तो कह कर नहीं आती... पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि रेल में क़दम रखा अच्छी भली ज़िंदगी मुसीबत हो गई।
बात ये हुई कि अगले नवम्बर में जोधपुर से बम्बई आ रही थी सबने कहा... “देखो पछताओगी मत जाओ...” मगर जब च्यूँटी के पर निकलते हैं तो मौत ही आती है।
सफ़र लंबा और रेल ज़्यादा हिलने वाली, नींद दूर और रेत के झपाके, ऊपर से तन्हाई, सारा का सारा डिब्बा ख़ाली पड़ा था। जैसे क़ब्रिस्तान में लंबी लंबी क़ब्रें हों... दिल घबराने लगा।
अख़बार पढ़ते पढ़ते तंग आ गई। दूसरा लिया... उसमें भी वही ख़बरें, दिल टूट गया।
काश मैं क़ब्रिस्तान में होती। बला से मुर्दे ही निकल पड़ते। बच्चों को देख-देखकर जी हौल रहा था... काश कोई आ जाए... काश-काश... मैंने दुआ मांगनी शुरू की।
एक दम से रेल जो रुकी... तो एक दम से जैसे पटरियाँ टूट पड़ीं। इन्सान तो कम आए, बच्चे और बच्चियाँ ज़्यादा। बच्चे ऐसे जो क़हत-ज़दा गाँव से आ रहे थे। कि आते ही ख़ुराक पर पिल पड़े... दूध पीने वालों को तो ख़ैर सारा मुआमला मिल गया और वो जुट गए। बाक़ी के तिल-मिलाने और तड़पने लगे।
पोटलियाँ इस क़दर बे-हंगम और फ़ुज़ूल जगह घेरने वाली वज़’अ से बंधी थीं कि किसी कल बैठती ही ना थीं। एक संभाली तो दूसरी तैयार।
मैं अलैहदा पटरी पर इस ज़ाविए से बैठी थी कि गठरी गिरे तो मेरी रीढ़ की हड्डी बच जाये। मुझे अपने जिस्म में रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है... कहते हैं रीढ़ की हड्डी टूट जाये तो आदमी लोथड़ा हो जाता है।
“कहाँ जा रही हो...”
बेचारी हमसफर ने गठरियों की तरफ़ से ग़ैर मुत्म’इन होते हुए भी निहायत फ़िक्रमंद हो कर पूछा।
“मैंने जल्दी से बताया और फिर उनकी तवज्जो उस वज़नी गठरी की तरफ़ मुफ़्तफ़र की जो शायद बर्तनों की थी और ज़रा सी ठेस से गिरने को तैयार थी। अगर इत्तिफ़ाक़िया ज़रा हाथ लग जाता तो बर्तन इस तेज़ी से आपस में टकराते कि जी घबरा उठता...
“कहाँ से आ रही हो...”
मैंने ज़रा कम मुस्तैद से बताया।
“मैके जा रही हो...” जब तक शादी ना हुई हो तब तक जगत में ही है। और कहीं भी नहीं। यानी मैके और ससुराल का सवाल ही नहीं, लिहाज़ा में चकराती...
सोचा अंदाज़न किस सूबे में शादी होने का ख़तरा है।
“मियाँ के पास जा रही हो...”
“नहीं...” मैंने चाहा मौज़ू बदल जाता तो अच्छा होता ख़्वाह-म-ख़्वाह कौन हमदर्दी वसूल करे...”
“तो फिर ससुराल जा रही होगी...?”
क्यों... ज़रा इन सवालों के जवाब बहुत फ़लसफ़ियाना होते हैं।
“नहीं तो... मैं बम्बई जा रही हूँ... शादी... शादी तो नहीं हुई...”
मैंने ज़रा दिल में कुछ हक़ीर हो कर कहा।
हालाँकि शादी के ख़िलाफ़ कॉलेज के मुबाहिसे में मुझे अव्वल इनाम मिला था। और अब भी... ख़ैर अब तो... हाँ तो मैंने कहा। वो मुतहय्यर हो कर इतनी ज़ोर से उछलें कि बच्चे के मुँह से दूध छूट गया।
और वो मज़बूहा बकरी की तरह चीख़ा... मैंने ध्यान बटाने को उनकी तवज्जा बच्चे की तरफ़ करना चाही। मगर वो टटोल-टटोल कर बच्चे की नाक में दूध ठूंसने लगी। और मैं यहां लिखना नहीं चाहती कि मुझे उन्होंने किस रहम और मेहरबान सी नज़रों से देखा।
उन्हें मुझ पर मुहब्बत सी आने लगी... और मैं डरी... कि कहीं वो मुझे चिमटाकर रो ना पड़ें... उनका दिल बहलाने के लिए मैंने चने वाले को बुलवाया। मगर वो ऐसी ही उदास रहीं।
उन्हों ने मुझे दो एक दाँव पेंच एक अच्छा सा शौहर फांसने के बताए। जो बाद में तजुर्बा से क़तई बेकार साबित हुए।
मेरी दुआ शायद ज़रूरत से ज़्यादा क़बूल हो गई... या शायद मेरी ख़ुदा के हुज़ूर में कातिबीन की ग़लती से दुबारा अर्ज़ी पेश हो गई... कि एक फ़ौज इन्सानों की फिर आई इस फ़ौज में बड़े-बड़े रेशमी बुर्क़े और छतरियाँ ज़ाइद तादाद में थीं।
उनके साथ गन्ने भी थे जिनके टुकड़े नाप-नाप कर इतने बड़े काटे गए थे कि रेल के किसी कोने में ठीक से ना रखे जा सकें।
उनके बिस्तर और संदूक़ भी कुछ ऐसे थे। जो किसी पटरी के ऊपर या नीचे किसी अंदाज़ से भी ना हो।
इन बीबीयों ने आते ही रेल में हलचल मचा दी, संदूक़ और पुलंदे घसीट कर तबाह कर दिए। पहले वाली मुसाफ़िरों की ज़िद्दी पोटलीयाँ जो शायद ताक में थीं बच्चों और औरतों पर गिरीं। और वो सब एक दूसरे पर गिरे।
“कहाँ जा रही हो...”
वो भी कुछ परेशान थीं...
बताया...
“कहाँ से आ रही हो...?” बोलीं। हालाँकि अभी ठीक से जमी भी ना थीं।
बुर्क़ा फांसी लगा रहा था। मगर बताया।
“मैके जा रही हो या ससुराल...”
काश मुझे मा’लूम होता। मगर चूकने का मौक़ा ना था।
“ससुराल...” ऐसे कहा कि वो हमसफ़र जो पहले जिरह कर चुकी थीं न सुन पाएं।
“क्या करते हैं मियाँ...”
अब मैंने सोचा कुछ तो करते ही होंगे... बेकार तो काहे को फिरते होंगे।
मगर काश वो मुझे भी ये बता देते तो अच्छा ही था... बहर-हाल निखट्टू तो ना होंगे पर...
वो ख़ुद ही बोलीं।
“रेलवे में हैं...”
“हाँ... हाँ...” मैंने पुर-शौक लहजे से उन्हें यक़ीन दिलाया। ये ठीक रहा। मैंने सोचा रेलवे का आदमी ख़ूब रहेगा। मज़े से मुफ़्त के टिकट तो मिलेंगे... हिन्दोस्तान भर में घूम लू... और मुझे तो वर्दी भी इन कम-बख़्तों की पसंद है। ख़ुसूसन वो टोपी और सलेटी लाल हरी झंडी... अच्छा ही हुआ जो ये बेचारी मिल गईं... वर्ना अपने को तो कभी गार्ड... बाबू वग़ैरा का ख़्याल भी ना आया।
“ए हाँ सच्च तो है।”
“कौन काम पे हैं। वो रेल में।”
“किसी ठीक ही काम पर होंगे... और कया...” मुझे ख़्याल ही ना आया कि गार्ड बाबू की बीबी बनना आसान है... मगर ये तफ़सील तो ज़रा भारी ख़ुराक है।
“फिर भी... क्या काम करते हैं...” रेल में तो हज़ार से ज़ाइद काम हैं...”
ए... सीटी... क़ुली... मैं ऐसी बौलाई कि कुछ बन न पड़ा। सामने एक क़ुली बड़ा सा बंडल, एक बिस्तरा, आधी दर्जन सुराहियों की सीढ़ी और दो लोटे लिए चला आ रहा था। और ऐसे बन रहा था जैसे बहुत भारी हैं।
“क़ुली... तुम्हारा मियाँ क़ुली है...”
हैरत का दौरा उन पर भी पड़ा।
मैं चाहती थी ज़रा हम आहिस्ता-आहिस्ता गुफ़्तगु करें वर्ना कहीं पहली हमसफ़र ना सुन लें...
उनका बच्चा सुकून से दूध पी रहा था। मगर एक दफ़ा बात मुँह से निकल जाये तो फिर मैं भी उस पर ही जम जाती हूँ और यहां तो जीने के लाले पड़े थे।
“हाँ... आँ क़ुली ही सही फिर तुम्हें क्या...” मैंने ज़रा बुरा मान कर कहा।
“तुम्हारा... मिं... मियाँ क़ुली...”
“हाँ फिर... तुम क्यों जलो... तुम्हारा जी चाहे तुम भी क़ुली से कर लो...”
“दस क़ुलियों से करो... कौन रोकता है... इतने सस्ते में क़ुली...” मगर मैं ज़रा चुप रही। और मज़लूम सी सूरत बना ली...
“बोलीं...”
“कैसे हो गई तुम्हारी शादी क़ुली से...”
फिर सोचने लगी क़ुलियों से किस तरह शादियां होती हैं मैंने चाहा दिल से कुछ गढ़ों किसी क़ुली की शादी का हाल... मगर वो इस क़दर ग़ैर दिलचस्प मा’लूम हुआ। फिर मैंने कहा, “एक क़ुली था...”
“उन्होंने तवज्जा से सुना...”
“वो रहा करता था...” मैं चाहती थी वो मेरी हर बात पर हूँ करें या कम अज़ कम सर हिलाएँ...
“फिर किया हुआ कि एक दिन... कि...” काश मुझे मा’लूम होता उस वक़्त कोई भी क़िस्सा तो याद ना आया।
“वो ले जा रहा था सामान...” मैंने चाहा वो पूछें।
“किस का...”
और उन्होंने पूछा
“एक निहायत ही ख़ूबसूरत लड़की का... फिर वो लड़की... वो लड़की आशिक़ हो गई।”
“कौन लड़की...” अरे ये तो मा’लूम ही नहीं पड़ा... ख़ैर क्या मज़ायक़ा है कोई बात नहीं...
“यक़ीनन होगी ही कोई ना कोई लड़की... कोई ख़ूबसूरत सी ही लड़की होगी।”
“तो वो क़ुली पे क्यों आशिक़ होगी...”
“वो आशिक़ यूं हो गई कि... कि... अरे भाई अब ये क्या मा’लूम कोई तो वजह है ही आशिक़ होने की...”
“वो मुस्कुराया होगा उसे देखकर...”
इतने में एक निहायत भयानक क़िस्म का बाबू मुझे देख कर मुस्कुराया और मैं डरी कि कहीं सच-मुच आशिक़ ना होना पड़े... अभी इंटरव्यू में जाना है, सुने हैं कि इश्क़ में बड़ी ख़राब हालत हो जाती है। भला परदेस में कहाँ आशिक़ होती फिरूँगी... वैसे ये जसीम भाई के हाँ जाना है और वो हैज़ा के बाद बस इश्क़ से घबराते हैं... ख़ैर बात गई गुज़री हो गई।
“ए बहन। ये क्या कह रही हो...? कौन लड़की किस का इश्क़, मैं कहती हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई...?”
“हाँ... इन बेचारी की शादी नहीं हुई...”
आख़िर को पहली मुसाफ़िरा को पता चल ही गया ना...
कितना मरदुई से कहा आहिस्ता बोल... आहिस्ता बोल... ये लीजीए वो क़ुली भी हाथ से गया।
“जब नहीं हुई थी...”
“मैंने चाहा। शायद मान जाएं...”
“हुई... क्या रेल में बैठे-बैठे हो गई...”
“काश ऐसा हो सकता...” काश गर्म-गर्म चाय की बजाय लोग अमीर-अमीर, कमाऊ शौहर बेचते होते तो सफ़र के लिए तो मैं ज़रूर ले लेती... फिर चाहे... फिर देखा जाता...
और मैंने इरादा कर लिया कि, अब कि एक मुनासिब क़िस्म का मियाँ ढूंढना चाहिए... ऐसा इसमें क्या टोटा है अपना... ठीक ही रहेगा। बला से हर मुसाफ़िर से नए-नए झूट तो ना बोलने पड़ेंगे।
“भई किसी ने पूछा...” हाज़िर मियाँ...
“अरे भई अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं...” वो मेरे मुस्तक़बिल से ना-उम्मीद हो कर बोलीं।
“मोटर मांगते हैं... गाड़ी घोड़ा दो... और कभी कमाऊँ जभी ना... ऐसे मिले जाते हैं कमाऊ लड़के...”
मैं रंजीदा हो गई...
आख़िर ये लड़के कमाऊ क्यों नहीं होते... कम्बख़्त अच्छे लड़के पहले ज़माने में कितने होते थे। मूली गाजर की तरह। पर अब चाहो कि आँख में लगाने के लिए अच्छा लड़का मिल जाये तो नहीं, इस लड़ाई ने तो उजाड़ कर रख दिया।
चलो भई... पहले लड़के तो थे कमाओ नकटू पर अब तो जिसे देखो लड़ाई पर चला जा रहा है।
“लो साहब यहां तो बीवीयां ताने दे रही हैं। और लड़के हैं कि मरने-कटने पर तुले हुए हैं...”
“तुम फिर शादी क्यों नहीं कर लेतीं...” एक बोलीं
“जैसे आपकी मर्ज़ी...” मैंने उस मासूम लड़की की तरह कहा जिसे वालदैन शादी तय करने के बाद रौशन ख़्याल बनने के लिए राय देते हैं।
“कब करोगी फिर, अब नहीं करोगी तो...”
“अब... यानी अभी... मेरे ख़्याल में... तो... अगर जंक्शन तक ठहर जाते तो अच्छा था...”
“क्या...?”
“यही कि... जब आपकी मर्ज़ी है तो फिर क्यों इस नेक काम में देर की जाये...”
“कैसा नेक काम... क्या कह रही है लड़की...?” बहुत ही घबरा गईं।
“मैंने पूछा... भई शादी क्यों नहीं करतीं तुम...” दूसरी बोलीं।
“तुम क्यों नहीं करतीं शादी...”
“बस...” मैं अब काफ़ी जल उठी थी। हालाँकि उनका बच्चा मुसलसल दूध पी रहा था... मगर मैंने उसे नज़र-अंदाज़ कर दिया।
“ओई... मा’लूम होता है कुछ दिमाग़ भी ख़राब है।” वो बच्चा को और वाज़ह तौर पर लाईं ताकि ये ना मा’लूम हो कि वो सिर्फ़ गोद में सो रहा है।”
“तो... अच्छा... तुम्हारी शादी हो गई है... कब की तुमने शादी...?”
मैंने बे-तकल्लुफ़ी से पूछा।
“हमारे माँ बाप ने की हमारी शादी... हम भला ख़ुद ही क्यों करते...”
“तो आप शादी के ख़िलाफ़ हैं... ठीक है... बिलकुल ठीक... मेरे भी माँ बाप ने शादी की... जाहिल इन्सान...!”
इसके बाद कुछ मुकद्दर सी हो गईं और ग़मगीं हो कर नाशते-दान दान में से इमरतियाँ निकाल कर ग़म ग़लत करने लगीं।
“ऐ ख़ुदा... तो जब दुआएं क़ुबूल करने पर आता है तो यूँ दुआ क़ुबूल करता है... तेरे बंदों को किसी कल चैन नहीं... ये तेरी नाचीज़ बंदी तन्हा थी...!”
उसने दूसरा हट चाही तो तू ने यूं की, अज़ाब की तरह मुसाफ़िर नाज़िल करना शुरू कर दिए। और मुसाफ़िरों से ज़्यादा अस्बाब। वैसे, भई हमें क्या हक़ कि बे बात तेरी मस्लिहत में दख़ील हों। मगर परवर-दिगार इतना तो सोचा होता के इन्सानों में जितनी तूने बर्दाश्त दी है, उतना ही बोझ लाद... कहते हैं हम तो बस... और मैं दिल में डरी कि अगर दुआओं के क़ुबूल होने का यही ढंग रहा... तो कहीं वो शौहर के लिए जो अभी-अभी दुआ माँगी थी उस का भी कुछ ऐसा ही क़िस्सा ना हो जाए, और ले चला-चल एक पे एक... मेरा तो दम टूट जाएगा।
मैं एक ही क़मीज़ में बटन लगा दूँ और चाय बना दूँ... तो बहुत जानो... मुझसे भला इतने काहे को झेले जाऐंगे। सुस्त मिट्टी वैसे ही हूँ। अब इतने मियाओं को कौन बैठ के भुगतेगा।
कहते हैं कि डाकख़ाने में अगर भूले से कोई ग़लत ख़त पढ़ा जाये तो थोड़ी सी रिश्वत ले कर वापिस ले सकते हैं... काश दुआओं के मुआमले में भी कुछ ऐसा ही इंतेज़ाम होता... मगर दुआ एक दफ़ा मांगी जा चुकी थी और पै-दर-पै क़ुबूल हो रही थीं।
नई हमसफ़र बहुत ही ख़लील मा’लूम होती थीं और ज़रूरत से ज़्यादा रक़ीक़-उल-क़ल्ब, कुछ साज़क सी शायराना बीमारी... कुछ आहिस्ता बोलने की आदी... मुझे उन पर बे बात प्यार आने लगा...
“हैदराबाद जा रही हैं आप...?” उन्होंने बड़े वुसूक़ से पूछा।
मैं डरी कि इनकार करूँगी तो ख़फ़ा हो जाएंगी... लिहाज़ा बड़ी आजिज़ी से इनकार किया और बताया कि बम्बई जा रही हूँ...
“अहमदाबाद से आई होंगी।”
किस होशियारी से वो पुरानी बोतलों में नई दवा भर-भर कर सर सहला-सहला कर पिला रही थीं मगर उनका चेहरा इस क़दर रोया हुआ था कि दिल दुखाने की हिम्मत ना पड़ी...
मैंने बताया,
“पढ़ती हैं वहां...”
“जी नहीं। इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ।”
“मेरे एक चचा के साले की ख़ाला भी बम्बई में रहती हैं... उनसे मिलीएगा।”
मैंने वाअदा कर लिया... भला मैं कहाँ उनके चचा के साले की ख़ालाओं को ढूंढती फिरती।
“वहां आपके वालिद वालिदा हैं...”
“नहीं... मेरे...” बोलने ही ना दिया ख़ुद बोलीं
“अच्छा आपके शौहर होंगे।”
घन्न... वो देखिए घुमा फिराकर वही एक टांग मुर्ग़े की, शौहर, शौहर...
हिन्दोस्तान के शौहर इस क़दर मर्ख़ने... नाकें काट लें, तलाक़ें दे दें, बड़ी मुश्किल से मिलें... और मिलें तो निखट्टू्... रंडी बाज़ी करें, जुआ खेलें... मगर बीवियां हैं कि वारी जा रही हैं... जिसे देखिए अपने या पराए शौहर का रोना रो रही है। कुंवारियाँ हैं तो शौहर के गीत गा रही हैं... ब्याहियाँ हैं तो प्रीतम पर फ़िदा... और ये प्रीतम कुत्ते ख़ून थुकवाए दे रहे हैं... इन मज़ालिम माशूक़ाना पर तो ये हाल है अगर ज़रा लाड कर लेते तो ना जाने क्या होता... मैंने सोचा मियाओं के ज़ुल्म में भी कुछ मस्लिहत है।
“कहाँ रहती हैं आप... बम्बई में... कितने बच्चे हैं आपके?” मैं तो सोच में पड़ी थी... और फिर वो मियाँ के बाद बच्चों की तादाद पर उतर आईं...
“आठ...?” मैंने प्लेटफार्म पर तख़्ते गिनते हुए कहा...
“ये रेलों के साथ मुसाफ़िरों से ज़्यादा कुत्ते कहाँ से आते हैं।”
“आठ...?”
“हाँ... क्यों आप क्यों बुरा मानती हैं... यक़ीन ना आए तो उतर कर गिन लीजिए...”
“अब मैं रास्ते में कैसे उतरूँ... हाँ इंशा-अल्लाह कभी अगर आना हुआ मेरे चचा के साले की ख़ाला के यहां तो... ख़ैर... मगर बहन मा’लूम नहीं होता मुँह से...”
“मुँह से मा’लूम ही क्या होता है...” मैंने फ़लसफ़ियों के से अंदाज़ में कहा।
जब दुनिया से मुझे नफ़रत होने लगती है और हर चीज़ नीम मुर्दा और उदास लगने लगती है तो मेरे दिमाग़ में फ़लसफ़ा भरने लगता है...!
“शादी को कितने बरस हुए...” उन्होंने कुछ देर बाद पूछा।
“चार बरस तीन महीने और...”
“और आठ बच्चे... ए बहन मैं समझी थी... चलो होंगे... मगर...” वो बहुत ग़म-ज़दा सी हो गईं।
मुझे रहम आ गया... मगर मैंने तहिय्या कर लिया कि कुछ हो जाए अब और नहीं दबूँगी... वर्ना बच्चों के बाद ये नवासे और पोते भी मेरे ही सर मंढ देंगी।
और वो बीवियाँ जो मेरे हाल-ए-ज़ार से वाक़िफ़ हैं...
मैं ऊँघ ना चुकी... फिर ख़्वाह-म-ख़्वाह की लय दे पड़ेगी। आठ बच्चों से वैसे ही रूह क़ब्ज़ हुई जा रही थी।
“हाँ हाँ कहती तो हूँ... आठ...”
“माशा-अल्लाह सब ज़िंदा हैं... मगर बहन ये हुए कैसे?”
“कैसे होते हैं, जैसे दुनिया जहान में होते हैं... वैसे ही हुए होंगे।”
“मेरा मतलब है चार साल में...”
“हाँ मैं समझी... अच्छा ये मा’लूम करना चाहती हैं आप तो... ये हुआ कि कभी दो कभी तीन... और...!”
“है है...” वो लरज़ीं और मुझे बुरा लगा।
आख़िर ये कौन होती हैं बुरा मानने वाली... ये मेरा ज़ाती मुआमला है... आख़िर इन्हें क्या... चाहे कोई एक बच्चा दे चाहे दस... वही हुआ जिसका मुझे डर था। पिछली मुलाक़ातें जाग उठीं...
“सुना बहन... इनके दो-दो तीन- तीन साथ हुए... बच्चे...!” उन्हों ने शिकायत की...
और वो घबराकर अपने बच्चे गिनने लगीं।
क्योंकि सिवाए बच्चों के उन्हों ने कुछ नहीं सुना।
“क्या क़िस्सा है...?” दूसरी बोलीं।
जब मुआमला ख़ूब समझा दिया गया तो तीनों बिगड़ खड़ी हुईं।
“अभी कहती थीं शादी नहीं हुई... और अभी दो-दो तीन-तीन बच्चे होने लगे...” एक ने डाँटा।
“मेरी क्यों ना होती शादी ख़ुदा ना करे... तुम्हारी ही नहीं हुई होगी...”
बात बिगड़ने लगी...
पास से एक टिकट चैकर गुज़रे... या जाने कौन थे मुझे तो हर रेल का नौकर टिकट चैकर ही सा लगता है। मैंने झुक कर उनसे वक़्त पूछा वो बताने के बाद मुस्कुराने लगे। और फिर मुस्कुराते हुए चल दिए।
“तुम तो कहती थीं अकेली जा रही हूँ... और ये तुम्हारे...”
“ये मेरा नवासा है...”
क़ब्ल उस के कि वो कोई रोमेंटिक सा रिश्ता क़ायम कर लेतीं मैंने ख़ुद ही अपने लिए फ़ैसला कर लिया।
“नवासा...” तीनों चीख़ीं...
“या अल्लाह...” ये आज उन लोगों को मुझसे कहाँ का बैर पड़ गया था कि मेरे कुन्बे के हर फ़र्द के ज़िक्र पर बन-बन कर चौंक रही थीं।
“क्या कहती है लड़की... ये तेरा नवासा है...”
“तो आपको क्या...?”
“बहन बाल तो सफ़ैद रखे थे उनके...” दूसरी बोलीं...
“नज़ले से हो गए होंगे...” मैं बड़-बड़ाई।
और फिर में बिलकुल खिड़की से बाहर झाँकने लगी... ख़ुदकुशी को दिल ना चाहा, चलती रेल से उतरने की प्रैक्टिस ना की... ज़मीन सख़्त... और आसमान दूर...
होनहार बात हो कर रहती है... जब ज़ाइद सामान तुलवा कर बिल्टी देने लगा तो क्लर्क ने कहा, “आप का नाम...? शौहर का नाम...?”
“चुग़द...” मैंने दाँत पीस कर कहा।
“चोखे...? क्या औंडा नाम है...?” उसने मुतअज्जिब हो कर क्लर्क के कहनी मारी।
ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब उसने मुझे मिसेज़ चोखे बनाकर रसीद दी तो मैंने उसके मुँह पर अपना बटवा मअ एक अदद मोटी किताब के खींच मारा और ये सब कुछ हुआ सिर्फ़ एक शौहर की ख़ातिर...
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.