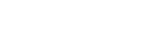लैम्प जलाने वाले
स्टोरीलाइन
यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी सच्चाई की तलाश में है। वो इस शहर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, नौकरी की, बच्चे पैदा किए और अब पेंशनधारी है। उसे यह मालूम है कि उसके शुभ चिंतकों और बुराई करने वालों की एक लम्बी सूचि है जो एक लम्बी ज़िंदगी का ज़रूरी नतीजा है। उन लोगों से उन्हें बचना भी पड़ता है और यदाकदा उसे उनकी ज़रूरत भी पड़ती रहती है। ज़िंदगी के आख़िरी मोड़ पर खड़े हो कर उसने महसूस किया था कि आपके साथ नया कुछ भी नहीं होता, सारे रिश्ते-नाते, घटनाएं-दुर्घटनाएं ख़ुद को दोहराते रहते हैं। स्मृति का देव आपको अपने चंगुल में लिए उड़ता रहता है।
(तुम सफ़र के बारे में सोच कैसे सकते हो? एक नई दुनिया के लिए ख़ुद को तैयार कर लो। अभी बहुत कुछ होना है। अभी इम्कानात ने अपने तमाम दरवाज़े खोले ही कहाँ हैं। लैम्पपोस्ट)
गली से निकलते ही नुक्कड़ पर एक आहनी लैम्पपोस्ट वाक़े’ है जिस पर पुराने वक़्तों में कभी केरोसीन तेल का लैम्प जला करता होगा। अब वो लैम्प अपने पिंजरे और शीशों समेत ग़ायब हो चुका है। अब खम्बे पर सिर्फ़ एक ब्रैकेट बची है जिस पर कबूतर या कव्वे बैठे पहरा दिया करते हैं। एक दिन उसका एक और मसरफ़ भी निकल आता है जब एक भिकारी उस ब्रैकेट से लटक कर ख़ुदकुशी कर लेता है। लेकिन इस वाक़िए’ को एक दहाई गुज़र चुकी है। मैं पहले के मुक़ाबले में कुछ ज़ियादा बूढ़ा हो गया हूँ। अपने पैंशन-याफ़्ता होने तक मैंने उस लैम्पपोस्ट का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था जो दूर से एक टूटी हुई सलीब की मानिंद दिखाई देता है और रात के धुँदलके में एक लंबे लाग़र इंसान में बदल जाता है जिसका सिर्फ़ एक हाथ हो।
“तुम मुझे नज़र-अंदाज नहीं कर सकते”, एक दिन लैम्पपोस्ट ने झुक कर मेरे दाहिने कान में कहा, क्योंकि अब मैं इसी कान से कुछ सुन पाता हूँ। मैंने मुज़्तरिब हो कर अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई। कहीं किसी ने देख लिया तो? जाने वो मेरे बारे में क्या राय क़ायम कर बैठे।
“और तुम इतने हैरान क्यों हो?”
“तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?”, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, “तुम कोई ज़िंदा चीज़ नहीं हो। तुम इस तरह झुक नहीं सकते, न बात कर सकते हो। ये तो एक बिल्कुल ही ग़ैर-हक़ीक़ी बात है।”
“मैं झुक तो गया हूँ”, खम्बे ने कहा।
मगर वो तन कर सीधा खड़ा हो जाता है क्योंकि चीनी दंदान-साज़ शांग फ़ो अपने रिक्शा में वापिस लौटता नज़र आता है। ये शांग फ़ो है जिसने मेरे तमाम ग़ैर-ज़रूरी दाँत निकाले हैं और तमाम ग़ैर-ज़रूरी दाँत लगाए भी हैं जिनके पीछे मेरा काफ़ी वक़्त सर्फ़ होता है और जिन्होंने, एक तरह से देखा जाए तो, नफ़सियाती तौर पर मुझे शांग फ़ो के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया है। इस छोटे से शहर में वो वाहिद दंदान-साज़ है। शायद मुझे किसी बी.डी.एस से रुजू’ करना चाहिए। अब इस तरह के ता’लीम-याफ़्ता डाक्टर आने लगे हैं, अगरचे चीनी दंदान साज़ों की साख अभी कम नहीं हुई है। शांग फ़ो नशे में है। वो मुझे पहचानने से इनकार कर देता है। उसके बड़े से घर का लकड़ी का सुर्ख़ फाटक खुलता है और वो रिक्शा के साथ अंदर चला जाता है। अब ये रिक्शा कल सुब्ह ही निकलने वाला है।
“शांग फ़ो बे-औलाद है”, खम्बे ने मुझसे सरगोशी की है, “और उसकी बीवी उससे उ’म्र में दस साल बड़ी है।”
“मुझे अफ़सोस है। मगर मुझे इससे क्या?”
“वो शहर का वाहिद चीनी बाशिंदा है। तुम्हें उसकी हिफ़ाज़त करनी चाहिए, तुम ये क्यों नहीं सोचते?”
“अरे हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह वो भी अपना एक ऐंटीक वैल्यू (antique value) रखता है।”, मैं हँसता हूँ।
“मुझे तुम्हारी हम-दर्दी समझ में आती है।”
और इससे पहले कि खंबा कोई जवाब दे, मैं अपने घर की तरफ़ चल देता हूँ। घर के दरवाज़े पर मैं पलट कर देखता हूँ। खंबा सुनसान सड़क पर उदास खड़ा है और शांग फ़ो की कोठी में ऊपर का एक कमरा रौशन हो गया है।
दिन के वक़्त ये खंबा किस क़दर बदनुमा और ग़ैर-ज़रूरी दिखाई देता है। पान खाने वाले उस पर उँगलियों का चूना साफ़ करते हैं और जिन्सी अमराज़ के माहिर उस पर अपने इश्तिहार चिपकाते हैं, जबकि सड़क पार शांग फ़ो की कोठी उस खम्बे की तरह क़दीम होते हुए भी उस पर रंग-ओ-रोग़न जारी है। हाल ही में उसकी दूसरी मंज़िल पर वाक़े’ खपरैल के एक छप्पर के ऊपर एक मुर्ग़-ए-बाद-नुमा नसब किया गया है जिसे शांग फ़ो के रिश्तेदारों ने मंचूरिया से भेजा है, जहाँ वो सोयाबीन की काश्त करते हैं।
“मैंने एक पूरा दौर देखा है। मैंने अंग्रेज़ी दौर-ए-हकूमत में हिन्दुस्तानी फ़ौज को मार्च करते हुए बर्मा के महाज़ की तरफ़ जाते हुए देखा है”, खंबा मुझे बता रहा है।
“और मैंने वो वक़्त भी देखा है जब आदी मुजरिम और पागल लोहे के कड़े पहना कर सड़क पर छोड़ दिए जाते थे।”
“मुझे इन बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती है?”, मैं कहता हूँ, “तुम वही बातें कह रहे हो जो सब जानते हैं।”
“मैंने बंगाल के दोनों क़हत देखे हैं।”
“आह!”, मैं मायूसी से सर हिलाता हूँ, “तुमसे बात करना बेकार है।”
खंबा चुप हो जाता है। एक चील आकर उसकी ब्रैकेट पर बैठ गई है। ब्रैकेट कमज़ोर है। वो बहुत मुश्किल से परिंदे का बोझ सँभाल पा रही है। परिंदे को आराम नहीं मिलता। वो उड़ कर शांग फ़ो की कोठी के मुर्ग़-ए-बाद-नुमा की तरफ़ चला जाता है जो वापिस लौटते हुए मौनसून के सबब घड़ी के रुख़ पर चक्कर लगा रहा है।
“ये शांग फ़ो, ये मेरे सामने पैदा हुआ”, आख़िर-कार खंबा कह उठता है।
“ये हुई न कोई बात!”, मैं सर-ता-पा तवज्जोह बन जाता हूँ।
“उसका बाप बला का अफ़ीमची था”, खंबा कहता रहा।
“वो शंघाई से ज़बरदस्ती पानी के जहाज़ पर मज़दूर बना कर लाया गया था। मगर ख़िज़रपूर की बंदरगाह में वो उस चीनी जहाज़ से भाग निकला। उसके बड़े से चेहरे पर एक इकलौता तिल था जिससे दो लाँबे बाल निकले हुए थे और उसकी आँखें थीं ही नहीं। मेरा मतलब है उसकी आँखें ऐसी थीं कि नज़र नहीं आती थीं। मगर सबको पता था उसकी आँखों में धूल झोंकना आसान काम न था। वो हमेशा अपनी चटाई पर लेता रहता और पाइप से अफ़ीम के कश लगाया करता।”
खंबा फिर दो दिन तक ख़ामोश रहता है और मुझे शक होने लगता है... क्या ये मेरा वाहिमा था? क्या वाक़ई’ मैं बूढ़ा हो रहा हूँ।
“शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो”, तीसरे दिन मैं उसे उकसाता हूँ। मगर खंबा ख़ामोश रहता है।
“ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों में यक़ीन नहीं करता”, मैं कहता हूँ, “मगर तुम समझ सकते हो, मैं आज का इंसान तो हूँ नहीं। मैंने भी इस मुल्क को तक़्सीम होते देखा है, मैंने भी इसकी सड़कों पर नफ़रत फैलाने वालों की ता’दाद को बढ़ते देखा है, बल्कि उनमें से कुछ तो अब हमारे मुल्क के नुमाइंदे बन कर दूसरे मुल्कों में भी जाने लगे हैं। मैं भी देख सकता हूँ कि किस तरह दिन-ब-दिन लोग नक़्ल-ए-हमल में इस्ति’माल होने वाले जानवरों की तरह जीने के आ’दी होते जा रहे हैं।”
“और तुम इस मुल्क के क़वानीन नाफ़िज़ करने वालों के बारे में बात नहीं करोगे”, यकायक खंबा कह उठता है, “जो अपने शहरियों की मक़अ’द तक को खंगाल लेना चाहता है?”
“मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं ख़ुद एक सरकारी दफ़्तर में अपनी ज़िंदगी गुज़ार आया हूँ”, मैं शर्मिंदगी से कहता हूँ।
“लोगों के साथ सद्द-ओ-मत करने के अ’मल में मैं भी बराबर का शरीक रहा हूँ। और अब मेरी हैसियत एक ना-सज़ा-याफ़्ता मुजरिम से भी बदतर है। मेरे ज़मीर पर एक बड़ा बोझ है।”
“आह और मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ रहा था।”
मैं खम्बे को अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाहता था। मगर मुझे मा’लूम है मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नादिर वाक़िआ’ कभी पेश नहीं आया जो किसी के लिए दिलचस्पी का हामिल हो।
मैं इस शहर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, नौकरी की, बच्चे पैदा किए और अब पैंशन-याफ़्ता हूँ। मेरे बही-ख़्वाहों और मेरी बद-गोई करने वालों की एक लंबी फ़हरिस्त है जो एक लंबी ज़िंदगी का लाज़िमी नतीजा है। उनसे मुझे बचना भी पड़ता है और गाहे-ब-गाहे मुझे उनकी ज़रूरत भी पड़ती रहती है। ज़िंदगी के आख़िरी मोड़ पर खड़े हो कर आप देखते हैं आपके साथ नया कुछ भी नहीं होता, सारे रिश्ते नाते, वाक़िआ’त-ओ-हादिसात ख़ुद को दोहराते रहते हैं। हाफ़िज़े का देव आपको अपने चंगुल में लिए उड़ता रहता है।
मेरे घर वालों का ख़याल है मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं। मैं बिला-वज्ह बीमार पड़ता हूँ और बिला-वज्ह ठीक हो जाता हूँ। मैं सारी ज़िम्मेदारियों से सुबुक-दोश हो चुका हूँ और अब मेरे और बच्चों के दरमियान एक नस्ल का फ़ासिला हो चुका है। मैं उन्हें उफ़ुक़ पर ग़ायब होते देखता रहता हूँ, बल्कि उनमें से बहुत सारे तो समंदर पार जा चुके हैं। समाज में रह कर मुझसे जिन बातों की तवक़्क़ो’ की जाती है, मैं उनमें पूरा नहीं उतरता और मुझे ख़ुद इस पर हैरत होती है, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी समाज के मुरव्वजा उसूलों को ध्यान में रखकर गुज़ारी है। मैं अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर खिड़की के रुख़ लेटा आसमान की तरफ़ ताकता रहता हूँ जिसमें शांग फ़ो का मुर्ग़-ए-बाद-नुमा अपना चक्कर लगाता रहता है। मेरी किताबों की अलमारी के शीशे धुँदले पड़ चुके हैं, उस पर लगे हुए क़ुफ़्ल पर ज़ंग चढ़ चुका है और सच तो ये है कि उनमें से बहुतेरी किताबों को मैंने छुआ तक नहीं है, जबकि एक वक़्त था मैं उनकी तलाश में ट्रेन और बसों में मेलों की मसाफ़त तय किया करता था। हर साल न जाने कौन मेरी मग़रिबी दीवार पर एक कैलेंडर टांग जाता है, इस बात से ला-पर्वा कि मुझे अब उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है। ये कैलेंडर हवा की ज़द में आकर दीवार के पलस्तर
पर एक नीम-बैज़वी लकीर खींच डालता है और दिन-ब-दिन उसे किसी ज़ख़्म की तरह गहरा करता जाता है। कभी-कभार मैं चौंक कर अपने बिस्तर पर उठ बैठता हूँ। कौन हूँ मैं? इस सय्यारे पर मेरा काम क्या है? जाने कितना वक़्त लग जाता है तब जाकर मैं इस क़ाबिल हो पाता हूँ कि ज़मान-ओ-मकाँ के निज़ाम मैं ख़ुद को दरियाफ़्त कर सकूँ। इस बार सर्दी ज़ोर की आई है। मैं एक लंबी बीमारी का शिकार हो जाता हूँ। मौसम-ए-सर्मा उ’म्र-दराज़ लोगों के लिए दूसरी दुनिया की तरफ़ कूच करने का मौसम होता है। क्या मैं इस सफ़र के लिए तैयार हूँ? मेरे जिस्म की हड्डियाँ सूख चुकी हैं। मुझे ठंड के ख़िलाफ़ बड़ी जद्द-ओ-जहद करनी पड़ती है। अक्सर मेरे न चाहने पर भी मेरी खिड़की में कोहरा भर जाता है। मेरे घर वाले मुझसे परेशान हैं। मैं उन्हें अपनी खिड़की बंद करने की इजाज़त नहीं देता। कभी जब मुर्ग़-ए-बाद-नुमा कोहरे में तहलील हो कर नज़र से ग़ायब हो जाता है तो मुझे घबराहट होती है। मैं अपनी ऐ’नक ढूँढ कर उसके अंदर से आसमान का जायज़ा लेता हूँ। वो मुझे कहीं गर्दिश करता दिखाई नहीं देता। फिर नज़र आने लगता है। वो बहुत धीमी रफ़्तार से चक्कर लगा रहा है, शायद घड़ी के रुख़ पर... नहीं, शायद घड़ी के मुख़ालिफ़। हाँ वो घड़ी के मुख़ालिफ़ चक्कर लगा रहा है। फिर वो ग़ायब हो जाता है।
मगर अब मुझे इत्मीनान है। मैं बिस्तर पर लेट कर चैन की सांस लेता हूँ। लिहाफ़ और कम्बल अपनी रतूबत भरी नाक तक खींच कर मुस्कुराता हूँ। अगर इस जाड़े से गुज़र पाया तो शायद दुबारा शांग फ़ो के क्लीनिक जाऊँ। मेरे कुछ और दाँत हिल रहे हैं। शायद इस बार शांग फ़ो मेरे दाँतों के साथ कोई चमत्कार कर सके। दुनिया कितनी तेज़ी से तरक़्क़ी कर रही है। साईंस अलादीन के जिन की तरह इंसान को अपनी हथेली पर लिए उड़ रही है, उसकी हर ख़्वाहिश पूरी करती जा रही है। अगले सौ साल के अंदर हमारे लिए करने को कुछ भी न रह जाएगा। हमारी हैसियत एक तमाश-बीन से ज़ियादा की न होगी।
सर्दी में कमी आ गई है। दूसरे तमाम उ’म्र-दराज़ लोगों की तरह मेरी भी तबीअ’त सुधरने लगी है। एक अ’र्से के बा’द मैं गहरी नींद सोया हूँ और अब रात हो चुकी है। रात साफ़ है, कहीं पर कोहरे का नाम-ओ-निशान नहीं। खिड़की से आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें तारे रौशन हैं। मेरे लिए गर्म सूप लाया जाता है। मैं पेट भर कर पीता हूँ। फिर सोने की कोशिश करता हूँ। शायद ये आधी रात का वक़्त है जब मैं अपने बिस्तर से उतर कर दो-चार क़दम चलता हूँ। इससे ज़ियादा ताज़ा-दम मैंने ज़िंदगी में कभी ख़ुद को न महसूस किया होगा। मैं कम्बल को अपने जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेट कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ। मेरे सबसे छोटे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला है। वो अपने कम्पयूटर पर कुछ प्रिंट कर रहा है। वो कभी शाइ’र बनना चाहता था। वो शाइ’र उसके अंदर जाने कहाँ गुम हो गया। कच्चे आँगन से गुज़र कर मैं सद्र दरवाज़ा खोलता हूँ और अब मैं बाहर फ़ुट-पाथ पर खड़ा हूँ। सड़क पर शांग फ़ो का घर तारीक पड़ा है। चाँद कुरह-ए-अर्ज़ के दूसरे निस्फ़ पर चमक रहा होगा जिसे धूप में लोग देख न पा रहे होंगे। इस पूरी सड़क पर सिर्फ़ मेरे कमरे की खिड़की से रोशनी का एक मुसल्लस फ़ुट-पाथ से गुज़र कर सड़क पर गिर रहा है। मेरी खिड़की के नीचे एक मतरूक संग-ए-मील है जिस पर बच्चे दिन के वक़्त क्रिकेट खेलते हैं और रात के वक़्त में बैठता हूँ। मैं उस पर बैठ कर (मैं अपने कूल्हों में उसकी ठंडक महसूस करता हूँ) सामने खड़े लैम्पपोस्ट की तरफ़ ताकता हूँ। उसका हयूला मुझे दिखाई देता है। मैं सड़क पार शांग फ़ो की बालाई मंज़िल के छप्पर को ताकता हूँ। मुर्ग़-ए-बाद-नुमा घर के ख़ाके से हम-आहंग हो गया है। अगर तारे कुछ और रोशन होते!
हवा बंद है। सड़क की दोनों जानिब दूर तक एक भी इंसानी साया नहीं। कुल मिला कर ये मेरी ज़िंदगी की एक अच्छी रात है। और जब मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे क़दमों की चाप सुनाई देती है। दो आदमी अपने कंधों पर एक सीढ़ी हुए एक उजालिये और कनस्तर के साथ मेरे सामने से गुज़रते हैं। दोनों अपने उजालिये की रोशनी में मुस्कुरा कर मेरी तरफ़ ताकते हैं और खम्बे से सीढ़ी टिका कर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं।
“लैम्प जलाने वाले...”, मैं हैरानी से सोचता हूँ मगर संग-ए-मील पर बैठा रहता हूँ। मैं देखता हूँ, पहला आदमी सीढ़ी पर चढ़ कर ब्रैकेट तक पहुँच गया है, दूसरा उसे कनस्तर थमा रहा है... और तब, मेरे ख़ुदा! मैं अपनी जगह उठ खड़ा होता हूँ। पहली बार में देखता हूँ कि लैम्पपोस्ट की ब्रैकेट से एक लैम्प लटक रहा है जिसके अंदर वो पैराफीन उंडेल रहा है। वो अपने साथी को पैराफीन का कनस्तर वापिस देकर उजालिया ले लेता है और तब वो वाक़िआ’ होता है जो इस कहानी का अहम मोड़ है। लैम्प अपने रंगीन शीशों के अंदर जल उठता है। सीढ़ी हटा ली जाती है और वो दोनों सीढ़ी कंधों से लटकाए वापिस लौटते हैं। वो मेरी तरफ़ देखकर दुबारा मुस्कुराते हैं और सड़क पर चलते हुए अँधेरे में गुम हो जाते हैं।
एक पल के लिए मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। क्या मैं ख़्वाब देख रहा हूँ? मगर मेरे यक़ीन न करने पर भी लैम्पपोस्ट की रोशनी सड़क पर फैल रही है और आस-पास की दीवारों पर जा टिकी है। मैं लैम्पपोस्ट के पास जाता हूँ।
क्या वाक़ई! मैं शश्दर सा लैम्पपोस्ट को जलते देखता रहता हूँ। उसमें सफ़ेद, हरे और नीले रंग के शीशे लगे हैं। अंदर फ़लीता ख़ासी लंबी लौ दे रहा है जिसने अपने दंदानेदार बैरम के सबब माही-ए-दम की शक्ल इख़तियार कर ली है। ये लैम्प फ़िलिज़्ज़ कारी एक नादिर नमूना है जिसके बालाई सिरे की मुजव्वफ़ सत्ह को इंगलिस्तानी ताज की शक्ल दे दी गई है।
“हाँ!”, लैम्पपोस्ट की सरगोशी सुनाई देती है। “ये मेरी ज़िंदगी की एक अच्छी रात है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सही सिम्त की तरफ़ लौट रहा है।”
“मुझे सोचने दो”, मैं कहता हूँ। मैं मुड़ कर देखता हूँ। मुझे सड़क की दोनों जानिब दूर तक क़दीम दौर के ये दो-रूया लैम्प रौशन दिखाई देते हैं। इसी दरमियान आसमान पर कुछ नए तारे भी बड़ी ता’दाद में आ गए हैं जिनकी रोशनी में शांग फ़ो का मुर्ग़-ए-बाद-नुमा नज़र आने लगा है। मुझे अपनी रगों में गर्म ख़ून दौड़ता सुनाई देता है।
“क्या ये मुम्किन है?”
“बिल्कुल!”, लैम्पपोस्ट वसूक़ के साथ कहता है।
“अच्छे दिनों की शुरू’आत कभी भी हो सकती है। देखो हम दोनों एक दूसरे को कितना सही समझ पा रहे हैं।”
“वो तो है।”, मैं खम्बे पर अपने दोनों हाथ टिका कर ऊपर ताकता हूँ जहाँ लैम्प अपने शीशों के अंदर जल रहा है और उसके पस-ए-मंज़र में तारे मुहद्दब आसमान पर अपने जावेदाँ सफ़र पर रवाँ हैं। “और मैं समझ रहा था ये मेरी ज़िंदगी की आख़िरी सर्दी है। वाक़ई’ ये एक नई शुरू’आत है। अभी सफ़र का मौसम नहीं आया।”
“तुम सफ़र के बारे में सोच कैसे सकते हो?”, लैम्पपोस्ट की आवाज़ में हम-दर्दी है।
“एक नई दुनिया के लिए ख़ुद को तैयार कर लो। अभी बहुत कुछ होना है। अभी इम्कानात ने अपने तमाम दरवाज़े खोले ही कहाँ हैं।”
“शुक्रिया!”, मैं मुस्कुराता हूँ और लैम्प की क़दीम रोशनी में सड़क पर चलने लगता हूँ। मैं इस रोशनी के हलक़े के आख़िरी सिरे से लौट आता हूँ, उसे आँखों में भर कर खड़ा रहता हूँ। आँखें खोल कर मुस्कुराता हूँ।
“वाक़ई’ इम्कानात ने अपने कुछ दरवाज़े खोले तो हैं।”
रात का बाक़ी हिस्सा मैं संग-ए-मील पर बैठ कर गुज़ार देता हूँ। मेरी आँखें लैम्पपोस्ट के रंगीन शीशों से हटती ही नहीं... यहाँ तक कि किसी क़रीबी मस्जिद से फ़ज्र की अज़ान सुनाई देती है। मैं अपने कमरे में लौटता हूँ और बड़ी गहरी नींद सो जाता हूँ। दिन का बड़ा हिस्सा बीत चुका है जब मैंने आँखें खोली हैं। सूरज आसमान पर नहीं है। मैं खिड़की के बाहर ताकता हूँ। कोहरा सड़क पर इधर से उधर फैल रहा है। मेरी ग़शी अभी दूर नहीं हुई है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। मैं रात के वाक़िए’ को याद कर के मुस्कुराना चाहता हूँ, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाता। मैं अव्वलीन ज़रूरियात से फ़राग़त पा कर बाहर सड़क पर आता हूँ और मेरी नज़र लैम्पपोस्ट की तरफ़ उठ जाती है जो अब वहाँ नहीं है। अब उस जगह पर एक ऊंचा बिजली का खंबा रस्सी के सहारे खड़ा किया जा रहा है। मैं घबरा कर सड़क पर दूर तक नज़र दौड़ाता हूँ। कहीं मैंने ग़लत तो नहीं देख लिया है? मगर सड़क पर ता-हद्द-ए-नज़र उसी तरह के खम्बे खड़े हैं या नसब किए जा रहे हैं।
“ये क्या कर रहे हो तुम लोग?”, मैं एक रस्सी खींचने वाले से पूछता हूँ। वो एक अन्न-पढ़ मज़दूर है। वो मेरी बात समझ नहीं पाता
“बस दो दिन की बात है जनाब, फिर आप लोगों को यहाँ रात की जगह दिन दिखाई देगा!”, एक ख़ुश-पोश ओवर-सीअर मुदाख़िलत करता है। और तब मुझे पुराना लैम्पपोस्ट ज़मीन पर पड़ा दिखाई देता है। उसकी ब्रैकेट उसके बराबर रखी हुई है।
“ये क्या किया तुम ने?”, मैं उस सफ़ेद-पोश शख़्स से कहता हूँ जो काम की निगरानी कर रहा है।
“ये फ़ैसला लेने वाले तुम लोग होते कौन हो? हमसे हमारी रातों को छीनने का हक़ तुम्हें किस ने दिया?”
वो शख़्स कुछ न समझ कर सर हिलाता है मगर एहतिरामन ख़ामोश रहता है। मैं झुक कर गिरे हुए खम्बे पर अपनी हम-दर्द उँगलियाँ रखता हूँ।
“ख़ुदा-हाफ़िज़!”, खम्बे ने मुझसे सरगोशी की है।
“अपने आँसुओं पर क़ाबू रखो। ये तो एक दिन होना ही था।”
“उसे न छूना!”, मुझे ओवर-सीअर की तंबीह सुनाई देती है।
“ये सरकारी प्रॉपर्टी है।”
“ख़ुदा-हाफ़िज़!”, मैं खम्बे को जवाब देता हूँ और मुड़ कर ओवर-सीअर से मुख़ातिब होता हूँ।
“तुम इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराए जाओगे।”
वो लोग बिजली के खम्बे को गाड़ कर पुराना खंबा ट्रक में लाद कर चले गए हैं। सिर्फ़ एक राज मिस्त्री मज़दूर की मदद से उसकी बुनियाद को सीमेंट रेत और कंक्रीट से भर रहा है। सूरज ने बादल के किनारों से एक पल के लिए झाँका है और मुझे लैम्पपोस्ट के संग-ए-मील पर बैठा पाया है। शांग फ़ो का मुर्ग़-ए-बा’द-नुमा तेज़ी से चक्कर लगा रहा है, जैसे उस पर दौरा पड़ गया हो। दो-रूया घरों के बावर्ची-ख़ानों का धुआँ कोहरे में मिलने लगा है। इस सड़क पर शाम की तैयारियाँ शुरू’ हो गई हैं। मेरी बाईं पसलियों में एक टीस उभरती है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में लौटता हूँ। दो दिन तक ये दर्द मुझे बेचैन रखता है। मैंने इस बारे में किसी को बताया नहीं है। तीसरी रात मुझे गहरी नींद आ जाती है। जाने क्यों मुझे लगता है मैं अब इस नींद से कभी जाग न पाऊँगा। मैं ख़्वाब में लैम्पपोस्ट को देखता हूँ जिससे एक भिकारी लटक रहा है। मैं शांग फ़ो के बाप को भी देखता हूँ जो चटाई पर लेटा हुआ पाइप पी रहा है।
“ये शब अपने-अपने करम का फल है”, वो कहता है, और मैं देखता हूँ वो अपनी बग़ैर आँखों वाली आँखों से मुझे ताक रहा है।
एक हफ़्ते के बा’द में सड़क पर आया हूँ। संग-ए-मील अपनी जगह पर नसब है। मुर्ग़-ए-बा’द-नुमा सुर्ख़ आसमान के नीचे धीरे-धीरे चक्कर लगा रहा है। नए लैम्पपोस्ट के नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं संग-ए-मील पर बैठा-बैठा दिन को दम तोड़ते देख रहा हूँ। अँधेरा अच्छा-ख़ासा फैल चुका है जब मुझ पर ये हक़ीक़त खुलती है कि लड़के क्रिकेट खेल कर जा चुके हैं और मैं अकेला संग-ए-मील पर बैठा हुआ हूँ। कोई राहगीर अँधेरे में मुझसे टकरा न जाए। शांग फ़ो की कोठी की बालाई मंज़िल की खिड़कियाँ रौशन हो गई हैं। कोहरा शहर की कसाफ़त के साथ मिलकर कुछ और गहरा हो गया है। अभी मैंने उठने का इरादा किया ही है कि लैम्पपोस्ट की चोटी पर एक हल्की, यर्क़ान-ज़दा रोशनी जाग उठती है। मैं उठने का इरादा मुल्तवी कर देता हूँ। धीरे-धीरे लैम्प की रोशनी में शिद्दत आ जाती है और आख़िर-कार ये पूरी आब-ओ-ताब के साथ जल उठता है। कोहरे के बावुजूद ये लैम्प हर शय को अपनी हैरत-अंगेज़ रोशनी की गिरफ़्त में ले लेता है। वो कितनी बेबाकी से हर दीवार पर अपनी पीली यर्क़ान-ज़दा रोशनी फैला रहा है, यहाँ तक कि शांग फ़ो का मुर्ग़-ए-बादनुमा भी इस में साफ़ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं शहर की किसी अजनबी सड़क पर चला आया हूँ। मैं धीरे-धीरे चलते हुए उस लैम्पपोस्ट के नीचे चला जाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सोडियम लैम्प है और कम-अज़-कम पच्चीस फ़ीट की ऊंचाई पर होने के बावुजूद उसकी पीली रोशनी इतनी तेज़ है कि मैं अपने हाथ की लकीरों को भी पढ़ सकता हूँ।
“हेलो लैम्प पोस्ट, कैसे हो?”
मैं खम्बे पर हाथ रखकर उससे मुख़ातिब होता हूँ। लैम्पपोस्ट किसी देव की तरह खड़ा अपने अफ़रीती लैम्प की वाहिद आँख से मेरी तरफ़ सर्द-मेहरी से ताक रहा है। उसकी रोशनी ज़र्द सय्याल की तरह मेरी आँखों में भर रही है। वो मेरी बात का जवाब नहीं देता। शायद उसे एक बहुत बड़े रक़्बे पर रोशनी फैलानी पड़ती है और मेरे लिए उसके पास वक़्त नहीं है।
मैं शिकस्त-ख़ुर्दा घर के अंदर लौटता हूँ। सोडियम वेपर लैम्प की ज़र्दी माइल रोशनी मेरे कमरे में भर गई है और कमरा अजनबी दिखाई पड़ रहा है। मैं खिड़की के पास जाता हूँ, एक नज़र नए लैम्पपोस्ट पर डालता हूँ, दूसरी नज़र मुर्ग़-ए-बाद-नुमा की तरफ़ दौड़ाता हूँ जो इतनी दूरी के बावुजूद साफ़ गर्दिश करता दिखाई दे रहा है। आह अब उसका इसरार ख़त्म हो चुका है। मैं खिड़की के दोनों किवाड़ सख़्ती से बंद कर के बिस्तर पर लेट जाता हूँ।
आँखें बंद करते ही मुझे पुराना लैम्पपोस्ट दिखाई देता है जिसके सामने से लैम्प जलाने वाले सीढ़ी उठाए हुए गुज़र रहे हैं। मैं भिकारी को भी देखता हूँ जो लैम्प पोस्ट से लटक रहा है और जिसके दोनों हाथ एड़ियों तक लाँबे हो गए हैं। और फिर मुझे शांग फ़ो का बाप दिखाई देता है जो एक पतली चटाई पर लेटा हुआ पंखा झल रहा है।
“ये शब अपने-अपने करम का फल है”, वो अफ़ीम की नलकी से मुँह हटा कर कहता है।
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.